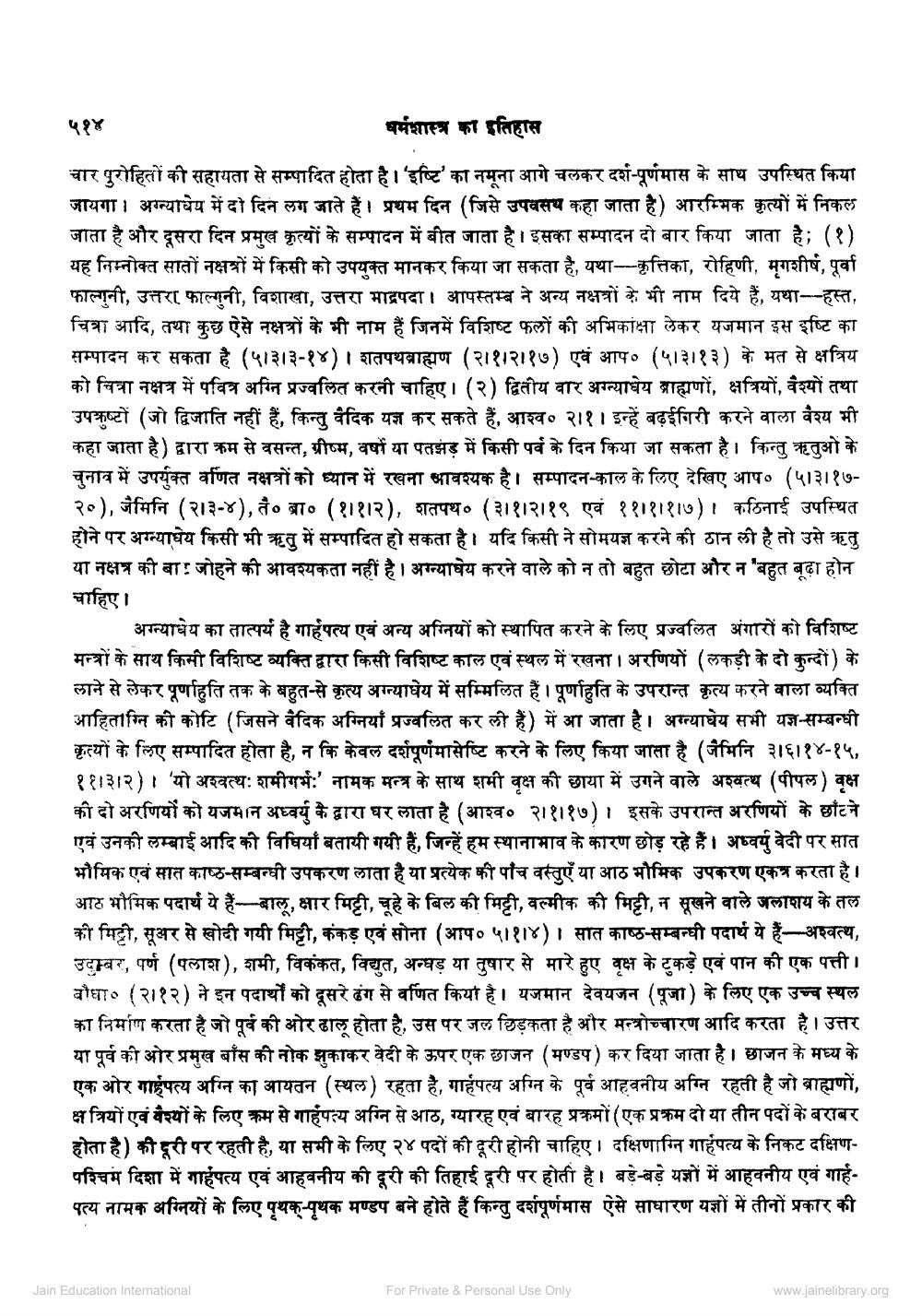________________
५१४
धर्मशास्त्र का इतिहास
चार पुरोहितों की सहायता से सम्पादित होता है । 'इष्टि' का नमूना आगे चलकर दर्श- पूर्णमास के साथ उपस्थित किया जायगा । अग्न्याधेष में दो दिन लग जाते हैं। प्रथम दिन (जिसे उपवसथ कहा जाता है) आरम्भिक कृत्यों में निकल जाता है और दूसरा दिन प्रमुख कृत्यों के सम्पादन में बीत जाता है। इसका सम्पादन दो बार किया जाता है; ( १ ) यह निम्नोक्त सातों नक्षत्रों में किसी को उपयुक्त मानकर किया जा सकता है, यथा -- कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तरा भाद्रपदा । आपस्तम्ब ने अन्य नक्षत्रों के भी नाम दिये हैं, यथा-हस्त, चित्रा आदि, तथा कुछ ऐसे नक्षत्रों के भी नाम हैं जिनमें विशिष्ट फलों की अभिकांक्षा लेकर यजमान इस इष्टि का सम्पादन कर सकता है ( ५।३।३-१४) । शतपथब्राह्मण ( २/१/२/१७) एवं आप० (५।३।१३ ) के मत से क्षत्रिय को चित्रा नक्षत्र में पवित्र अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। (२) द्वितीय वार अग्न्याधेय ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा उपक्रुष्टों (जो द्विजाति नहीं हैं, किन्तु वैदिक यज्ञ कर सकते हैं, आश्व० २।१ । इन्हें बढ़ईगिरी करने वाला वैश्य मी कहा जाता है) द्वारा क्रम से वसन्त, ग्रीष्म, वर्षों या पतझड़ में किसी पर्व के दिन किया जा सकता है। किन्तु ऋतुओं के चुनाव में उपर्युक्त वर्णित नक्षत्रों को ध्यान में रखना आवश्यक है । सम्पादन -काल के लिए देखिए आप० (५।३।१७२०), जैमिनि (२।३-४), तै० ब्रा० (१।१।२), शतपथ ० ( ३ | १ |२| १९ एवं ११ । १ । १ । ७ ) | कठिनाई उपस्थित होने पर अग्न्याधेय किसी भी ऋतु में सम्पादित हो सकता । यदि किसी ने सोमयज्ञ करने की ठान ली है तो उसे ऋतु या नक्षत्र की बाट जोहने की आवश्यकता नहीं है। अग्न्याधेय करने वाले को न तो बहुत छोटा और न बहुत बूढ़ा होन चाहिए ।
अग्न्याधेय का तात्पर्य है गार्हपत्य एवं अन्य अग्नियों को स्थापित करने के लिए प्रज्वलित अंगारों को विशिष्ट मन्त्रों के साथ किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट काल एवं स्थल में रखना। अरणियों ( लकड़ी के दो कुन्दों) के लाने से लेकर पूर्णाहुति तक के बहुत-से कृत्य अग्न्याधेय में सम्मिलित हैं। पूर्णाहुति के उपरान्त कृत्य करने वाला व्यक्ति आहिताग्नि की कोटि ( जिसने वैदिक अग्नियाँ प्रज्वलित कर ली हैं) में आ जाता है । अग्न्याधेय सभी यज्ञ - सम्बन्धी कृत्यों के लिए सम्पादित होता है, न कि केवल दर्शपूर्णमासेष्टि करने के लिए किया जाता है (जैमिनि ३।६।१४-१५, ११।३।२ ) । 'यो अश्वत्थः शमीगर्भः' नामक मन्त्र के साथ शमी वृक्ष की छाया में उगने वाले अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष दो अरणियों को यजमान अध्वर्यु के द्वारा घर लाता है ( आश्व० २।१।१७ ) । इसके उपरान्त अरणियों के छाँटने एवं उनकी लम्बाई आदि की विधियां बतायी गयी हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव के कारण छोड़ रहे हैं। अध्वर्यु वेदी पर सात एवं सात काष्ठ-सम्बन्धी उपकरण लाता है या प्रत्येक की पाँच वस्तुएँ या आठ भौमिक उपकरण एकत्र करता है। आठ भौमिक पदार्थ ये हैं- बालू, क्षार मिट्टी, चूहे के बिल की मिट्टी, वल्मीक की मिट्टी, न सूखने वाले जलाशय के तल की मिट्टी, सूअर से खोदी गयी मिट्टी, कंकड़ एवं सोना ( आप ० ५।१।४ ) । सात काष्ठ सम्बन्धी पदार्थ ये हैं अश्वत्थ, उदुम्बर, पर्ण ( पलाश), शमी, विकंकत, विद्युत, अन्धड़ या तुषार से मारे हुए वृक्ष के टुकड़े एवं पान की एक पत्ती । बौधा० (२०१२) ने इन पदार्थों को दूसरे ढंग से वर्णित किया है। यजमान देवयजन (पूजा) के लिए एक उच्च स्थल का निर्माण करता है जो पूर्व की ओर ढालू होता है, उस पर जल छिड़कता है और मन्त्रोच्चारण आदि करता है। उत्तर या पूर्व की ओर प्रमुख बाँस की नोक झुकाकर वेदी के ऊपर एक छाजन (मण्डप) कर दिया जाता है । छाजन के मध्य के एक ओर गार्हपत्य अग्नि का आयतन (स्थल) रहता है, गार्हपत्य अग्नि के पूर्व आहवनीय अग्नि रहती है जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए क्रम से गार्हपत्य अग्नि से आठ, ग्यारह एवं बारह प्रक्रमों ( एक प्रक्रम दो या तीन पदों के बराबर होता है) की दूरी पर रहती है, या सभी के लिए २४ पदों की दूरी होनी चाहिए। दक्षिणाग्नि गार्हपत्य के निकट दक्षिणपश्चिम दिशा में गार्हपत्य एवं आहवनीय की दूरी की तिहाई दूरी पर होती है। बड़े-बड़े यज्ञों में आहवनीय एवं गाईपत्य नामक अग्नियों के लिए पृथक-पृथक मण्डप बने होते हैं किन्तु दर्शपूर्णमास ऐसे साधारण यज्ञों में तीनों प्रकार की
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org