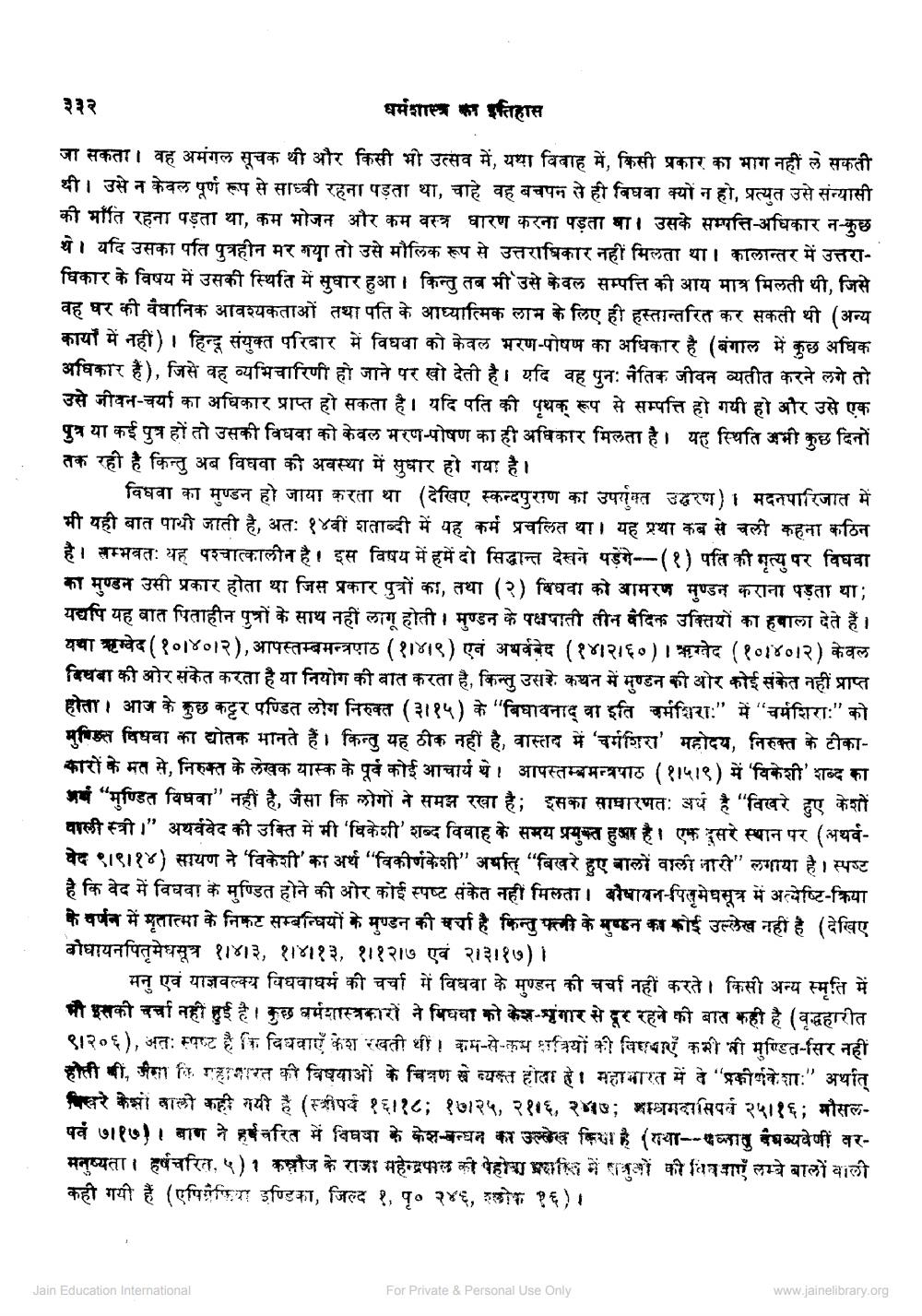________________
३३२
धर्मशास्त्र का इतिहास जा सकता। वह अमंगल सूचक थी और किसी भी उत्सव में, यथा विवाह में, किसी प्रकार का भाग नहीं ले सकती थी। उसे न केवल पूर्ण रूप से साध्वी रहना पड़ता था, चाहे वह बचपन से ही विधवा क्यों न हो, प्रत्युत उसे संन्यासी की भाँति रहना पड़ता था, कम भोजन और कम वस्त्र धारण करना पड़ता था। उसके सम्पत्ति-अधिकार न-कुछ थे। यदि उसका पति पुत्रहीन मर गया तो उसे मौलिक रूप से उत्तराधिकार नहीं मिलता था। कालान्तर में उत्तराधिकार के विषय में उसकी स्थिति में सुधार हुआ। किन्तु तब भी उसे केवल सम्पत्ति की आय मात्र मिलती थी, जिसे वह घर की वैधानिक आवश्यकताओं तथा पति के आध्यात्मिक लाभ के लिए ही हस्तान्तरित कर सकती थी (अन्य कार्यों में नहीं)। हिन्द संयक्त परिवार में विधवा को केवल भरण-पोषण का अधिकार है अधिकार हैं), जिसे वह व्यभिचारिणी हो जाने पर खो देती है। यदि वह पुनः नैतिक जीवन व्यतीत करने लगे तो उसे जीवन-चर्या का अधिकार प्राप्त हो सकता है। यदि पति की पृथक रूप से सम्पत्ति हो गयी हो और उसे एक पुत्र या कई पुत्र हों तो उसकी विधवा को केवल भरण-पोषण का ही अधिकार मिलता है। यह स्थिति अभी कुछ दिनों तक रही है किन्तु अब विधवा की अवस्था में सुधार हो गया है।
विधवा का मुण्डन हो जाया करता था (देखिए स्कन्दपुराण का उपर्युक्त उद्धरण) । मदनपारिजात में भी यही बात पायी जाती है, अतः १४वीं शताब्दी में यह कर्म प्रचलित था। यह प्रथा कब से चली कहना कठिन है। सम्भवतः यह पश्चात्कालीन है। इस विषय में हमें दो सिद्धान्त देखने पड़ेंगे--(१) पति की मृत्यु पर विधवा का मुण्डन उसी प्रकार होता था जिस प्रकार पुत्रों का, तथा (२) विधवा को आमरण मुण्डन कराना पड़ता था; यद्यपि यह वात पिताहीन पुत्रों के साथ नहीं लागू होती। मुण्डन के पक्षपाती तीन वैदिक उक्तियों का हवाला देते हैं। यथा ऋग्वेद (१०।४०१२), आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।४।९) एवं अथर्ववेद (१४१२।६०) । ऋग्वेद (१०४०।२) केवल विधबा की ओर संकेत करता है या नियोग की बात करता है, किन्तु उसरे कथन में मुण्डन की ओर कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। आज के कुछ कट्टर पण्डित लोग निरुक्त (३।१५) के "बिधावनाद् वा इति चर्मशिराः" में "चर्मशिराः” को मुवित विधवा का द्योतक मानते हैं। किन्तु यह ठीक नहीं है, वास्तव में 'चशिरा' महोदय, निरुक्त के टीकाकारों के मत से, निरुक्त के लेखक यास्क के पूर्व कोई आचार्य थे। आपस्तम्बमन्त्रपाठ (११५१९) में 'विकेशी' शब्द का अर्थ "मुण्डित विधवा" नहीं है, जैसा कि लोगों ने समझ रखा है। इसका साधारणतः अर्थ है "विखरे हुए केशों पाली स्त्री।" अथर्ववेद की उक्ति में भी विकेशी' शब्द विवाह के समय प्रयुक्त हुआ है। एक दूसरे स्थान पर (अथर्ववेद ९।९।१४) सायण ने 'विकेशी' का अर्थ "विकीर्णकेशी" अर्थात् “बिखरे हुए बालों वाली नारी" लगाया है। स्पष्ट है कि वेद में विधवा के मुण्डित होने की ओर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। बौधायन-पितृमेघसूत्र में अत्येष्टि-क्रिया के वर्णन में मृतात्मा के निकट सम्बन्धियों के मुण्डन की चर्चा है किन्तु फ्ली के मुण्डन का कोई उल्लेख नहीं है (देखिए बौधायनपितृमेधसूत्र १।४।३, १।४।१३, १।१२।७ एवं २।३।१७) ।
__ मनु एवं याज्ञवल्क्य विधवाधर्म की चर्चा में विधवा के मुण्डन की चर्चा नहीं करते। किसी अन्य स्मृति में भी इसकी चर्चा नहीं हुई है। कुछ धर्मशास्त्रकारों ने मिघवा को केश-श्रृंगार से दूर रहने की बात कही है (वृद्धहारीत ९।२०६), अतः स्पष्ट है कि विधवाएँ कैश रखती थीं। कम-से-कम शात्रियों की विधाएँ कभी भी मुण्डित-सिर नहीं होती थी, जैसा कि महाभारत की विषयाओं के चित्रण खे व्यक्त होता है। महाभारत में ते "प्रकीर्णके शाः' अर्थात् बिसरे केशी वालो कही गयी है (स्त्रीपद १६।१८; १७३२५, २११६, २०७; माधगदासिपर्व २५।१६; मौसलपर्व ७।१५)। बाग ने हर्षचरित में विधवा के केश-बन्धन का उल्लेख किया है (गया--लातु वैधव्यवेणी वरमनुष्यता। हर्षचरित, ५)। कनौज के राजा महेन्द्रपाल की पेहोश प्रसारित में शत्रुओं की विधवाएँ लम्बे बालों वाली कही गयी हैं (एपिरोफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० २४६, श्लोक १६) ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org