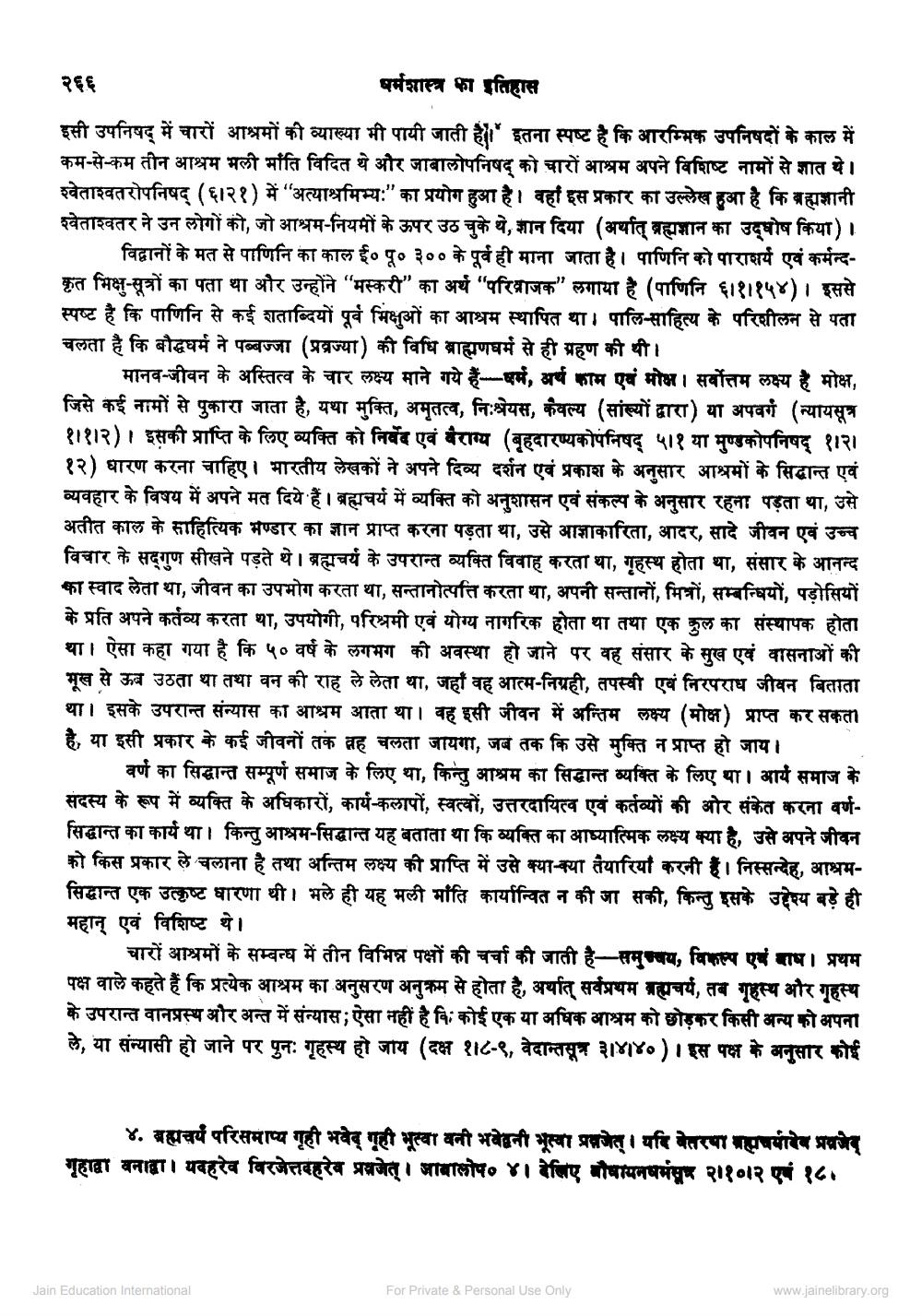________________
२६६
धर्मशास्त्र का इतिहास
इसी उपनिषद् में चारों आश्रमों की व्याख्या भी पायी जाती है। इतना स्पष्ट है कि आरम्भिक उपनिषदों के काल में कम-से-कम तीन आश्रम भली भांति विदित थे और जाबालोपनिषद् को चारों आश्रम अपने विशिष्ट नामों से ज्ञात थे। श्वेताश्वतरोपनिषद् (६।२१) में “अत्याश्रमिभ्यः” का प्रयोग हुआ है। वहां इस प्रकार का उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मज्ञानी श्वेताश्वतर ने उन लोगों को, जो आश्रम-नियमों के ऊपर उठ चुके थे, ज्ञान दिया (अर्थात् ब्रह्मज्ञान का उद्घोष किया)।
विद्वानों के मत से पाणिनि का काल ई० पू० ३०० के पूर्व ही माना जाता है। पाणिनि को पाराशर्य एवं कर्मन्दकृत भिक्षु-सूत्रों का पता था और उन्होंने “मस्करी" का अर्थ "परिव्राजक" लगाया है (पाणिनि ६।१।१५४)। इससे
नि से कई शताब्दियों पूर्व मिक्षओं का आश्रम स्थापित था। पालि-साहित्य के परिशीलन से पता चलता है कि बौद्धधर्म ने पब्बज्जा (प्रव्रज्या) की विधि ब्राह्मणधर्म से ही ग्रहण की थी।
मानव-जीवन के अस्तित्व के चार लक्ष्य माने गये हैं-धर्म, अर्थ काम एवं मोन। सर्वोत्तम लक्ष्य है मोक्ष, जिसे कई नामों से पुकारा जाता है, यथा मुक्ति, अमृतत्व, निःश्रेयस, कैवल्य (सांख्यों द्वारा) या अपवर्ग (न्यायसूत्र १।१।२)। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निर्वेद एवं वैराग्य (बृहदारण्यकोपनिषद् ५।१ या मुण्डकोपनिषद् ११२। १२) धारण करना चाहिए। भारतीय लेखकों ने अपने दिव्य दर्शन एवं प्रकाश के अनुसार आश्रमों के सिद्धान्त एवं व्यवहार के विषय में अपने मत दिये हैं । ब्रह्मचर्य में व्यक्ति को अनुशासन एवं संकल्प के अनुसार रहना पड़ता था, उसे अतीत काल के साहित्यिक भण्डार का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था, उसे आज्ञाकारिता, आदर, सादे जीवन एवं उच्च विचार के सद्गुण सीखने पड़ते थे। ब्रह्मचर्य के उपरान्त व्यक्ति विवाह करता था, गृहस्थ होता था, संसार के आनन्द का स्वाद लेता था, जीवन का उपभोग करता था, सन्तानोत्पत्ति करता था, अपनी सन्तानों, मित्रों, सम्बन्धियों, पड़ोसियों के प्रति अपने कर्तव्य करता था, उपयोगी, परिश्रमी एवं योग्य नागरिक होता था तथा एक कुल का संस्थापक होता था। ऐसा कहा गया है कि ५० वर्ष के लगभग की अवस्था हो जाने पर वह संसार के सुख एवं वासनाओं की भूख से ऊब उठता था तथा वन की राह ले लेता था, जहाँ वह आत्म-निग्रही, तपस्वी एवं निरपराध जीवन बिताता था। इसके उपरान्त संन्यास का आश्रम आता था। वह इसी जीवन में अन्तिम लक्ष्य (मोक्ष) प्राप्त कर सकता है, या इसी प्रकार के कई जीवनों तक वह चलता जायगा, जब तक कि उसे मुक्ति न प्राप्त हो जाय।
वर्ण का सिद्धान्त सम्पूर्ण समाज के लिए था, किन्तु आश्रम का सिद्धान्त व्यक्ति के लिए था। आर्य समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति के अधिकारों, कार्य-कलापों, स्वत्वों, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों की ओर संकेत करना वर्णसिद्धान्त का कार्य था। किन्तु आश्रम-सिद्धान्त यह बताता था कि व्यक्ति का आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, उसे अपने जीवन को किस प्रकार ले चलाना है तथा अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति में उसे क्या-क्या तैयारियां करनी है। निस्सन्देह, आश्रमसिद्धान्त एक उत्कृष्ट धारणा थी। भले ही यह भली भांति कार्यान्वित न की जा सकी, किन्तु इसके उद्देश्य बड़े ही महान् एवं विशिष्ट थे।
__ चारों आश्रमों के सम्बन्ध में तीन विभिन्न पक्षों की चर्चा की जाती है-समुच्चय, विकल्प एवं बाप। प्रथम पक्ष वाले कहते हैं कि प्रत्येक आश्रम का अनुसरण अनुक्रम से होता है, अर्थात् सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य, तब गृहस्थ और गृहस्थ के उपरान्त वानप्रस्थ और अन्त में संन्यास ; ऐसा नहीं है कि कोई एक या अधिक आश्रम को छोड़कर किसी अन्य को अपना ले, या संन्यासी हो जाने पर पुनः गृहस्थ हो जाय (दक्ष २८-९, वेदान्तसूत्र ३।४।४०) । इस पक्ष के अनुसार कोई
४. ब्रह्मचर्य परिसमाप्य गृही भवेद् गृही भूत्वा वनी भवेद्वनी भूत्वा प्रवजेत् । यदि बेतरपा ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेन् गृहावा वनाद्वा। यवहरेव विरजेत्तदहरेव प्रवजेत् । जाबालोप० ४। देखिए बौधायनधर्मसूक २०१०२ एवं १८.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org