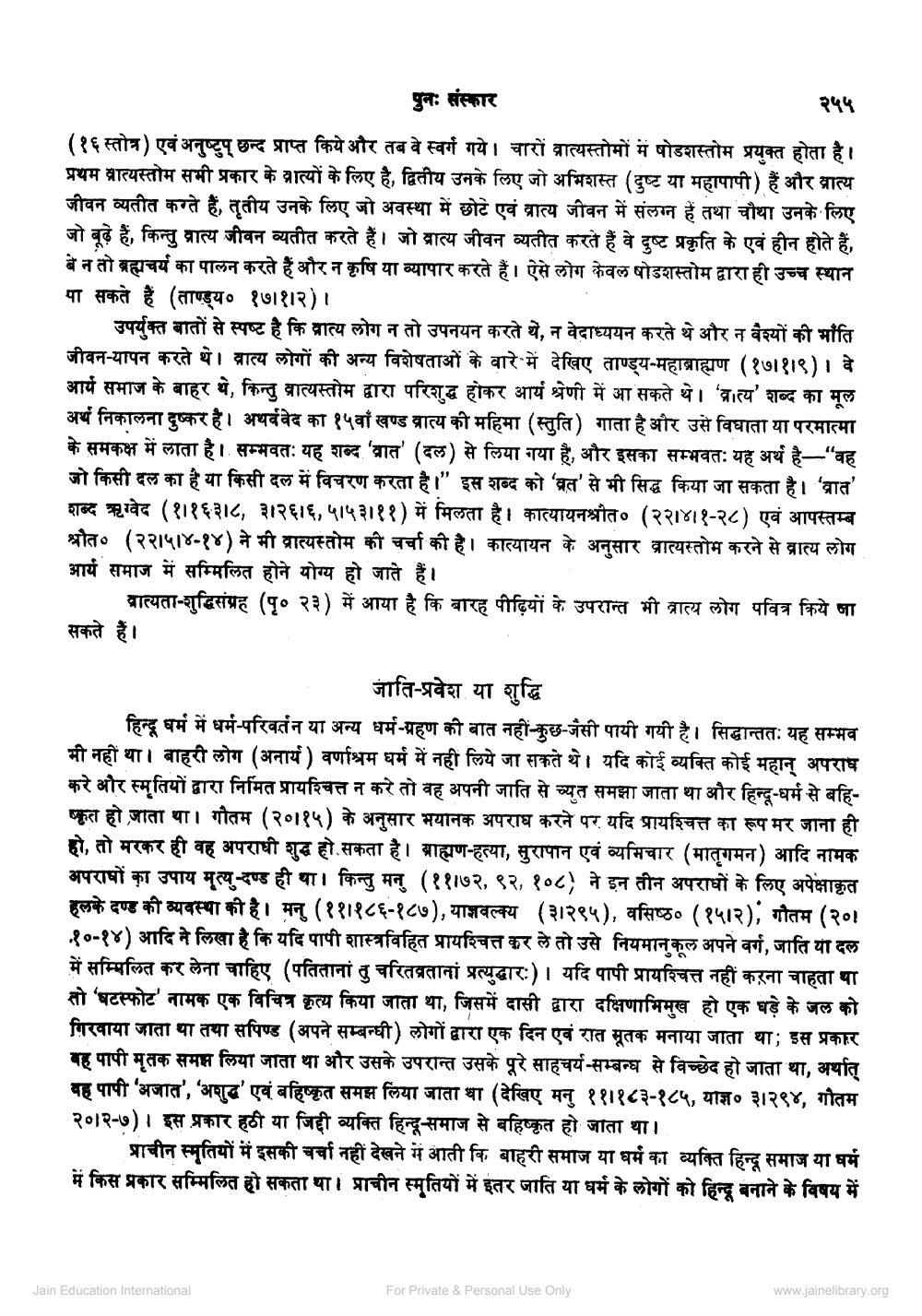________________
२५५
पुनः संस्कार (१६ स्तोत्र) एवं अनुष्टुप् छन्द प्राप्त किये और तब वे स्वर्ग गये। चारों व्रात्यस्तोमों में षोडशस्तोम प्रयुक्त होता है। प्रथम प्रात्यस्तोम सभी प्रकार के प्रात्यों के लिए है, द्वितीय उनके लिए जो अभिशस्त (दुष्ट या महापापी) हैं और व्रात्य जीवन व्यतीत करते हैं, तृतीय उनके लिए जो अवस्था में छोटे एवं व्रात्य जीवन में संलग्न हैं तथा चौथा उनके लिए जो बूढ़े हैं, किन्तु व्रात्य जीवन व्यतीत करते हैं। जो व्रात्य जीवन व्यतीत करते हैं वे दुष्ट प्रकृति के एवं हीन होते हैं, बे न तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और न कृषि या व्यापार करते हैं। ऐसे लोग केवल षोडशस्तोम द्वारा ही उच्च स्थान पा सकते हैं (ताण्ड्य० १७.१२)।
उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि व्रात्य लोग न तो उपनयन करते थे, न वेदाध्ययन करते थे और न वैश्यों की भांति जीवन-यापन करते थे। व्रात्य लोगों की अन्य विशेषताओं के बारे में देखिए ताण्ड्य-महाब्राह्मण (१७।११९)। वे आर्य समाज के बाहर थे, किन्तु व्रात्यस्तोम द्वारा परिशुद्ध होकर आर्य श्रेणी में आ सकते थे। 'वात्य' शब्द का मल अर्थ निकालना दुष्कर है। अथर्ववेद का १५वा खण्ड व्रात्य की महिमा (स्तुति) गाता है और उसे विधाता या परमात्मा के समकक्ष में लाता है। सम्भवतः यह शब्द 'वात' (दल) से लिया गया है, और इसका सम्भवतः यह अर्थ है-“वह जो किसी दल का है या किसी दल में विचरण करता है।" इस शब्द को 'व्रत' से भी सिद्ध किया जा सकता है। 'वात' शब्द ऋग्वेद (१३१६३।८, ३।२६।६, ५।५३।११) में मिलता है। कात्यायनीत० (२२।४।१-२८) एवं आपस्तम्ब श्रौत० (२२।५।४-१४) ने भी व्रात्यस्तोम की चर्चा की है। कात्यायन के अनुसार व्रात्यस्तोम करने से व्रात्य लोग आर्य समाज में सम्मिलित होने योग्य हो जाते हैं।
वात्यता-शुद्धिसंग्रह (पृ० २३) में आया है कि बारह पीढ़ियों के उपरान्त भी व्रात्य लोग पवित्र किये जा सकते हैं।
__ जाति-प्रवेश या शुद्धि हिन्दू धर्म में धर्म-परिवर्तन या अन्य धर्म-ग्रहण की बात नहीं-कुछ-जैसी पायी गयी है। सिद्धान्ततः यह सम्भव भी नहीं था। बाहरी लोग (अनार्य) वर्णाश्रम धर्म में नहीं लिये जा सकते थे। यदि कोई व्यक्ति कोई महान् अपराध करे और स्मतियों द्वारा निर्मित प्रायश्चित्त न करे तो वह अपनी जाति से च्यत समझा जाता था और हिन्दू-धर्म से बहिकृत हो जाता था। गौतम (२०१५) के अनुसार भयानक अपराध करने पर यदि प्रायश्चित्त का रूप मर जाना ही हो, तो मरकर ही वह अपराधी शुद्ध हो सकता है। ब्राह्मण-हत्या, सुरापान एवं व्यभिचार (मातृगमन) आदि नामक अपराधों का उपाय मृत्यु-दण्ड ही था। किन्तु मनु (११।७२, ९२, १०८) ने इन तीन अपराधों के लिए अपेक्षाकृत हलके दण्ड की व्यवस्था की है। मनु (१११८६-१८७), याज्ञवल्क्य (३।२९५), वसिष्ठ० (१५।२), गौतम (२०॥ १०-१४) आदि ने लिखा है कि यदि पापी शास्त्रविहित प्रायश्चित्त कर ले तो उसे नियमानुकूल अपने वर्ग, जाति या दल में सम्मिलित कर लेना चाहिए (पतितानां तु चरितव्रतानां प्रत्युद्धारः)। यदि पापी प्रायश्चित्त नहीं करना चाहता था सो 'घटस्फोट' नामक एक विचित्र कृत्य किया जाता था, जिसमें दासी द्वारा दक्षिणाभिमुख हो एक घड़े के जल को गिरवाया जाता था तथा सपिण्ड (अपने सम्बन्धी) लोगों द्वारा एक दिन एवं रात सूतक मनाया जाता था; इस प्रकार बह पापी मृतक समझ लिया जाता था और उसके उपरान्त उसके पूरे साहचर्य-सम्बन्ध से विच्छेद हो जाता था, अर्थात् वह पापी 'अजात', 'अशुद्ध' एवं बहिष्कृत समझ लिया जाता था (देखिए मनु १११८३-१८५, याज्ञ० ३।२९४, गौतम २०१२-७)। इस प्रकार हठी या जिद्दी व्यक्ति हिन्दू-समाज से बहिष्कृत हो जाता था।
प्राचीन स्मृतियों में इसकी चर्चा नहीं देखने में आती कि बाहरी समाज या धर्म का व्यक्ति हिन्दू समाज या धर्म में किस प्रकार सम्मिलित हो सकता था। प्राचीन स्मृतियों में इतर जाति या धर्म के लोगों को हिन्दू बनाने के विषय में
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org