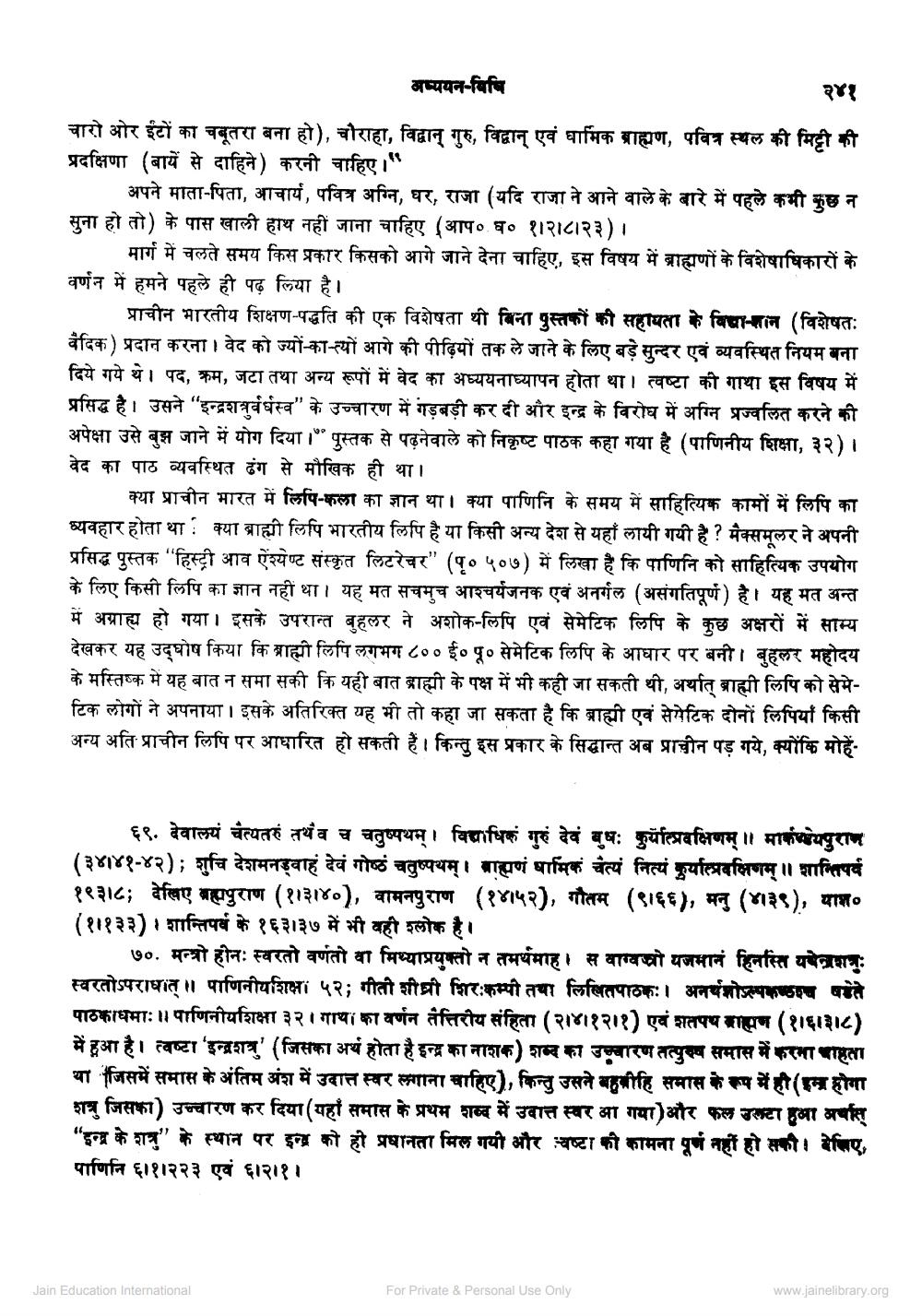________________
अध्ययन-विषि
२४१ चारो ओर ईंटों का चबूतरा बना हो), चौराहा, विद्वान् गुरु, विद्वान् एवं धार्मिक ब्राह्मण, पवित्र स्थल की मिट्टी की प्रदक्षिणा ( बायें से दाहिने) करनी चाहिए ।"
अपने माता-पिता, आचार्य, पवित्र अग्नि, घर, राजा (यदि राजा ने आने वाले के बारे में पहले कभी कुछ न सुना हो तो) के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ( आप० ६० ११२८/२३ ) ।
मार्ग में चलते समय किस प्रकार किसको आगे जाने देना चाहिए, इस विषय में ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के वर्णन में हमने पहले ही पढ़ लिया है।
प्राचीन भारतीय शिक्षण-पद्धति की एक विशेषता थी बिना पुस्तकों की सहायता के विद्या-ज्ञान (विशेषतः वैदिक) प्रदान करना । वेद को ज्यों-का-त्यों आगे की पीढ़ियों तक ले जाने के लिए बड़े सुन्दर एवं व्यवस्थित नियम बना दिये गये थे । पद, क्रम, जटा तथा अन्य रूपों में वेद का अध्ययनाध्यापन होता था । त्वष्टा की गाथा इस विषय में प्रसिद्ध है। उसने “इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व" के उच्चारण में गड़बड़ी कर दी और इन्द्र के विरोध में अग्नि प्रज्वलित करने की अपेक्षा उसे बुझ जाने में योग दिया।" पुस्तक से पढ़नेवाले को निकृष्ट पाठक कहा गया है (पाणिनीय शिक्षा, ३२) । वेद का पाठ व्यवस्थित ढंग से मौखिक ही था ।
क्या प्राचीन भारत में लिपि कला का ज्ञान था। क्या पाणिनि के समय में साहित्यिक कामों में लिपि का व्यवहार होता था? क्या ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपि है या किसी अन्य देश से यहाँ लायी गयी है ? मैक्समूलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "हिस्ट्री आव ऐंश्येण्ट संस्कृत लिटरेचर" ( पृ० ५०७ ) में लिखा है कि पाणिनि को साहित्यिक उपयोग के लिए किसी लिपि का ज्ञान नहीं था । यह मत सचमुच आश्चर्यजनक एवं अनर्गल (असंगतिपूर्ण) है। यह मत अन्त में अग्राह्य हो गया। इसके उपरान्त बुहलर ने अशोक - लिपि एवं सेमेटिक लिपि के कुछ अक्षरों में साम्य देखकर यह उद्घोष किया कि ब्राह्मी लिपि लगभग ८०० ई० पू० सेमेटिक लिपि के आधार पर बनी । बुहलर महोदय के मस्तिष्क में यह बात न समा सकी कि यही बात ब्राह्मी के पक्ष में भी कही जा सकती थी, अर्थात् ब्राह्मी लिपि को सेमेटिक लोगों ने अपनाया। इसके अतिरिक्त यह भी तो कहा जा सकता है कि ब्राह्मी एवं सेमेटिक दोनों लिपियाँ किसी अन्य अति प्राचीन लिपि पर आधारित हो सकती हैं। किन्तु इस प्रकार के सिद्धान्त अब प्राचीन पड़ गये, क्योंकि मोहें
६९. देवालयं चैत्यतरुं तथैव च चतुष्पथम् । विद्याधिकं गुरुं देवं बुधः कुर्यात्प्रदक्षिणम् ॥ मार्कण्डेयपुरान ( ३४०४१-४२ ); शुचि देशमनड्वाहं देवं गोष्ठं चतुष्पथम् । ब्राह्मणं धार्मिक चैत्यं नित्यं कुर्यात्प्रदक्षिणम् ॥ शान्तिपर्व १९३८; देखिए ब्रह्मपुराण ( १।३।४० ), वामनपुराण (१४|५२), गौतम ( ९/६६ ), मनु ( ४१३९), याश० (१०१३३) । शान्तिपर्व के १६३।३७ में भी वही श्लोक है।
७०. मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वत्रो यजमानं हिनस्ति यचेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ॥ पाणिनीयशिक्ष। ५२; गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः । अनर्थशोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः ॥ पाणिनीयशिक्षा ३२ | गाथा का वर्णन तैत्तिरीय संहिता ( २।४।१२।१) एवं शतपथ ब्राह्मण (१२६०३०८) में हुआ है। त्वष्टा 'इन्द्रशत्रु' (जिसका अर्थ होता है इन्द्र का नाशक) शब्द का उच्चारण तत्पुरुष समास में करना चाहता था जिसमें समास के अंतिम अंश में उदात्त स्वर लगाना चाहिए), किन्तु उसने बहुब्रीहि समास के रूप में ही (इन्द्र होगा शत्रु जिसका) उच्चारण कर दिया (यहाँ समास के प्रथम शब्द में उदात्त स्वर आ गया) और फल उलटा हुआ अर्थात् "इन्द्र के शत्रु " के स्थान पर इन्द्र को ही प्रधानता मिल गयी और स्वष्टा की कामना पूर्ण नहीं हो सकी। देखिए, पाणिनि ६।१।२२३ एवं ६।२।१ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org