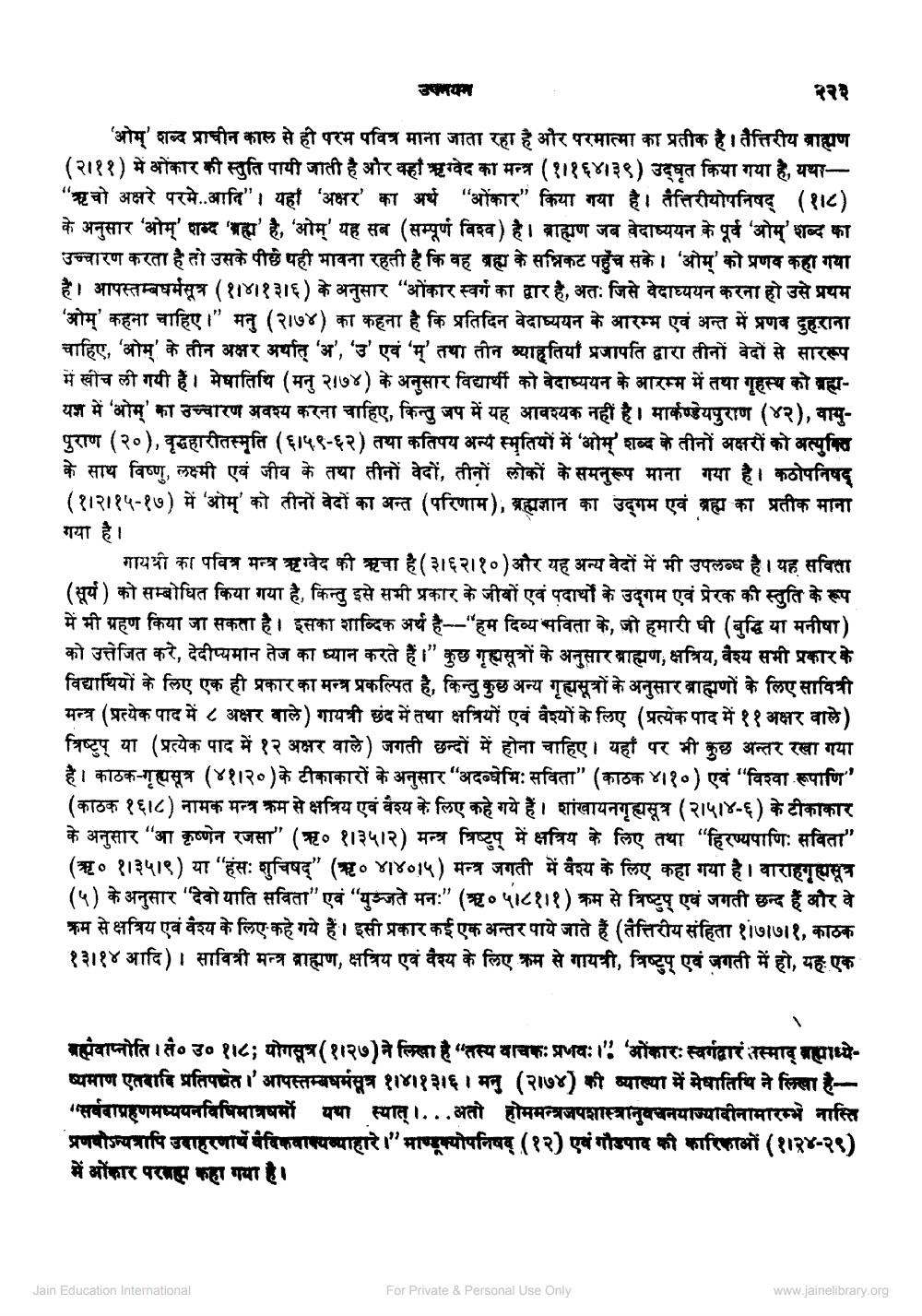________________
उपनयन
ዝቅ 'ओम्' शब्द प्राचीन काल से ही परम पवित्र माना जाता रहा है और परमात्मा का प्रतीक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२०११) में ओंकार की स्तुति पायी जाती है और वहाँ ऋग्वेद का मन्त्र (१।१६४।३९) उद्धृत किया गया है, यथा"ऋचो अक्षरे परमे..आनि"। यहाँ 'अक्षर' का अर्थ “ओंकार" किया गया है। तैत्तिरीयोपनिषद् (१।८) के अनुसार 'ओम्' शब्द 'ब्रह्म' है, 'ओम्' यह सब (सम्पूर्ण विश्व) है। ब्राह्मण जब वेदाध्ययन के पूर्व 'ओम्' शब्द का उच्चारण करता है तो उसके पीछे यही भावना रहती है कि वह ब्रह्म के सन्निकट पहुंच सके। 'ओम्' को प्रणव कहा गया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१३।६) के अनुसार “ओंकार स्वर्ग का द्वार है, अतः जिसे वेदाध्ययन करना हो उसे प्रथम 'ओम्' कहना चाहिए।" मनु (२।७४) का कहना है कि प्रतिदिन वेदाध्ययन के आरम्भ एवं अन्त में प्रणव दुहराना चाहिए, 'ओम्' के तीन अक्षर अर्थात् 'अ', 'उ' एवं 'म्' तथा तीन व्याहृतियाँ प्रजापति द्वारा तीनों वेदों से साररूप में खींच ली गयी हैं। मेषातिथि (मनु २१७४) के अनुसार विद्यार्थी को वेदाध्ययन के आरम्भ में तथा गृहस्थ को ब्रह्मयज्ञ में 'ओम्' का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, किन्तु जप में यह आवश्यक नहीं है। मार्कण्डेयपुराण (४२), वायुपुराण (२०), वृद्धहारीतस्मृति (६।५९-६२) तथा कतिपय अन्य स्मृतियों में 'ओम्' शब्द के तीनों अक्षरों को अत्युक्ति के साथ विष्णु, लक्ष्मी एवं जीव के तथा तीनों वेदों, तीनों लोकों के समनुरूप माना गया है। कठोपनिषद् (१।२।१५-१७) में 'ओम्' को तीनों वेदों का अन्त (परिणाम), ब्रह्मज्ञान का उद्गम एवं ब्रह्म का प्रतीक माना गया है।
___गायत्री का पवित्र मन्त्र ऋग्वेद की ऋचा है (३।६२।१०) और यह अन्य वेदों में भी उपलब्ध है। यह सविता (सूर्य) को सम्बोधित किया गया है, किन्तु इसे सभी प्रकार के जीवों एवं पदार्थों के उद्गम एवं प्रेरक की स्तुति के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ है--"हम दिव्य पविता के, जो हमारी घी (बुद्धि या मनीषा) को उत्तेजित करे, देदीप्यमान तेज का ध्यान करते हैं।" कुछ गृह्यसूत्रों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार का मन्त्र प्रकल्पित है, किन्तु कुछ अन्य गृह्यसूत्रों के अनुसार ब्राह्मणों के लिए सावित्री मन्त्र (प्रत्येक पाद में ८ अक्षर वाले) गायत्री छंद में तथा क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए (प्रत्येक पाद में ११ अक्षर वाले) त्रिष्टुप् या (प्रत्येक पाद में १२ अक्षर वाले) जगती छन्दों में होना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ अन्तर रखा गया है। काठक-गृह्यसूत्र (४१।२०) के टीकाकारों के अनुसार “अदब्धेमिः सविता" (काठक ४।१०) एवं “विश्वा रूपाणि" (काठक १६१८) नामक मन्त्र क्रम से क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए कहे गये हैं। शांखायनगृह्यसूत्र (२।५।४-६) के टीकाकार के अनुसार “आ कृष्णेन रजसा" (ऋ० ११३५।२) मन्त्र त्रिष्टुप् में क्षत्रिय के लिए तथा “हिरण्यपाणिः सविता" (ऋ० १।३५।९) या "हंसः शुचिषद्” (ऋ० ४।४०१५) मन्त्र जगती में वैश्य के लिए कहा गया है। वाराहगृह्यसूत्र (५) के अनुसार "देवो याति सविता" एवं “युञ्जते मनः" (ऋ० ५।८१३१) क्रम से त्रिष्टुप् एवं जगती छन्द हैं और वे क्रम से क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए कहे गये हैं। इसी प्रकार कई एक अन्तर पाये जाते हैं (तैत्तिरीय संहिता १७७४१, काठक १३॥१४ आदि)। सावित्री मन्त्र ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रम से गायत्री, त्रिष्टुप् एवं जगती में हो, यह एक
ब्रह्मवाप्नोति । से० उ० ११८; योगसूत्र (१२७) ने लिखा है "तस्य वाचकः प्रणवः।' 'ओंकारः स्वर्गद्वारं तस्माद् ब्रह्माध्येष्यमाण एतवावि प्रतिपचेत।' आपस्तम्बधर्मसूत्र १०४१३३६ । मनु (२०७४) की व्याख्या में मेधातिथि ने लिखा है"सर्वदामहणमध्ययनविषिमात्रधर्मों यथा स्यात् ।...अतो होममन्त्रजपशास्त्रानुवचनयाज्यावीनामारम्भे नास्ति प्रणयोग्यत्रापि उदाहरणार्ये वैविकवास्यव्याहारे।" माण्डूक्योपनिषद् (१२) एवं गौडपाद की कारिकाओं (११२४-२९) में ओंकार परब्रह्म कहा गया है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org