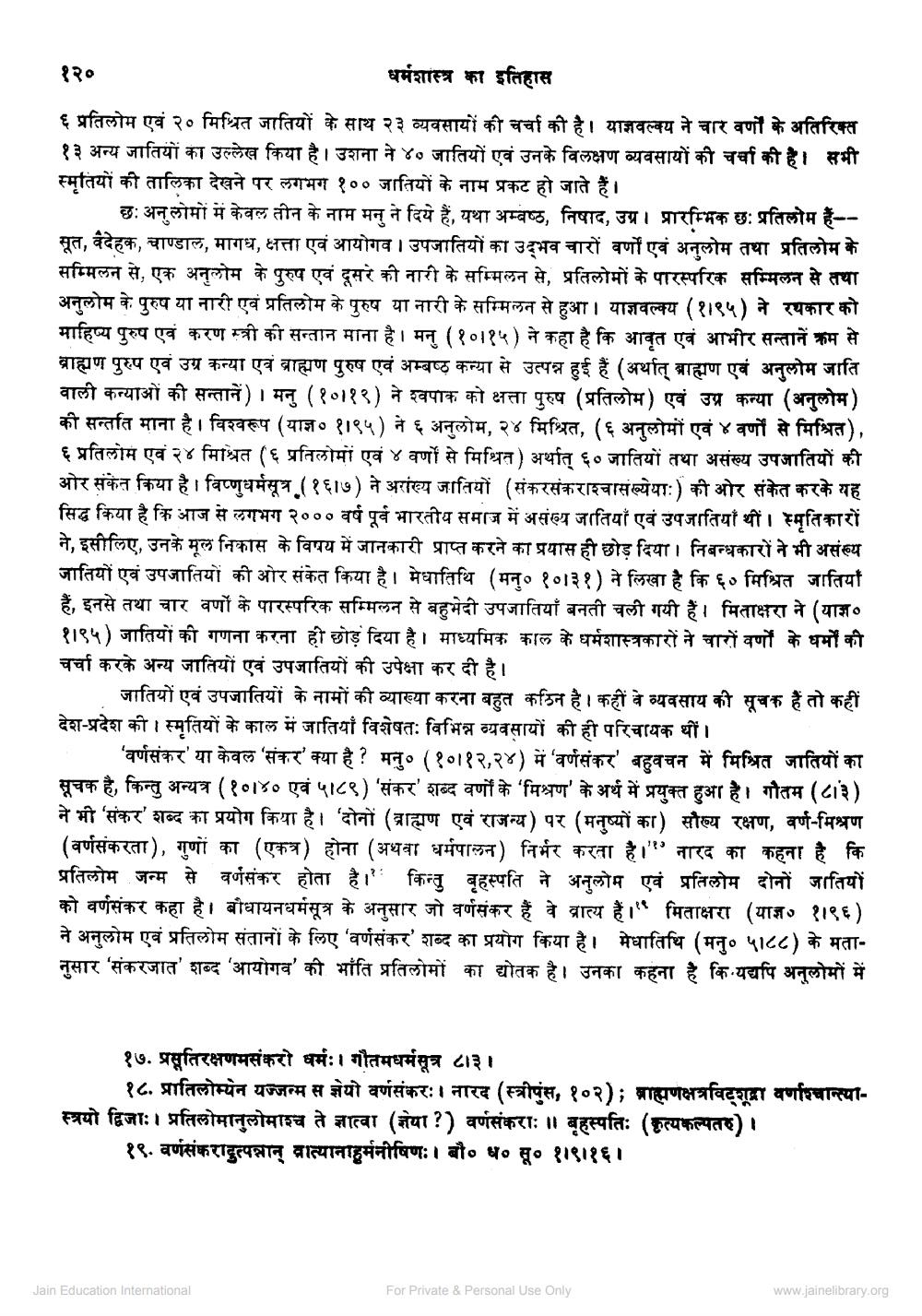________________
१२०
धर्मशास्त्र का इतिहास ६ प्रतिलोम एवं २० मिश्रित जातियों के साथ २३ व्यवसायों की चर्चा की है। याज्ञवल्क्य ने चार वर्गों के अतिरिक्त १३ अन्य जातियों का उल्लेख किया है। उशना ने ४० जातियों एवं उनके विलक्षण व्यवसायों की चर्चा की है। सभी स्मतियों की तालिका देखने पर लगभग १०० जातियों के नाम प्रकट हो जाते हैं।
____ छ: अनुलोमों में केवल तीन के नाम मनु ने दिये हैं, यथा अम्बष्ठ, निषाद, उग्र। प्रारम्भिक छ: प्रतिलोम हैं-- सूत, वैदेहक, चाण्डाल, मागध, क्षत्ता एवं आयोगव । उपजातियों का उद्भव चारों वर्णों एवं अनुलोम तथा प्रतिलोम के सम्मिलन से, एक अनुलोम के पुरुष एवं दूसरे की नारी के सम्मिलन से, प्रतिलोमों के पारस्परिक सम्मिलन से तथा अनुलोम के पुरुष या नारी एवं प्रतिलोम के पुरुष या नारी के सम्मिलन से हुआ। याज्ञवल्क्य (१२९५) ने रथकार को माहिष्य पुरुष एवं करण स्त्री की सन्तान माना है। मनु (१०।१५) ने कहा है कि आवृत एवं आभीर सन्ताने क्रम से ब्राह्मण पुरुप एवं उग्र कन्या एवं ब्राह्मण पुरुष एवं अम्बष्ठ कन्या से उत्पन्न हुई हैं (अर्थात् ब्राह्मण एवं अनुलोम जाति वाली कन्याओं की सन्तानें)। मनु (१०११९) ने श्वपाक को क्षत्ता पुरुष (प्रतिलोम) एवं उग्र कन्या (अनुलोम) की सन्तति माना है। विश्वरूप (याज्ञ० १।९५) ने ६ अनुलोम, २४ मिश्रित, (६ अनुलोमों एवं ४ वर्णों से मिश्रित), ६ प्रतिलोम एवं २४ मिाश्रत (६ प्रतिलोमों एवं ४ वर्णों से मिश्रित) अर्थात् ६० जातियों तथा असंख्य उपजातियों की ओर संकेत किया है। विष्णुधर्मसूत्र (१६।७) ने असंख्य जातियों (संकरसंकराश्चासंख्येयाः) की ओर संकेत करके यह सिद्ध किया है कि आज से लगभग २००० वर्ष पूर्व भारतीय समाज में असंख्य जातियाँ एवं उपजातियाँ थीं। स्मृतिकारों ने, इसीलिए, उनके मूल निकास के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास ही छोड़ दिया। निबन्धकारों ने भी असंख्य जातियों एवं उपजातियों की ओर संकेत किया है। मेधातिथि (मनु० १०॥३१) ने लिखा है कि ६० मिश्रित जातियाँ हैं, इनसे तथा चार वर्गों के पारस्परिक सम्मिलन से बहुभेदी उपजातियाँ बनती चली गयी हैं। मिताक्षरा ने (याज्ञ० १२९५) जातियों की गणना करना ही छोड़ दिया है। माध्यमिक काल के धर्मशास्त्रकारों ने चारों वर्गों के धर्मों की चर्चा करके अन्य जातियों एवं उपजातियों की उपेक्षा कर दी है।
जातियों एवं उपजातियों के नामों की व्याख्या करना बहुत कठिन है। कहीं वे व्यवसाय की सूचक हैं तो कहीं देश-प्रदेश की। स्मृतियों के काल में जातियाँ विशेषतः विभिन्न व्यवसायों की ही परिचायक थीं।
'वर्णसंकर' या केवल 'संकर' क्या है ? मनु० (१०।१२,२४) में 'वर्णसंकर' बहुवचन में मिश्रित जातियों का सूचक है, किन्तु अन्यत्र (१०।४० एवं ५।८९) 'संकर' शब्द वर्गों के 'मिश्रण' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। गौतम (८३) ने भी 'संकर' शब्द का प्रयोग किया है। दोनों (ब्राह्मण एवं राजन्य) पर (मनुष्यों का) सौख्य रक्षण, वर्ण-मिश्रण (वर्णसंकरता), गुणों का (एकत्र) होना (अथवा धर्मपालन) निर्भर करता है। नारद का कहना है कि प्रतिलोम जन्म से वर्णसंकर होता है। किन्तु बृहस्पति ने अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों जातियों को वर्णसंकर कहा है। बौधायनधर्मसूत्र के अनुसार जो वर्णसंकर हैं वे व्रात्य हैं।" मिताक्षरा (याज्ञ. १८९६) ने अनुलोम एवं प्रतिलोम संतानों के लिए 'वर्णसंकर' शब्द का प्रयोग किया है। मेधातिथि (मनु० ५।८८) के मतानुसार 'संकरजात' शब्द 'आयोगव' की भाँति प्रतिलोमों का द्योतक है। उनका कहना है कि यद्यपि अनुलोमों में
१७. प्रसूतिरक्षणमसंकरो धर्मः। गौतमधर्मसूत्र ८।३।
१८. प्रातिलोम्येन यज्जन्म स ज्ञेयो वर्णसंकरः । नारद (स्त्रीपुंस, १०२); ब्राह्मणक्षत्रविट्शूद्रा वर्णाश्चान्स्यास्त्रयो द्विजाः। प्रतिलोमानुलोमाश्च ते ज्ञात्वा (जेया ?) वर्णसंकराः ॥ बृहस्पतिः (कृत्यकल्पतरु)।
१९. वर्णसंकरादुत्पन्नान् वात्यानाहुर्मनीषिणः। बौ० ५० सू० १।९।१६।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org