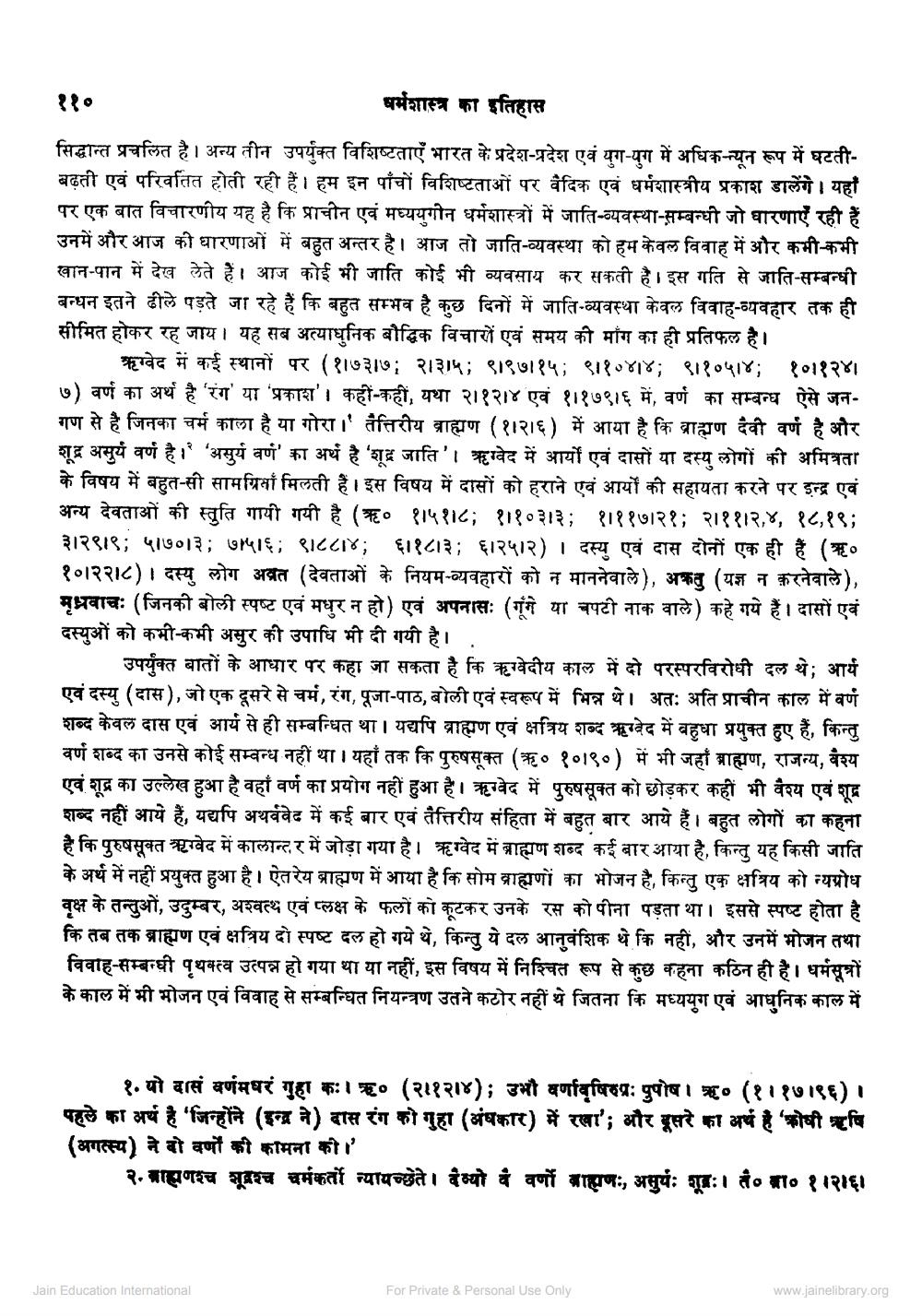________________
११०
धर्मशास्त्र का इतिहास सिद्धान्त प्रचलित है। अन्य तीन उपर्युक्त विशिष्टताएँ भारत के प्रदेश-प्रदेश एवं युग-युग में अधिक न्यून रूप में घटतीबढ़ती एवं परिवर्तित होती रही हैं। हम इन पांचों विशिष्टताओं पर वैदिक एवं धर्मशास्त्रीय प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर एक बात विचारणीय यह है कि प्राचीन एवं मध्ययुगीन धर्मशास्त्रों में जाति-व्यवस्था-सम्बन्धी जो धारणाएं रही हैं उनमें और आज की धारणाओं में बहुत अन्तर है। आज तो जाति-व्यवस्था को हम केवल विवाह में और कभी-कभी खान-पान में देख लेते हैं। आज कोई भी जाति कोई भी व्यवसाय कर सकती है। इस गति से जाति-सम्बन्धी बन्धन इतने ढीले पड़ते जा रहे हैं कि बहुत सम्भव है कुछ दिनों में जाति-व्यवस्था केवल विवाह-व्यवहार तक ही सीमित होकर रह जाय। यह सब अत्याधुनिक बौद्धिक विचारों एवं समय की माँग का ही प्रतिफल है।
ऋग्वेद में कई स्थानों पर (११७३।७; २।३।५; ९।९७।१५; ९।१०४।४; ९।१०५।४; १०११२४। ७) वर्ण का अर्थ है 'रंग' या 'प्रकाश'। कहीं-कहीं, यथा २।१२।४ एवं १३१७९१६ में, वर्ण का सम्बन्ध ऐसे जनगण से है जिनका चर्म काला है या गोरा।' तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।२।६) में आया है कि ब्राह्मण देवी वर्ण है और शूद्र असुर्य वर्ण है। 'असुर्य वर्ण' का अर्थ है 'शूद्र जाति'। ऋग्वेद में आर्यों एवं दासों या दस्यु लोगों की अमित्रता के विषय में बहुत-सी सामग्रियां मिलती हैं। इस विषय में दासों को हराने एवं आर्यों की सहायता करने पर इन्द्र एवं अन्य देवताओं की स्तुति गायी गयी है (ऋ० ११५१३८; १।१०३।३; १।११७।२१, २।११।२,४, १८,१९; ३।२९।९; ५।७०।३; ७५।६, ९।८८।४; ६।१८।३; ६।२५।२) । दस्यु एवं दास दोनों एक ही हैं (ऋ० १०।२२।८)। दस्यु लोग अव्रत (देवताओं के नियम-व्यवहारों को न माननेवाले), अऋतु (यज्ञ न करनेवाले), मृध्रवाचः (जिनकी बोली स्पष्ट एवं मधुर न हो) एवं अपनासः (गूंगे या चपटी नाक वाले) कहे गये हैं। दासों एवं दस्युओं को कभी-कभी असुर की उपाधि भी दी गयी है। .
उपर्युक्त बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋग्वेदीय काल में दो परस्परविरोधी दल थे; आर्य एवं दस्यु (दास), जो एक दूसरे से चर्म, रंग, पूजा-पाठ, बोली एवं स्वरूप में भिन्न थे। अतः अति प्राचीन काल में वर्ण शब्द केवल दास एवं आर्य से ही सम्बन्धित था। यद्यपि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय शब्द ऋग्वेद में बहुधा प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु वर्ण शब्द का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं था। यहाँ तक कि पुरुषसूक्त (ऋ० १०१९०) में भी जहाँ ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख हुआ है वहाँ वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऋग्वेद में पुरुषसूक्त को छोड़कर कहीं भी वैश्य एवं शूद्र शब्द नहीं आये हैं, यद्यपि अथर्ववेद में कई बार एवं तैत्तिरीय संहिता में बहुत बार आये हैं। बहुत लोगों का कहना है कि पुरुषसूक्त ऋग्वेद में कालान्तर में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द कई बार आया है, किन्तु यह किसी जाति के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में आया है कि सोम ब्राह्मणों का भोजन है, किन्तु एक क्षत्रिय को न्यग्रोध वृक्ष के तन्तुओं, उदुम्बर, अश्वत्थ एवं प्लक्ष के फलों को कूटकर उनके रस को पीना पड़ता था। इससे स्पष्ट होता है कि तब तक ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दो स्पष्ट दल हो गये थे, किन्तु ये दल आनुवंशिक थे कि नहीं, और उनमें भोजन तथा विवाह-सम्बन्धी पृथक्त्व उत्पन्न हो गया था या नहीं, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन ही है। धर्मसूत्रों के काल में भी भोजन एवं विवाह से सम्बन्धित नियन्त्रण उतने कठोर नहीं थे जितना कि मध्ययुग एवं आधुनिक काल में
१. यो दासं वर्णमघरं गुहा कः। ऋ० (२।१२।४); उभौ वर्णावृषिकप्रः पुपोष। ऋ० (१।१७।९६)। पहले का अर्थ है "जिन्होंने (इन्द्र ने) दास रंग को गुहा (अंधकार) में रखा'; और दूसरे का अर्थ है 'क्रोषी ऋषि (अगत्स्य) ने दो वर्षों की कामना की।
२. ब्राह्मणश्च भूवश्च चर्मकर्ता न्यायच्छेते। देन्यो वै वर्गों ब्राह्मणः, असुर्यः शूद्धः। ते बा० ११२१६
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org