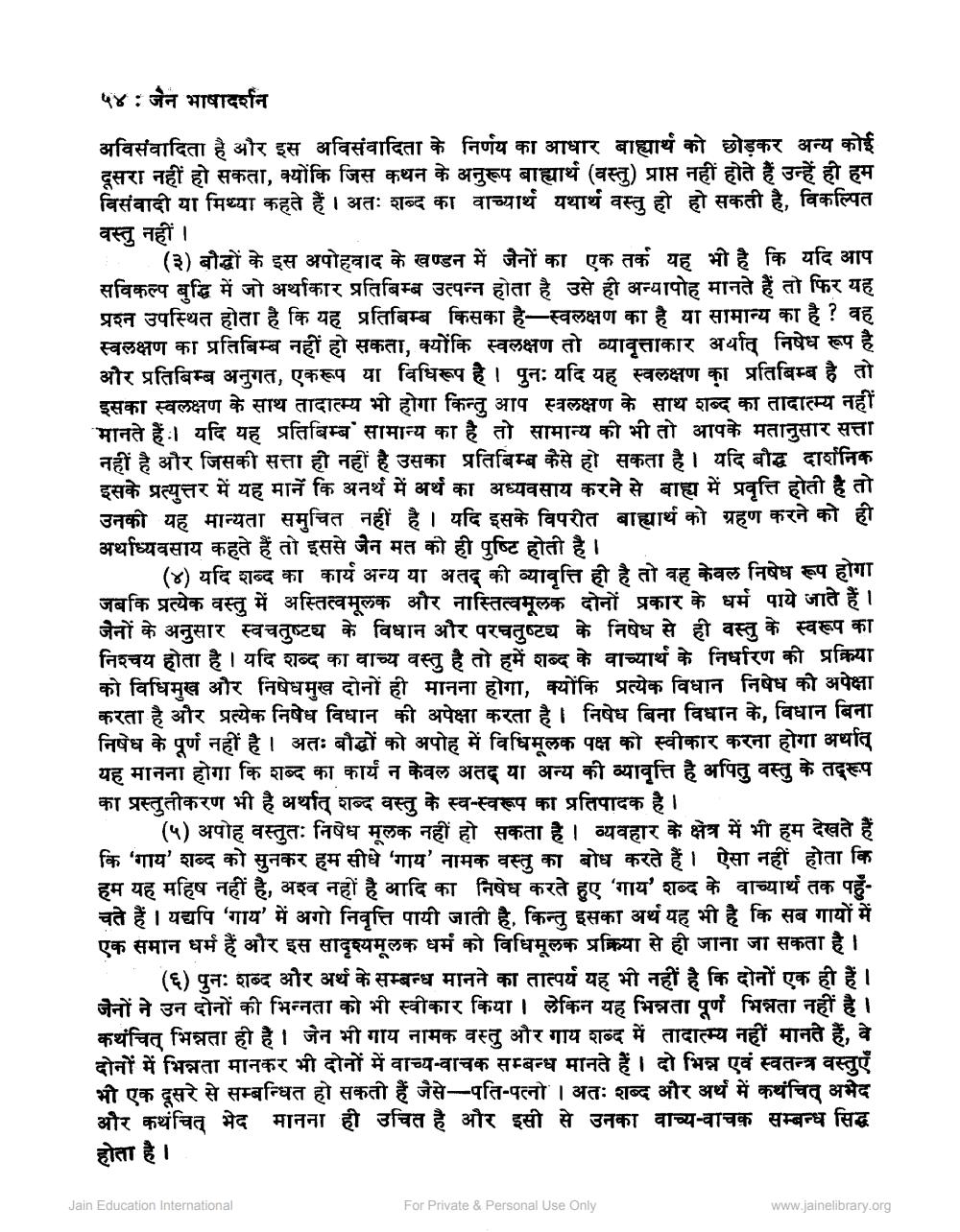________________
५४ : जैन भाषादर्शन
अविसंवादिता है और इस अविसंवादिता के निर्णय का आधार बाह्यार्थ को छोड़कर अन्य कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस कथन के अनुरूप बाह्यार्थ (वस्तु) प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें ही हम विसंवादी या मिथ्या कहते हैं । अतः शब्द का वाच्यार्थ यथार्थं वस्तु हो हो सकती है, विकल्पित वस्तु नहीं ।
(३) बौद्धों के इस अपोहवाद के खण्डन में जैनों का एक तर्क यह भी है कि यदि आप सविकल्प बुद्धि में जो अर्थाकार प्रतिबिम्ब उत्पन्न होता है उसे ही अन्यापोह मानते हैं तो फिर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह प्रतिबिम्ब किसका है - स्वलक्षण का है या सामान्य का है ? वह स्वलक्षण का प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता, क्योंकि स्वलक्षण तो व्यावृत्ताकार अर्थात् निषेध रूप है और प्रतिबिम्ब अनुगत, एकरूप या विधिरूप है । पुनः यदि यह स्वलक्षण का प्रतिबिम्ब है तो इसका स्वलक्षण के साथ तादात्म्य भी होगा किन्तु आप स्वलक्षण के साथ शब्द का तादात्म्य नहीं मानते हैं । यदि यह प्रतिबिम्ब सामान्य का है तो सामान्य की भी तो आपके मतानुसार सत्ता नहीं है और जिसकी सत्ता ही नहीं है उसका प्रतिबिम्ब कैसे हो सकता है। यदि बौद्ध दार्शनिक इसके प्रत्युत्तर में यह मानें कि अनर्थ में अर्थ का अध्यवसाय करने से बाह्य में प्रवृत्ति होती है तो उनकी यह मान्यता समुचित नहीं है । यदि इसके विपरीत बाह्यार्थ को ग्रहण करने को ही अर्थाध्यवसाय कहते हैं तो इससे जैन मत को ही पुष्टि होती है ।
(४) यदि शब्द का कार्य अन्य या अतद् की व्यावृत्ति ही है तो वह केवल निषेध रूप होगा जबकि प्रत्येक वस्तु में अस्तित्वमूलक और नास्तित्वमूलक दोनों प्रकार के धर्म पाये जाते हैं । जैनों के अनुसार स्वचतुष्टय के विधान और परचतुष्टय के निषेध से ही वस्तु के स्वरूप का निश्चय होता है । यदि शब्द का वाच्य वस्तु है तो हमें शब्द के वाच्यार्थ के निर्धारण की प्रक्रिया को विधिमुख और निषेधमुख दोनों ही मानना होगा, क्योंकि प्रत्येक विधान निषेध की अपेक्षा करता है और प्रत्येक निषेध विधान की अपेक्षा करता है । निषेध बिना विधान के, विधान बिना निषेध के पूर्ण नहीं है । अतः बौद्धों को अपोह में विधिमूलक पक्ष को स्वीकार करना होगा अर्थात् यह मानना होगा कि शब्द का कार्य न केवल अतद् या अन्य की व्यावृत्ति है अपितु वस्तु के तद्रूप का प्रस्तुतीकरण भी है अर्थात् शब्द वस्तु के स्व-स्वरूप का प्रतिपादक है।
(५) अपोह वस्तुतः निषेध मूलक नहीं हो सकता है । व्यवहार के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि 'गाय' शब्द को सुनकर हम सीधे 'गाय' नामक वस्तु का बोध करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम यह महिष नहीं है, अश्व नहीं है आदि का निषेध करते हुए 'गाय' शब्द के वाच्यार्थ तक पहुँचते हैं | यद्यपि 'गाय' में अगो निवृत्ति पायी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह भी है कि सब गायों में एक समान धर्म हैं और इस सादृश्यमूलक धर्मं को विधिमूलक प्रक्रिया से ही जाना जा सकता है । (६) पुन: शब्द और अर्थ के सम्बन्ध मानने का तात्पर्य यह भी नहीं है कि दोनों एक ही हैं। जैनों ने उन दोनों की भिन्नता को भी स्वीकार किया। लेकिन यह भिन्नता पूर्ण भिन्नता नहीं है । कथंचित् भिन्नता ही है । जैन भी गाय नामक वस्तु और गाय शब्द में तादात्म्य नहीं मानते हैं, वे दोनों में भिन्नता मानकर भी दोनों में वाच्य वाचक सम्बन्ध मानते हैं । दो भिन्न एवं स्वतन्त्र वस्तुएँ भी एक दूसरे से सम्बन्धित हो सकती हैं जैसे - पति - पत्नी । अतः शब्द और अर्थ में कथंचित् अभेद और कथंचित् भेद मानना ही उचित है और इसी से उनका वाच्य वाचक सम्बन्ध सिद्ध होता है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org