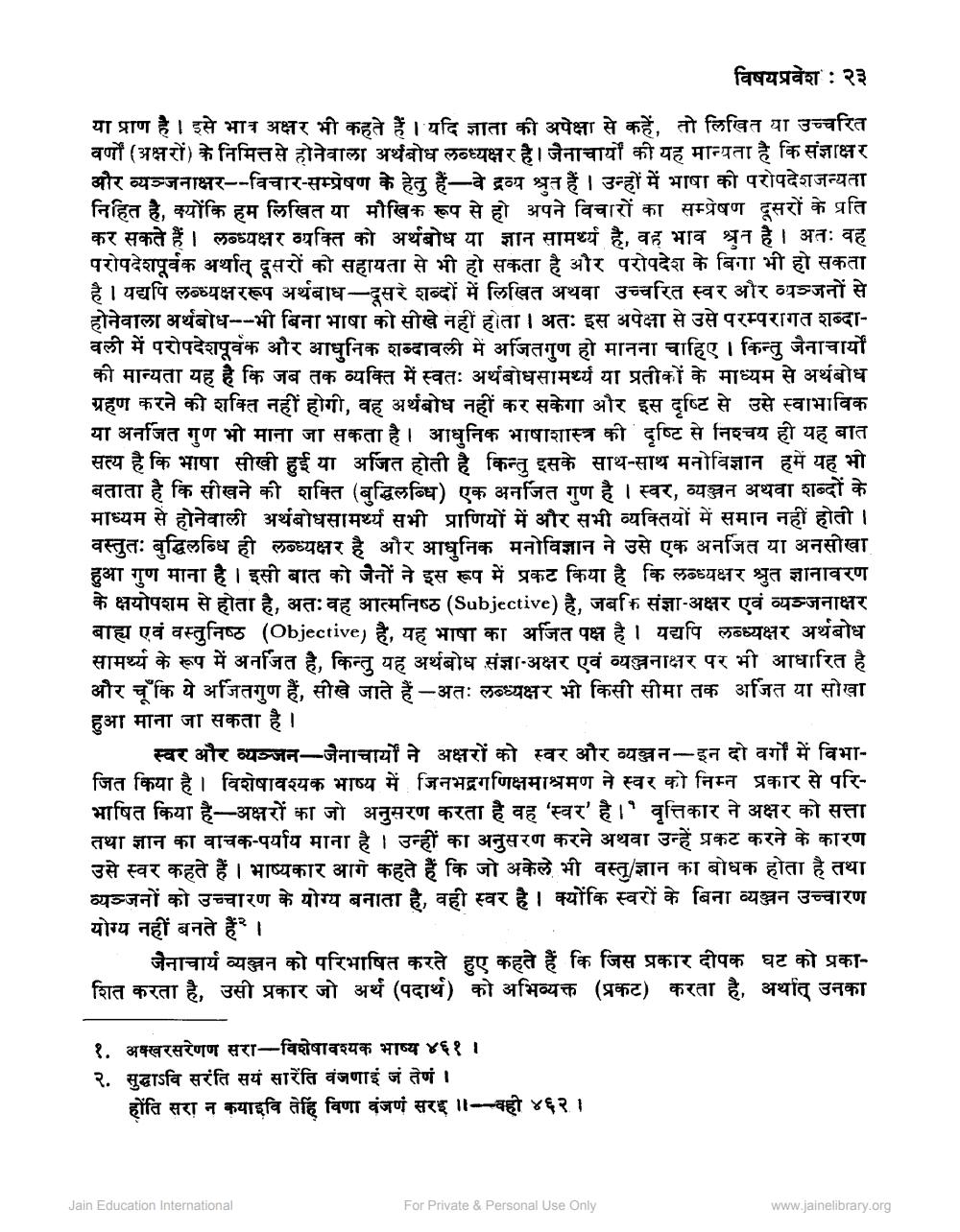________________
विषयप्रवेश : २३
या प्राण है। इसे भाव अक्षर भी कहते हैं। यदि ज्ञाता की अपेक्षा से कहें, तो लिखित या उच्चरित वर्णों (अक्षरों) के निमित्तसे होनेवाला अर्थबोध लब्ध्यक्षर है। जैनाचार्यों की यह मान्यता है कि संज्ञाक्षर
और व्यञ्जनाक्षर--विचार-सम्प्रेषण के हेतु हैं-वे द्रव्य श्रुत हैं । उन्हों में भाषा को परोपदेशजन्यता निहित है, क्योंकि हम लिखित या मौखिक रूप से हो अपने विचारों का सम्प्रेषण दूसरों के प्रति कर सकते हैं। लब्ध्यक्षर व्यक्ति को अर्थबोध या ज्ञान सामर्थ्य है, वह भाव श्रन है। अतः वह परोपदेशपूर्वक अर्थात् दूसरों को सहायता से भी हो सकता है और परोपदेश के बिना भी हो सकता है । यद्यपि लब्ध्यक्षररूप अर्थबाध-दूसरे शब्दों में लिखित अथवा उच्चरित स्वर और व्यञ्जनों से होनेवाला अर्थबोध--भी बिना भाषा को सीखे नहीं होता। अतः इस अपेक्षा से उसे परम्परागत शब्दावली में परोपदेशपूर्वक और आधुनिक शब्दावली में अजितगुण हो मानना चाहिए । किन्तु जैनाचार्यों की मान्यता यह है कि जब तक व्यक्ति में स्वतः अर्थबोधसामर्थ्य या प्रतीकों के माध्यम से अर्थबोध ग्रहण करने की शक्ति नहीं होगी, वह अर्थबोध नहीं कर सकेगा और इस दृष्टि से उसे स्वाभाविक या अजित गुण भी माना जा सकता है। आधुनिक भाषाशास्त्र की दृष्टि से निश्चय ही यह बात सत्य है कि भाषा सीखी हुई या अर्जित होती है किन्तु इसके साथ-साथ मनोविज्ञान हमें यह भी बताता है कि सीखने की शक्ति (बुद्धिलब्धि) एक अनर्जित गुण है । स्वर, व्यञ्जन अथवा शब्दों के माध्यम से होनेवाली अर्थबोधसामर्थ्य सभी प्राणियों में और सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती। वस्तुतः बुद्धिलब्धि ही लब्ध्यक्षर है और आधुनिक मनोविज्ञान ने उसे एक अजित या अनसीखा हआ गुण माना है। इसी बात को जैनों ने इस रूप में प्रकट किया है कि लब्ध्यक्षर श्रत ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है, अतःवह आत्मनिष्ठ (Subjective) है, जबकि संज्ञा-अक्षर एवं व्यञ्जनाक्षर बाह्य एवं वस्तुनिष्ठ (Objective) है, यह भाषा का अजित पक्ष है । यद्यपि लब्ध्यक्षर अर्थबोध सामर्थ्य के रूप में अर्जित है, किन्तु यह अर्थबोध संज्ञा-अक्षर एवं व्यञ्जनाक्षर पर भी आधारित है और यूँकि ये अजितगुण हैं, सीखे जाते हैं -अतः लब्ध्यक्षर भी किसी सीमा तक अजित या सोखा हुआ माना जा सकता है।
स्वर और व्यञ्जन-जैनाचार्यों ने अक्षरों को स्वर और व्यञ्जन-इन दो वर्गों में विभाजित किया है। विशेषावश्यक भाष्य में जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण ने स्वर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है-अक्षरों का जो अनुसरण करता है वह 'स्वर' है।' वृत्तिकार ने अक्षर को सत्ता तथा ज्ञान का वाचक-पर्याय माना है। उन्हीं का अनुसरण करने अथवा उन्हें प्रकट करने के कारण उसे स्वर कहते हैं । भाष्यकार आगे कहते हैं कि जो अकेले भी वस्तु/ज्ञान का बोधक होता है तथा व्यञ्जनों को उच्चारण के योग्य बनाता है, वही स्वर है। क्योंकि स्वरों के बिना व्यञ्जन उच्चारण योग्य नहीं बनते हैं।
जैनाचार्य व्यञ्जन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक घट को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जो अर्थ (पदार्थ) को अभिव्यक्त (प्रकट) करता है, अर्थात् उनका
१. अक्खरसरेणण सरा-विशेषावश्यक भाष्य ४६१ । २. सुद्धाऽवि सरंति सयं सारेंति वंजणाई जं तेणं ।
होति सरा न कयाइवि तेहिं विणा वंजणं सरइ ॥--वही ४६२ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org