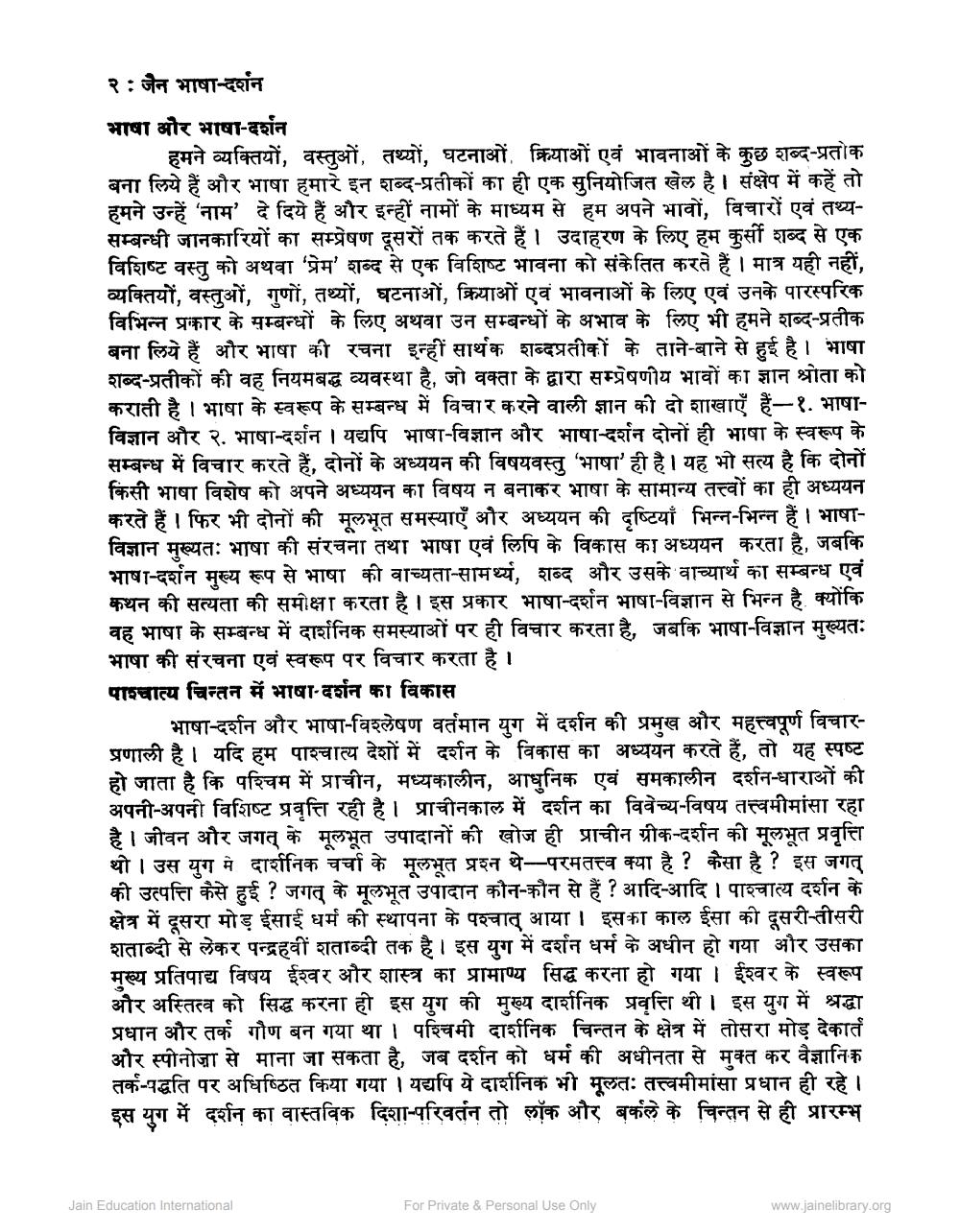________________
२: जैन भाषा-दर्शन भाषा और भाषा-दर्शन
हमने व्यक्तियों, वस्तुओं, तथ्यों, घटनाओं, क्रियाओं एवं भावनाओं के कुछ शब्द-प्रतोक बना लिये हैं और भाषा हमारे इन शब्द-प्रतीकों का ही एक सुनियोजित खेल है। संक्षेप में कहें तो हमने उन्हें 'नाम' दे दिये हैं और इन्हीं नामों के माध्यम से हम अपने भावों, विचारों एवं तथ्यसम्बन्धी जानकारियों का सम्प्रेषण दूसरों तक करते हैं। उदाहरण के लिए हम कुर्सी शब्द से एक विशिष्ट वस्तु को अथवा 'प्रेम' शब्द से एक विशिष्ट भावना को संकेतित करते हैं । मात्र यही नहीं, व्यक्तियों, वस्तुओं, गुणों, तथ्यों, घटनाओं, क्रियाओं एवं भावनाओं के लिए एवं उनके पारस्परिक विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों के लिए अथवा उन सम्बन्धों के अभाव के लिए भी हमने शब्द-प्रतीक बना लिये हैं और भाषा की रचना इन्हीं सार्थक शब्दप्रतीकों के ताने-बाने से हुई है। भाषा शब्द-प्रतीकों की वह नियमबद्ध व्यवस्था है, जो वक्ता के द्वारा सम्प्रेषणीय भावों का ज्ञान श्रोता को कराती है। भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार करने वाली ज्ञान की दो शाखाएँ हैं-१. भाषाविज्ञान और २. भाषा-दर्शन । यद्यपि भाषा-विज्ञान और भाषा-दर्शन दोनों ही भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार करते हैं, दोनों के अध्ययन की विषयवस्तु 'भाषा' ही है। यह भी सत्य है कि दोनों किसी भाषा विशेष को अपने अध्ययन का विषय न बनाकर भाषा के सामान्य तत्त्वों का ही अध्ययन करते हैं। फिर भी दोनों की मूलभूत समस्याएँ और अध्ययन की दृष्टियाँ भिन्न-भिन्न हैं। भाषाविज्ञान मुख्यतः भाषा की संरचना तथा भाषा एवं लिपि के विकास का अध्ययन करता है, जबकि भाषा-दर्शन मुख्य रूप से भाषा की वाच्यता-सामर्थ्य, शब्द और उसके वाच्यार्थ का सम्बन्ध एवं कथन की सत्यता की समीक्षा करता है । इस प्रकार भाषा-दर्शन भाषा-विज्ञान से भिन्न है क्योंकि वह भाषा के सम्बन्ध में दार्शनिक समस्याओं पर ही विचार करता है, जबकि भाषा-विज्ञान मुख्यतः भाषा की संरचना एवं स्वरूप पर विचार करता है। पाश्चात्य चिन्तन में भाषा-दर्शन का विकास
भाषा-दर्शन और भाषा-विश्लेषण वर्तमान युग में दर्शन की प्रमुख और महत्त्वपूर्ण विचारप्रणाली है। यदि हम पाश्चात्य देशों में दर्शन के विकास का अध्ययन करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिम में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक एवं समकालीन दर्शन-धाराओं की अपनी-अपनी विशिष्ट प्रवृत्ति रही है। प्राचीनकाल में दर्शन का विवेच्य-विषय तत्त्वमीमांसा रहा है। जीवन और जगत् के मलभत उपादानों की खोज ही प्राचीन ग्रीक-दर्शन की मुलभत प्रवत्ति थो । उस युग मे दार्शनिक चर्चा के मूलभूत प्रश्न थे—परमतत्त्व क्या है ? कैसा है ? इस जगत् की उत्पत्ति कैसे हुई ? जगत् के मूलभूत उपादान कौन-कौन से हैं ? आदि-आदि । पाश्चात्य दर्शन के क्षेत्र में दूसरा मोड़ ईसाई धर्म की स्थापना के पश्चात् आया। इसका काल ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी तक है। इस युग में दर्शन धर्म के अधीन हो गया और उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय ईश्वर और शास्त्र का प्रामाण्य सिद्ध करना हो गया । ईश्वर के स्वरूप
और अस्तित्व को सिद्ध करना ही इस युग की मुख्य दार्शनिक प्रवृत्ति थी। इस युग में श्रद्धा प्रधान और तर्क गौण बन गया था। पश्चिमी दार्शनिक चिन्तन के क्षेत्र में तोसरा मोड़ देकार्त
और स्पीनोज़ा से माना जा सकता है, जब दर्शन को धर्म की अधीनता से मक्त कर वैज्ञानिक तर्क-पद्धति पर अधिष्ठित किया गया । यद्यपि ये दार्शनिक भी मूलतः तत्त्वमीमांसा प्रधान ही रहे । इस युग में दर्शन का वास्तविक दिशा-परिवर्तन तो लॉक और बर्कले के चिन्तन से ही प्रारम्भ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org