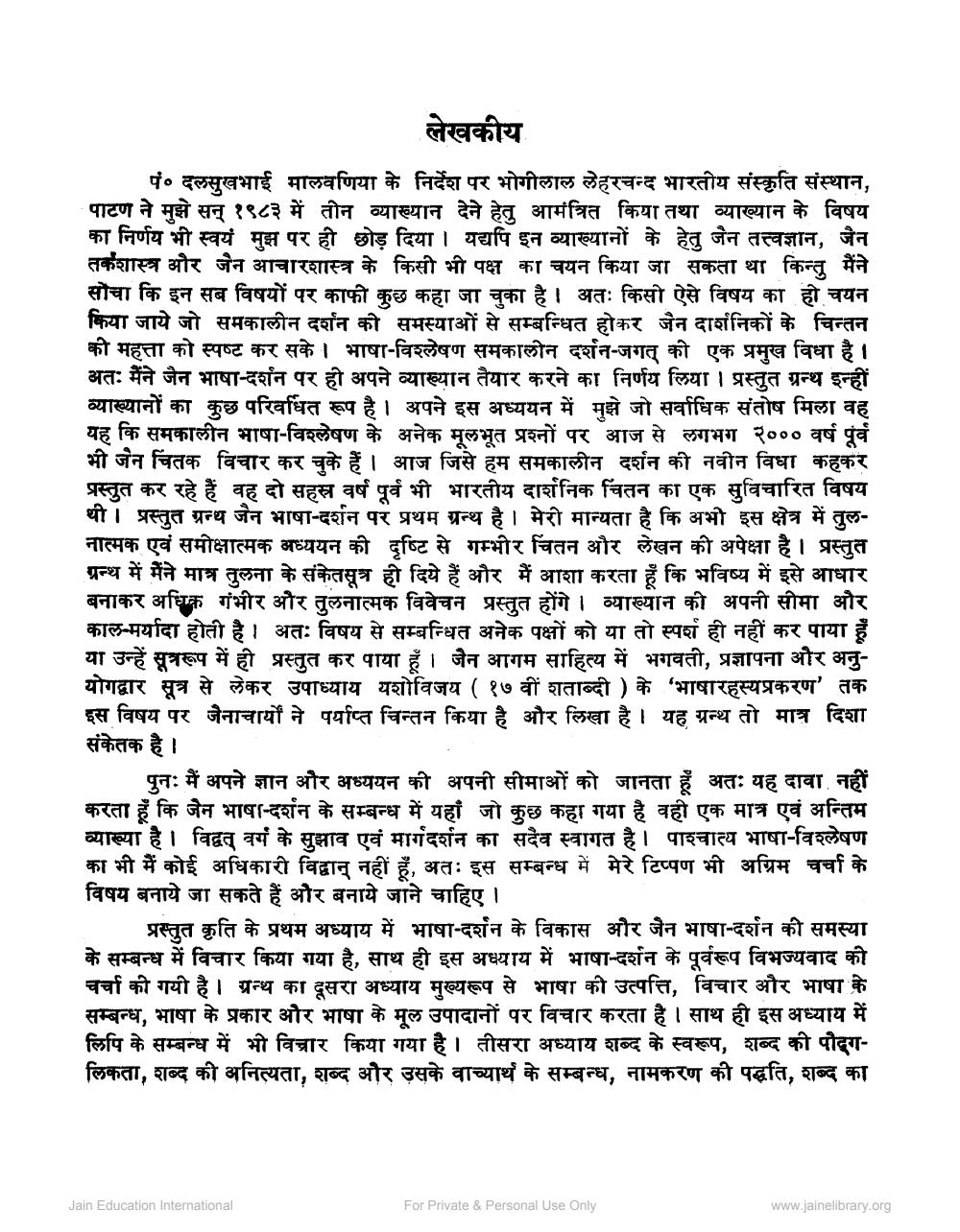________________
लेखकीय पं० दलसुखभाई मालवणिया के निर्देश पर भोगीलाल लेहरचन्द भारतीय संस्कृति संस्थान, पाटण ने मुझे सन् १९८३ में तीन व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया तथा व्याख्यान के विषय का निर्णय भी स्वयं मुझ पर ही छोड़ दिया। यद्यपि इन व्याख्यानों के हेतु जैन तत्त्वज्ञान, जैन तर्कशास्त्र और जैन आचारशास्त्र के किसी भी पक्ष का चयन किया जा सकता था किन्तु मैंने सोचा कि इन सब विषयों पर काफी कुछ कहा जा चुका है। अतः किसी ऐसे विषय का हो चयन किया जाये जो समकालीन दर्शन की समस्याओं से सम्बन्धित होकर जैन दार्शनिकों के चिन्तन की महत्ता को स्पष्ट कर सके। भाषा-विश्लेषण समकालीन दर्शन-जगत् को एक प्रमुख विधा है। अतः मैंने जैन भाषा-दर्शन पर ही अपने व्याख्यान तैयार करने का निर्णय लिया। प्रस्तुत ग्रन्थ इन्हीं व्याख्यानों का कुछ परिवर्धित रूप है। अपने इस अध्ययन में मुझे जो सर्वाधिक संतोष मिला वह यह कि समकालीन भाषा-विश्लेषण के अनेक मूलभूत प्रश्नों पर आज से लगभग २००० वर्ष पूर्व भी जैन चिंतक विचार कर चुके हैं। आज जिसे हम समकालीन दर्शन की नवीन विधा कहकर प्रस्तुत कर रहे हैं वह दो सहस्र वर्ष पूर्व भी भारतीय दार्शनिक चिंतन का एक सुविचारित विषय थी। प्रस्तुत ग्रन्थ जैन भाषा-दर्शन पर प्रथम ग्रन्थ है। मेरी मान्यता है कि अभी इस क्षेत्र में तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन की दृष्टि से गम्भीर चिंतन और लेखन की अपेक्षा है। प्रस्तुत ग्रन्थ में मैंने मात्र तुलना के संकेतसूत्र ही दिये हैं और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इसे आधार बनाकर अधिक गंभीर और तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत होंगे। व्याख्यान की अपनी सीमा और काल-मर्यादा होती है। अतः विषय से सम्बन्धित अनेक पक्षों को या तो स्पर्श ही नहीं कर पाया हूँ या उन्हें सूत्ररूप में ही प्रस्तुत कर पाया हूँ। जैन आगम साहित्य में भगवती, प्रज्ञापना और अनुयोगद्वार सूत्र से लेकर उपाध्याय यशोविजय ( १७ वीं शताब्दी ) के 'भाषारहस्यप्रकरण' तक इस विषय पर जैनाचार्यों ने पर्याप्त चिन्तन किया है और लिखा है। यह ग्रन्थ तो मात्र दिशा संकेतक है।
पुनः मैं अपने ज्ञान और अध्ययन की अपनी सीमाओं को जानता हूँ अतः यह दावा नहीं करता हूँ कि जैन भाषा-दर्शन के सम्बन्ध में यहाँ जो कुछ कहा गया है वही एक मात्र एवं अन्तिम व्याख्या है। विद्वत् वर्ग के सुझाव एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है। पाश्चात्य भाषा-विश्लेषण का भी मैं कोई अधिकारी विद्वान नहीं है, अतः इस सम्बन्ध में मेरे टिप्पण भी अग्निम चर्चा के विषय बनाये जा सकते हैं और बनाये जाने चाहिए।
प्रस्तुत कृति के प्रथम अध्याय में भाषा-दर्शन के विकास और जैन भाषा-दर्शन की समस्या के सम्बन्ध में विचार किया गया है, साथ ही इस अध्याय में भाषा-दर्शन के पूर्वरूप विभज्यवाद की चर्चा की गयी है। ग्रन्थ का दूसरा अध्याय मुख्यरूप से भाषा की उत्पत्ति, विचार और भाषा के सम्बन्ध, भाषा के प्रकार और भाषा के मूल उपादानों पर विचार करता है । साथ ही इस अध्याय में लिपि के सम्बन्ध में भी विचार किया गया है। तीसरा अध्याय शब्द के स्वरूप, शब्द की पौद्गलिकता, शब्द की अनित्यता, शब्द और उसके वाच्यार्थ के सम्बन्ध, नामकरण की पद्धति, शब्द का
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org