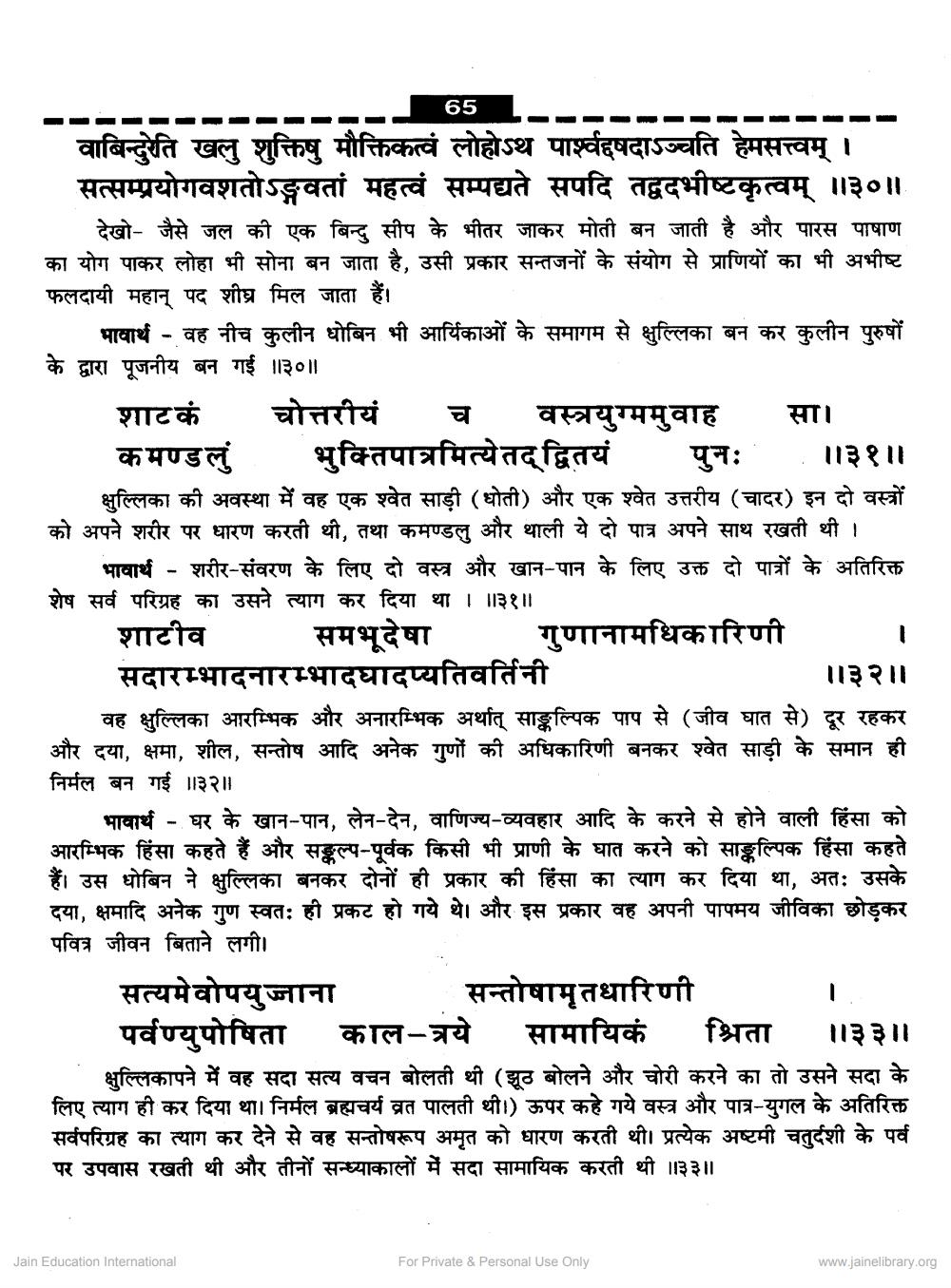________________
65
वाबिन्दुरेति खलु शुक्तिषु मौक्तिकत्वं लोहोऽथ पार्श्वद्दषदाऽञ्चति हेमसत्त्वम् । सत्सम्प्रयोगवशतोऽङ्गवतां महत्वं सम्पद्यते सपदि तद्वदभीष्टकृत्वम् ॥३०॥
देखो - जैसे जल की एक बिन्दु सीप के भीतर जाकर मोती बन जाती है और पारस पाषाण का योग पाकर लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार सन्तजनों के संयोग से प्राणियों का भी अभीष्ट फलदायी महान् पद शीघ्र मिल जाता हैं।
भावार्थ वह नीच कुलीन धोबिन भी आर्यिकाओं के समागम से क्षुल्लिका बन कर कुलीन पुरुषों के द्वारा पूजनीय बन गई ||३०||
चोत्तरीयं
शाटकं
च
कमण्डलुं
भुक्तिपात्रमित्येतद् द्वितयं
पुनः
॥३१॥
क्षुल्लिका की अवस्था में वह एक श्वेत साड़ी (धोती) और एक श्वेत उत्तरीय ( चादर) इन दो वस्त्रों को अपने शरीर पर धारण करती थी, तथा कमण्डलु और थाली ये दो पात्र अपने साथ रखती थी । शरीर-संवरण के लिए दो वस्त्र और खान-पान के लिए उक्त दो पात्रों के अतिरिक्त शेष सर्व परिग्रह का उसने त्याग कर दिया था । ||३१||
भावार्थ
शाटीव
गुणानामधिकारिणी
समभूदेषा सदारम्भादनारम्भादघादप्यतिवर्तिनी
॥३२॥
वह क्षुल्लिका आरम्भिक और अनारम्भिक अर्थात् साङ्कल्पिक पाप से ( जीव घात से) दूर रहकर और दया, क्षमा, शील, सन्तोष आदि अनेक गुणों की अधिकारिणी बनकर श्वेत साड़ी के समान ही निर्मल बन गई ॥३२॥
-
सत्यमेवोपयुज्जाना पर्वण्युपोषिता
वस्त्रयुग्ममुवाह
भावार्थ घर के खान-पान, लेन-देन, वाणिज्य-व्यवहार आदि के करने से होने वाली हिंसा को आरम्भिक हिंसा कहते हैं और सङ्कल्प- पूर्वक किसी भी प्राणी के घात करने को साङ्कल्पिक हिंसा कहते हैं। उस धोबिन ने क्षुल्लिका बनकर दोनों ही प्रकार की हिंसा का त्याग कर दिया था, अतः उसके दया, क्षमादि अनेक गुण स्वतः ही प्रकट हो गये थे। और इस प्रकार वह अपनी पापमय जीविका छोड़कर पवित्र जीवन बिताने लगी।
Jain Education International
सन्तोषामृतधारिणी सामायिकं
सा।
1
I
काल-त्रये
श्रिता
॥३३॥
क्षुल्लिकापने में वह सदा सत्य वचन बोलती थी (झूठ बोलने और चोरी करने का तो उसने सदा के लिए त्याग ही कर दिया था। निर्मल ब्रह्मचर्य व्रत पालती थी।) ऊपर कहे गये वस्त्र और पात्र - युगल के अतिरिक्त सर्वपरिग्रह का त्याग कर देने से वह सन्तोषरूप अमृत को धारण करती थी। प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी के पर्व पर उपवास रखती थी और तीनों सन्ध्याकालों में सदा सामायिक करती थी ॥३३॥
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org