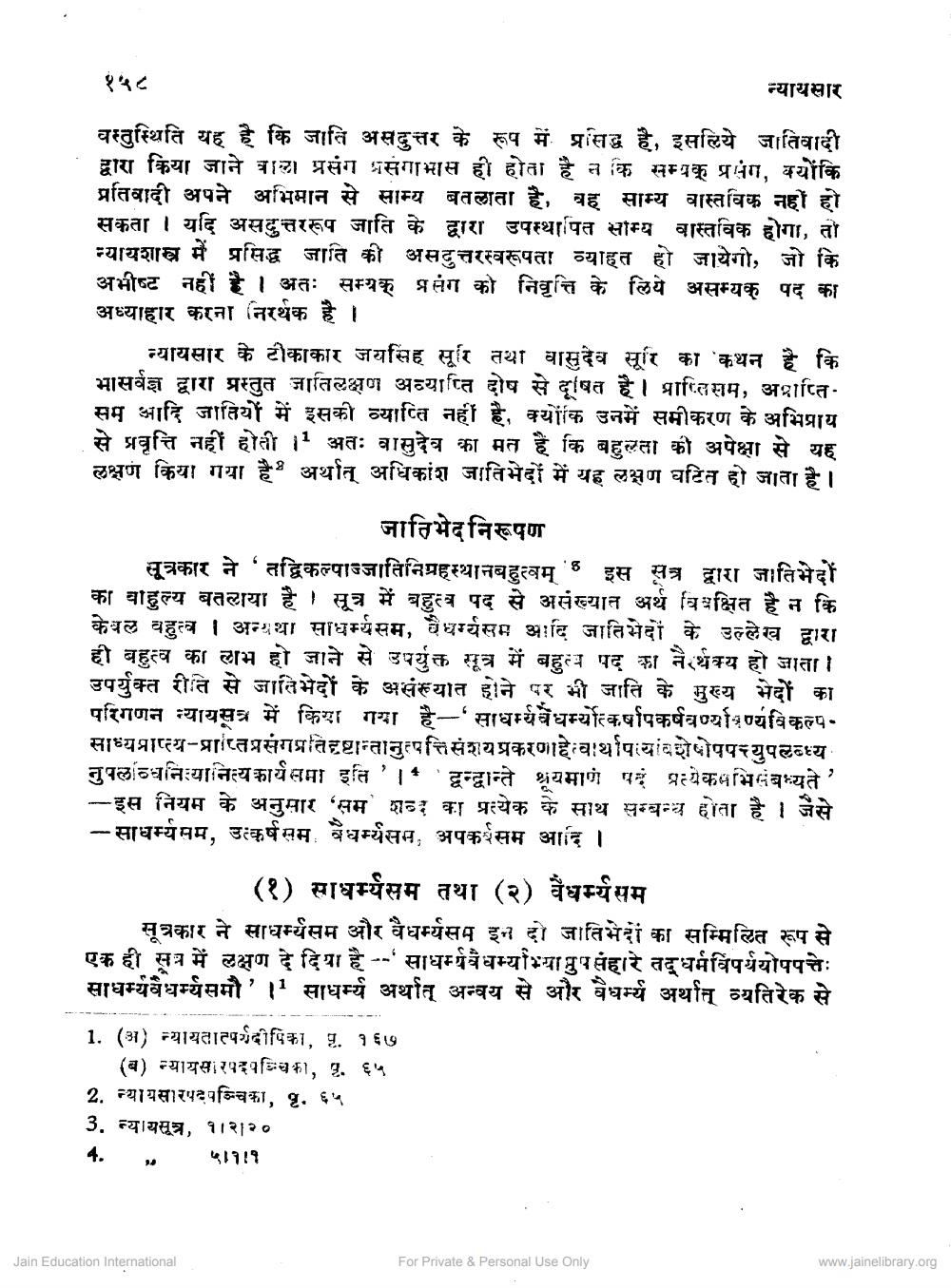________________
१५८
न्यायसार
वस्तुस्थिति यह है कि जाति असदुत्तर के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिये जातिवादी द्वारा किया जाने वाला प्रसंग प्रसंगाभास ही होता है न कि सम्यक् प्रसंग, क्योंकि प्रतिवादी अपने अभिमान से साम्य बतलाता है, वह साम्य वास्तविक नहीं हो सकता । यदि असदुत्तररूप जाति के द्वारा उपस्थापित साम्य वास्तविक होगा, तो न्यायशास्त्र में प्रसिद्ध जाति की असदुत्तरस्वरूपता व्याहत हो जायेगो, जो कि अभीष्ट नहीं है । अतः सम्यक् प्रसंग को निवृत्ति के लिये असम्यक् पद का अध्याहार करना निरर्थक है ।
न्यायसार के टीकाकार जयसिंह सूरि तथा वासुदेव सूरि का कथन है कि भासर्वज्ञ द्वारा प्रस्तुत जातिलक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित है । प्राप्तिसम, अप्राप्तिसम आदि जातियों में इसकी व्याप्ति नहीं है, क्योंकि उनमें समीकरण के अभिप्राय से प्रवृत्ति नहीं होती । अतः वासुदेव का मत हैं कि बहुलता की अपेक्षा से यह लक्षण किया गया है " अर्थात् अधिकांश जातिभेदों में यह लक्षण घटित हो जाता है ।
जातिभेद निरूपण
8
सूत्रकार ने 'तद्विकल्पाज्जातिनिग्रहस्थानबहुत्वम् इस सूत्र द्वारा जातिभेदों का बाहुल्य बतलाया है। सूत्र में बहुत्व पद से असंख्यात अर्थ विवक्षित है न कि केवल वहुत्व | अन्यथा साधर्म्यसम, वैधर्ग्यसम आदि जातिभेदों के उल्लेख द्वारा ही बहुत्व का लाभ हो जाने से उपर्युक्त सूत्र में बहुल पद का नैरर्थक्य हो जाता । उपर्युक्त रीति से जातिभेदों के असंख्यात होने पर भी जाति के मुख्य भेदों का परिगणन न्यायसूत्र में किया गया है- 'साधर्म्य वैधम्र्योत्कर्षापकर्षवत्रयविकल्पसाध्यप्राप्त्य-प्राप्तिप्रसंगप्रतिदृष्टान्तानुत्पत्ति संशय प्रकरणा हेत्वार्थापत्यविशेषोपपत्त्युपलब्ध्य नुपलब्धिनित्यानित्य कार्यसमा इति I * द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं परं प्रत्येकमभिसंबध्यते ' - इस नियम के अनुसार 'सम' शब्द का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध होता है । जैसे - साधर्म्यसम, उत्कर्षसम वैधर्म्यसम, अपकर्षसम आदि ।
(१) साधर्म्यम तथा ( २ ) वैधर्म्य सम
सूत्रकार ने साधर्म्यसम और वैधर्म्यसम इन दो जातिभेदों का सम्मिलित रूप से एक ही सूत्र में लक्षण दे दिया है--' साधर्म्य वैधर्म्याभ्यामुपसंहारे तद्धर्मविपर्ययोपपत्तेः साधर्म्य वैधर्म्य समौ' ।' साधर्म्य अर्थात् अन्वय से और वैधर्म्य अर्थात् व्यतिरेक से
1. ( अ ) न्यायतात्पर्यदीपिका, पृ. १६७
(ब) न्यायसारपदपञ्चिका
६५
2. न्यायसारपदपञ्चिका, पृ. ६५
3. न्यायसूत्र
4.
28
Jain Education International
1
१।२।२०
५।१८१
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org