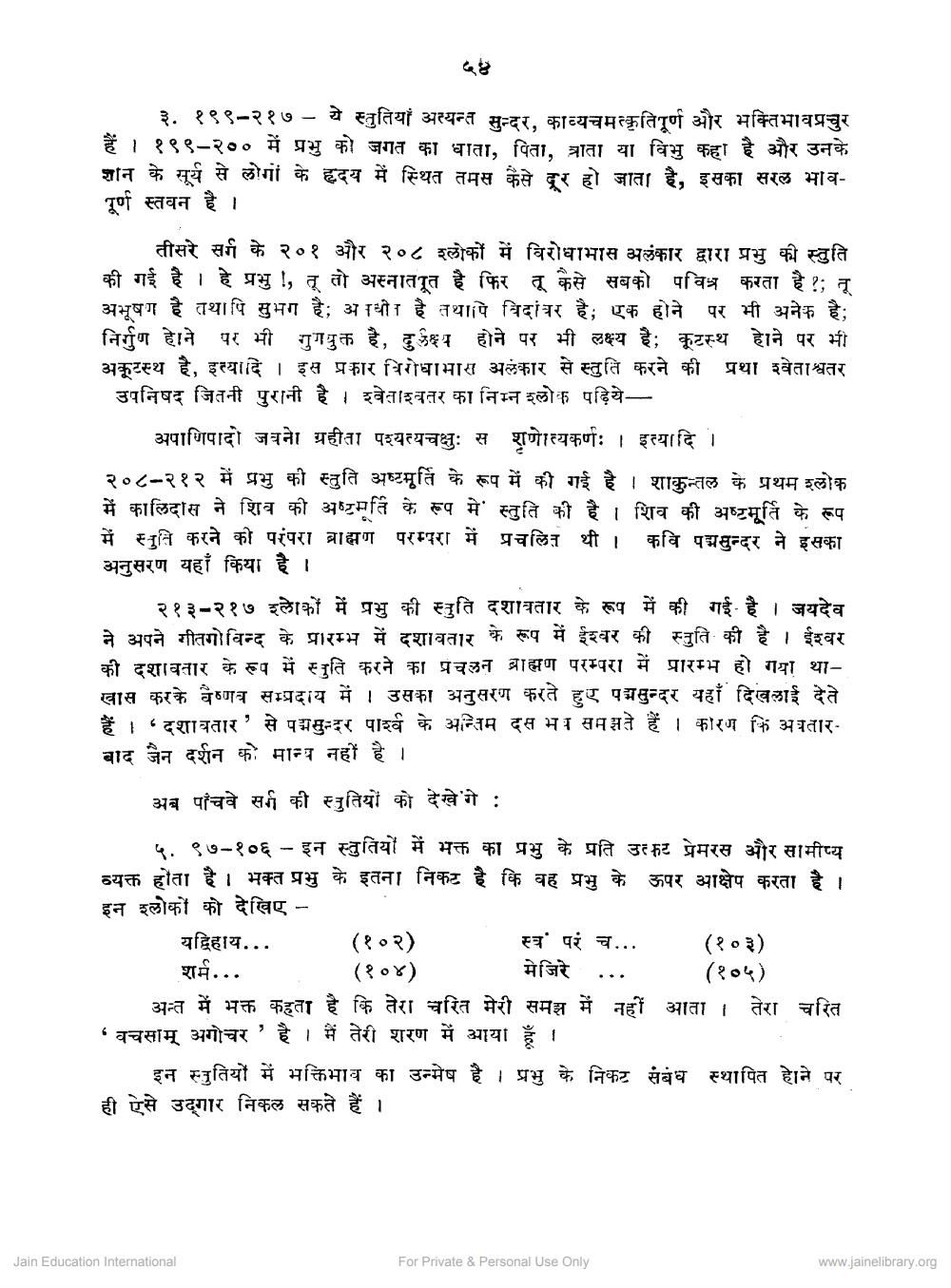________________
३. १९९-२१७ - ये स्तुतियां अत्यन्त सुन्दर, काव्यचमत्कृतिपूर्ण और भक्तिभावप्रचुर हैं । १९९-२०० में प्रभु को जगत का धाता, पिता, त्राता या विभु कहा है और उनके शान के सूर्य से लोगों के हृदय में स्थित तमस कैसे दूर हो जाता है, इसका सरल भावपूर्ण स्तवन है ।
__ तीसरे सर्ग के २०१ और २०८ श्लोकों में विरोधाभास अलंकार द्वारा प्रभु की स्तुति की गई है । हे प्रभु !, त तो अस्नातात है फिर त कैसे सबको पवित्र करता है १: त अभूषण है तथापि सुभग है; अधीन है तथापि विदांवर है; एक होने पर भी अनेक है; निर्गुण होने पर भी गुगयुक्त है, दुर्लक्ष्य होने पर भी लक्ष्य है; कूटस्थ होने पर भी अकूटस्थ है, इत्यादि । इस प्रकार विरोधाभास अलंकार से स्तुति करने की प्रथा श्वेताश्वतर उपनिषद जितनी पुरानी है । श्वेताश्वतर का निम्न श्लोक पढ़िये
अपाणिपादो जवना ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । इत्यादि । २०८-२१२ में प्रभु की स्तुति अष्टमूर्ति के रूप में की गई है । शाकुन्तल के प्रथम श्लोक में कालिदास ने शिव की अष्टमूर्ति के रूप मे स्तुति की है । शिव की अष्टमूर्ति के रूप में स्तुति करने को परंपरा ब्राह्मण परम्परा में प्रचलित थी। कवि पद्मसुन्दर ने इसका अनुसरण यहाँ किया है ।
२१३-२१७ इलाकों में प्रभु की स्तुति दशावतार के रूप में की गई है । जयदेव ने अपने गीतगोविन्द के प्रारम्भ में दशावतार के रूप में ईश्वर की स्तुति की है । ईश्वर की दशावतार के रूप में स्तुति करने का प्रचलन ब्राह्मण परम्परा में प्रारम्भ हो गया थाखास करके वैष्णव सम्प्रदाय में । उसका अनुसरण करते हुए पद्मसुन्दर यहाँ दिखलाई देते हैं । “दशावतार' से पद्मसुन्दर पाव के अन्तिम दस भर समझते हैं । कारण कि अवतारबाद जैन दर्शन को मान्य नहीं है ।
अब पांचवे सर्ग की स्तुतियों को देखेंगे :
५. ९७-१०६ - इन स्तुतियों में भक्त का प्रभु के प्रति उत्कट प्रेमरस और सामीप्य व्यक्त होता है। भक्त प्रभु के इतना निकट है कि वह प्रभु के ऊपर आक्षेप करता है। इन इलोकों को देखिए - यद्विहाय... (१०२)
स्व परं च... (१०३) शर्म... (१०४)
मेजिरे ... (१०५) अन्त में भक्त कहता है कि तेरा चरित मेरी समझ में नहीं आता । तेरा चरित 'वचसाम् अगोचर' है । मैं तेरी शरण में आया हूँ ।
इन स्तुतियों में भक्तिभाव का उन्मेष है । प्रभु के निकट संबंध स्थापित होने पर ही ऐसे उद्गार निकल सकते हैं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org