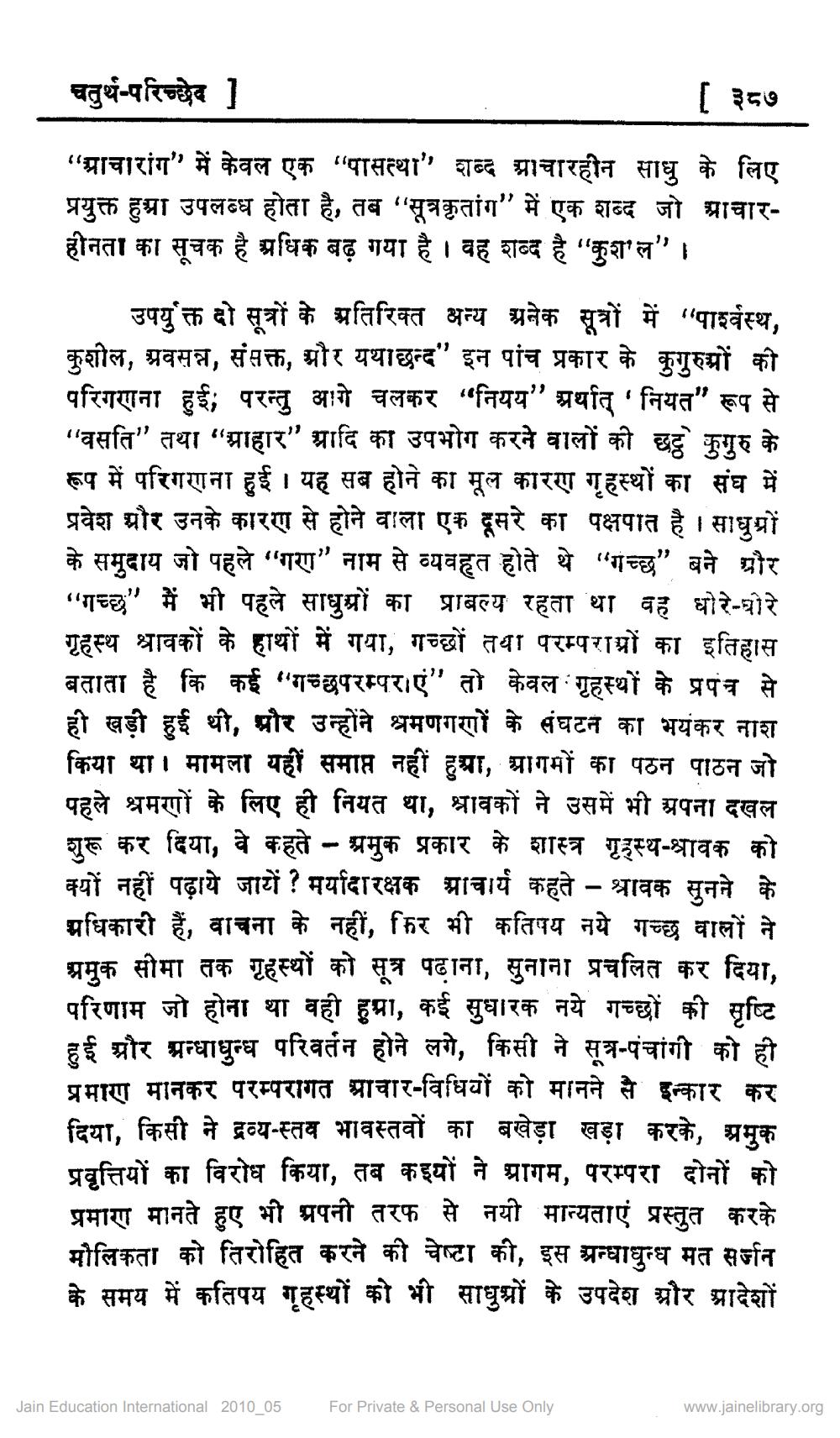________________
चतुर्थ-परिच्छेद ]
[ ३८७
"प्राचारांग' में केवल एक "पासत्था'' शब्द प्राचारहीन साधु के लिए प्रयुक्त हुआ उपलब्ध होता है, तब "सूत्रकृतांग" में एक शब्द जो प्राचारहीनता का सूचक है अधिक बढ़ गया है । वह शब्द है "कुश'ल' ।
उपर्युक्त दो सूत्रों के अतिरिक्त अन्य अनेक सूत्रों में 'पार्श्वस्थ, कुशील, अवसन्न, संसक्त, और यथाछन्द" इन पांच प्रकार के कुगुरुपों की परिगणना हुई; परन्तु आगे चलकर "नियय" अर्थात् 'नियत" रूप से "वसति" तथा "पाहार" प्रादि का उपभोग करने वालों की छ8 कुगुरु के रूप में परिगणना हुई । यह सब होने का मूल कारण गृहस्थों का संघ में प्रवेश और उनके कारण से होने वाला एक दूसरे का पक्षपात है । साधुनों के समुदाय जो पहले "गण" नाम से व्यवहृत होते थे “गच्छ” बने और "गच्छ” मैं भी पहले साधुओं का प्राबल्य रहता था वह धोरे-घोरे गृहस्थ श्रावकों के हाथों में गया, गच्छों तथा परम्परामों का इतिहास बताता है कि कई "गच्छपरम्पराएं" तो केवल गृहस्थों के प्रपंच से ही खड़ी हुई थी, और उन्होंने श्रमणगणों के संघटन का भयंकर नाश किया था। मामला यहीं समाप्त नहीं हुअा, पागमों का पठन पाठन जो पहले श्रमणों के लिए ही नियत था, श्रावकों ने उसमें भी अपना दखल शुरू कर दिया, वे कहते - अमुक प्रकार के शास्त्र गृहस्थ-श्रावक को क्यों नहीं पढ़ाये जायें? मर्यादारक्षक आचार्य कहते - श्रावक सुनने के अधिकारी हैं, वाचना के नहीं, फिर भी कतिपय नये गच्छ वालों ने अमुक सीमा तक गृहस्थों को सूत्र पढ़ाना, सुनाना प्रचलित कर दिया, परिणाम जो होना था वही हुमा, कई सुधारक नये गच्छों की सृष्टि हुई और अन्धाधुन्ध परिवर्तन होने लगे, किसी ने सूत्र-पंचांगी को ही प्रमाण मानकर परम्परागत प्राचार-विधियों को मानने से इन्कार कर दिया, किसी ने द्रव्य-स्तव भावस्तवों का बखेड़ा खड़ा करके, अमुक प्रवृत्तियों का विरोध किया, तब कइयों ने प्रागम, परम्परा दोनों को प्रमाण मानते हुए भी अपनी तरफ से नयी मान्यताएं प्रस्तुत करके मौलिकता को तिरोहित करने की चेष्टा की, इस अन्धाधुन्ध मत सर्जन के समय में कतिपय गृहस्थों को भी साधुओं के उपदेश और आदेशों
Jain Education International 2010_05
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org