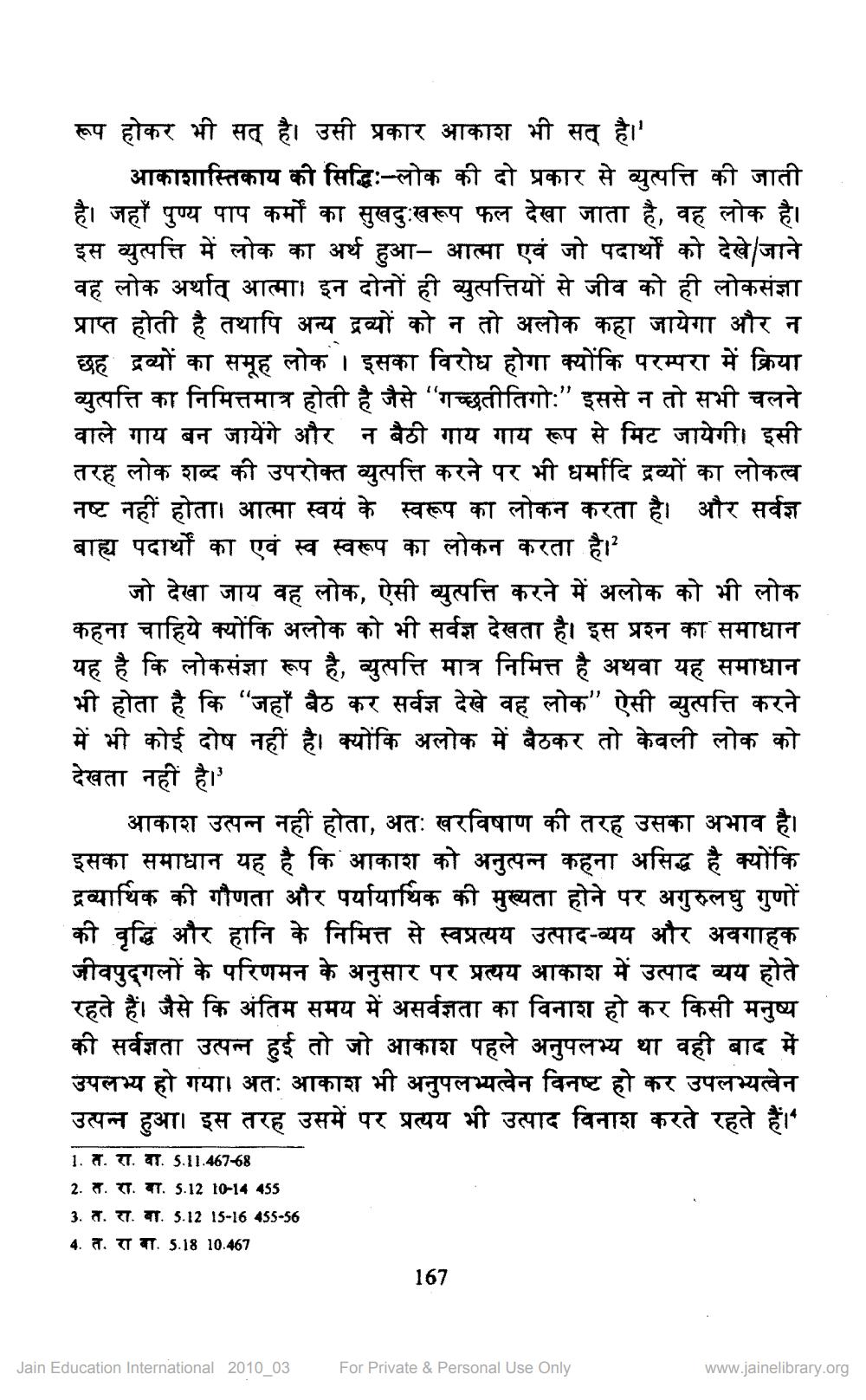________________
रूप होकर भी सत् है। उसी प्रकार आकाश भी सत् है।'
आकाशास्तिकाय की सिद्धिः-लोक की दो प्रकार से व्युत्पत्ति की जाती है। जहाँ पुण्य पाप कर्मों का सुखदुःखरूप फल देखा जाता है, वह लोक है। इस व्युत्पत्ति में लोक का अर्थ हुआ- आत्मा एवं जो पदार्थों को देखे जाने वह लोक अर्थात् आत्मा। इन दोनों ही व्युत्पत्तियों से जीव को ही लोकसंज्ञा प्राप्त होती है तथापि अन्य द्रव्यों को न तो अलोक कहा जायेगा और न छह द्रव्यों का समूह लोक । इसका विरोध होगा क्योंकि परम्परा में क्रिया व्युत्पत्ति का निमित्तमात्र होती है जैसे “गच्छतीतिगोः" इससे न तो सभी चलने वाले गाय बन जायेंगे और न बैठी गाय गाय रूप से मिट जायेगी। इसी तरह लोक शब्द की उपरोक्त व्युत्पत्ति करने पर भी धर्मादि द्रव्यों का लोकत्व नष्ट नहीं होता। आत्मा स्वयं के स्वरूप का लोकन करता है। और सर्वज्ञ बाह्य पदार्थों का एवं स्व स्वरूप का लोकन करता है।
जो देखा जाय वह लोक, ऐसी व्युत्पत्ति करने में अलोक को भी लोक कहना चाहिये क्योंकि अलोक को भी सर्वज्ञ देखता है। इस प्रश्न का समाधान यह है कि लोकसंज्ञा रूप है, व्युत्पत्ति मात्र निमित्त है अथवा यह समाधान भी होता है कि "जहाँ बैठ कर सर्वज्ञ देखे वह लोक" ऐसी व्युत्पत्ति करने में भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि अलोक में बैठकर तो केवली लोक को देखता नहीं है।'
__ आकाश उत्पन्न नहीं होता, अतः खरविषाण की तरह उसका अभाव है। इसका समाधान यह है कि आकाश को अनुत्पन्न कहना असिद्ध है क्योंकि द्रव्यार्थिक की गौणता और पर्यायार्थिक की मुख्यता होने पर अगुरुलघु गुणों की वृद्धि और हानि के निमित्त से स्वप्रत्यय उत्पाद-व्यय और अवगाहक जीवपुद्गलों के परिणमन के अनुसार पर प्रत्यय आकाश में उत्पाद व्यय होते रहते हैं। जैसे कि अंतिम समय में असर्वज्ञता का विनाश हो कर किसी मनुष्य की सर्वज्ञता उत्पन्न हुई तो जो आकाश पहले अनुपलभ्य था वही बाद में उपलभ्य हो गया। अतः आकाश भी अनुपलभ्यत्वेन विनष्ट हो कर उपलभ्यत्वेन उत्पन्न हुआ। इस तरह उसमें पर प्रत्यय भी उत्पाद विनाश करते रहते हैं।'
1. त. रा. वा. 5.11.467-68 2. स. रा. बा. 5.12 10-14455 3. त. रा. बा. 5.12 15-16 455-56 4. त. रावा. 5.18 10.467
167
___Jain Education International 2010_03
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org