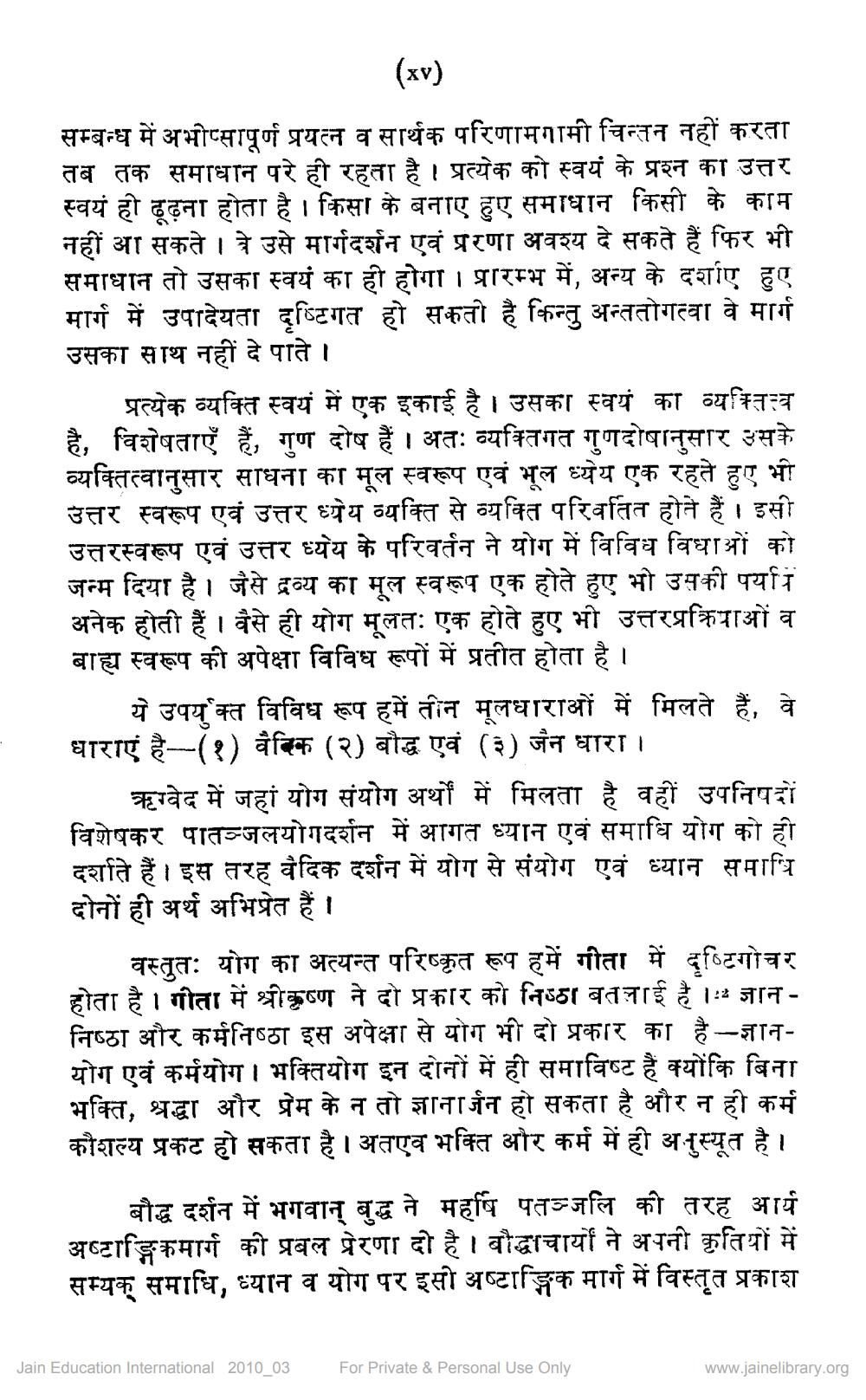________________
(xv)
सम्बन्ध में अभीप्सापूर्ण प्रयत्न व सार्थक परिणामगामी चिन्तन नहीं करता तब तक समाधान परे ही रहता है। प्रत्येक को स्वयं के प्रश्न का उत्तर स्वयं ही ढूढ़ना होता है। किसा के बनाए हुए समाधान किसी के काम नहीं आ सकते । वे उसे मार्गदर्शन एवं प्ररणा अवश्य दे सकते हैं फिर भी समाधान तो उसका स्वयं का ही होगा। प्रारम्भ में, अन्य के दर्शाए हुए मार्ग में उपादेयता दृष्टिगत हो सकती है किन्तु अन्ततोगत्वा वे मार्ग उसका साथ नहीं दे पाते।
प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में एक इकाई है। उसका स्वयं का व्यक्तित्व है, विशेषताएँ हैं, गुण दोष हैं । अतः व्यक्तिगत गुणदोषानुसार उसके व्यक्तित्वानुसार साधना का मूल स्वरूप एवं भूल ध्येय एक रहते हुए भी उत्तर स्वरूप एवं उत्तर ध्येय व्यक्ति से व्यक्ति परिवर्तित होते हैं। इसी उत्तरस्वरूप एवं उत्तर ध्यय के परिवर्तन ने योग में विविध विधाओं को जन्म दिया है। जैसे द्रव्य का मूल स्वरूप एक होते हुए भी उसकी पर्याय अनेक होती हैं । वैसे ही योग मूलतः एक होते हुए भी उत्तरप्रक्रियाओं व बाह्य स्वरूप की अपेक्षा विविध रूपों में प्रतीत होता है।
ये उपयुक्त विविध रूप हमें तीन मूलधाराओं में मिलते हैं, वे धाराएं है-(१) वैरिक (२) बौद्ध एवं (३) जैन धारा।
ऋग्वेद में जहां योग संयोग अर्थों में मिलता है वहीं उपनिषदों विशेषकर पातञ्जलयोगदर्शन में आगत ध्यान एवं समाधि योग को ही दर्शाते हैं। इस तरह वैदिक दर्शन में योग से संयोग एवं ध्यान समाधि दोनों ही अर्थ अभिप्रेत हैं।
वस्तुतः योग का अत्यन्त परिष्कृत रूप हमें गीता में दृष्टिगोचर होता है । गीता में श्रीकृष्ण ने दो प्रकार को निष्ठा बतलाई है । ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा इस अपेक्षा से योग भी दो प्रकार का है-ज्ञानयोग एवं कर्मयोग। भक्तियोग इन दोनों में ही समाविष्ट हैं क्योंकि बिना भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के न तो ज्ञानार्जन हो सकता है और न ही कर्म कौशल्य प्रकट हो सकता है । अतएव भक्ति और कर्म में ही अनुस्यूत है।
__ बौद्ध दर्शन में भगवान् बुद्ध ने महर्षि पतञ्जलि की तरह आर्य अष्टाङ्गिकमार्ग की प्रबल प्रेरणा दो है। बौद्धाचार्यों ने अपनी कृतियों में सम्यक् समाधि, ध्यान व योग पर इसी अष्टाङ्गिक मार्ग में विस्तृत प्रकाश
Jain Education International 2010_03
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org