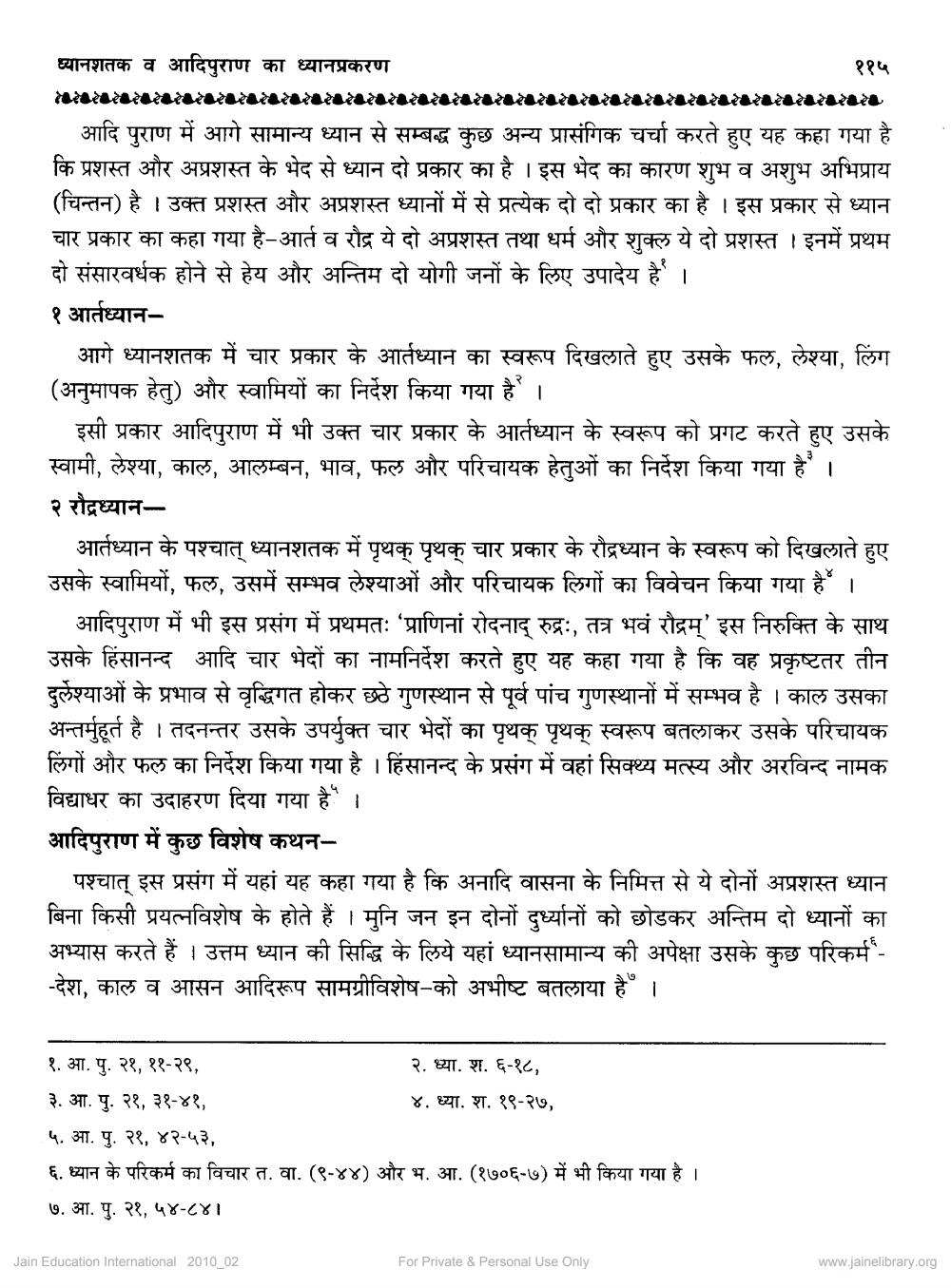________________
ध्यानशतक व आदिपुराण का ध्यानप्रकरण
११५ પ્રખે 2002 2 પ્રસરે રે
રે રે રે ? __ आदि पुराण में आगे सामान्य ध्यान से सम्बद्ध कुछ अन्य प्रासंगिक चर्चा करते हुए यह कहा गया है कि प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से ध्यान दो प्रकार का है । इस भेद का कारण शुभ व अशुभ अभिप्राय (चिन्तन) है । उक्त प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यानों में से प्रत्येक दो दो प्रकार का है । इस प्रकार से ध्यान चार प्रकार का कहा गया है-आर्त व रौद्र ये दो अप्रशस्त तथा धर्म और शुक्ल ये दो प्रशस्त । इनमें प्रथम दो संसारवर्धक होने से हेय और अन्तिम दो योगी जनों के लिए उपादेय है। १ आर्तध्यान
आगे ध्यानशतक में चार प्रकार के आर्तध्यान का स्वरूप दिखलाते हुए उसके फल, लेश्या, लिंग (अनुमापक हेतु) और स्वामियों का निर्देश किया गया है ।
इसी प्रकार आदिपुराण में भी उक्त चार प्रकार के आर्तध्यान के स्वरूप को प्रगट करते हुए उसके स्वामी, लेश्या, काल, आलम्बन, भाव, फल और परिचायक हेतुओं का निर्देश किया गया है। २ रौद्रध्यान
आर्तध्यान के पश्चात् ध्यानशतक में पृथक् पृथक् चार प्रकार के रौद्रध्यान के स्वरूप को दिखलाते हुए उसके स्वामियों, फल, उसमें सम्भव लेश्याओं और परिचायक लिगों का विवेचन किया गया है ।
आदिपुराण में भी इस प्रसंग में प्रथमतः ‘प्राणिनां रोदनाद् रुद्रः, तत्र भवं रौद्रम्' इस निरुक्ति के साथ उसके हिंसानन्द आदि चार भेदों का नामनिर्देश करते हुए यह कहा गया है कि वह प्रकृष्टतर तीन दुर्लेश्याओं के प्रभाव से वृद्धिगत होकर छठे गुणस्थान से पूर्व पांच गुणस्थानों में सम्भव है । काल उसका अन्तर्मुहूर्त है । तदनन्तर उसके उपर्युक्त चार भेदों का पृथक् पृथक् स्वरूप बतलाकर उसके परिचायक लिंगों और फल का निर्देश किया गया है । हिंसानन्द के प्रसंग में वहां सिक्थ्य मत्स्य और अरविन्द नामक विद्याधर का उदाहरण दिया गया है । आदिपुराण में कुछ विशेष कथन
पश्चात् इस प्रसंग में यहां यह कहा गया है कि अनादि वासना के निमित्त से ये दोनों अप्रशस्त ध्यान बिना किसी प्रयत्नविशेष के होते हैं । मुनि जन इन दोनों दुानों को छोडकर अन्तिम दो ध्यानों का अभ्यास करते हैं । उत्तम ध्यान की सिद्धि के लिये यहां ध्यानसामान्य की अपेक्षा उसके कुछ परिकर्म-देश, काल व आसन आदिरूप सामग्रीविशेष-को अभीष्ट बतलाया है ।
१. आ. पु. २१, ११-२९,
२. ध्या. श. ६-१८, ३. आ. पु. २१, ३१-४१,
४. ध्या. श. १९-२७, ५. आ. पु. २१, ४२-५३, ६. ध्यान के परिकर्म का विचार त. वा. (९-४४) और भ. आ. (१७०६-७) में भी किया गया है । ७. आ. पु. २१, ५४-८४।
Jain Education International 2010_02
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org