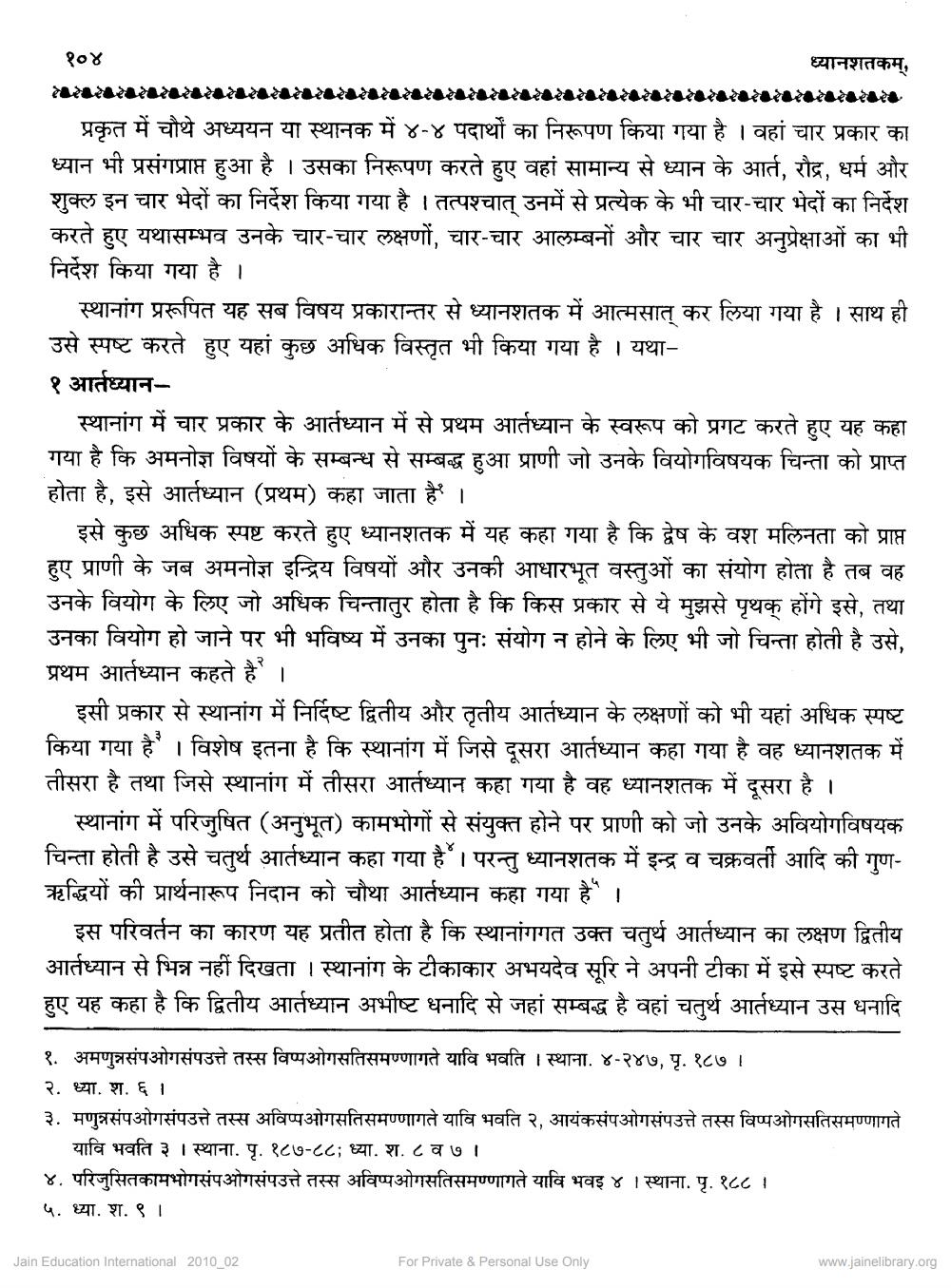________________
ध्यानशतकम्,
982228
प्रकृत में चौथे अध्ययन या स्थानक में ४-४ पदार्थों का निरूपण किया गया है । वहां चार प्रकार का ध्यान भी प्रसंगप्राप्त हुआ है । उसका निरूपण करते हुए वहां सामान्य से ध्यान के आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल इन चार भेदों का निर्देश किया गया है । तत्पश्चात् उनमें से प्रत्येक के भी चार-चार भेदों का निर्देश करते हुए यथासम्भव उनके चार-चार लक्षणों, चार-चार आलम्बनों और चार चार अनुप्रेक्षाओं का भी निर्देश किया गया है ।
१०४
स्थानांग प्ररूपित यह सब विषय प्रकारान्तर से ध्यानशतक में आत्मसात् कर लिया गया है । साथ ही उसे स्पष्ट करते हुए यहां कुछ अधिक विस्तृत भी किया गया है । यथा
१ आर्तध्यान
स्थानांग में चार प्रकार के आर्तध्यान में से प्रथम आर्तध्यान के स्वरूप को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि अमनोज्ञ विषयों के सम्बन्ध से सम्बद्ध हुआ प्राणी जो उनके वियोगविषयक चिन्ता को प्राप्त होता है, इसे आर्तध्यान ( प्रथम ) कहा जाता है ।
इसे कुछ अधिक स्पष्ट करते हुए ध्यानशतक में यह कहा गया है कि द्वेष के वश मलिनता को प्राप्त हुए प्राणी के जब अमनोज्ञ इन्द्रिय विषयों और उनकी आधारभूत वस्तुओं का संयोग होता है तब वह उनके वियोग के लिए जो अधिक चिन्तातुर होता है कि किस प्रकार से ये मुझसे पृथक् होंगे इसे, तथा उनका वियोग हो जाने पर भी भविष्य में उनका पुनः संयोग न होने के लिए भी जो चिन्ता होती है उसे, प्रथम आर्तध्यान कहते है ।
इसी प्रकार से स्थानांग में निर्दिष्ट द्वितीय और तृतीय आर्तध्यान के लक्षणों को भी यहां अधिक स्पष्ट किया गया है । विशेष इतना है कि स्थानांग में जिसे दूसरा आर्तध्यान कहा गया है वह ध्यानशतक में तीसरा है तथा जिसे स्थानांग में तीसरा आर्तध्यान कहा गया है वह ध्यानशतक में दूसरा है I
स्थानांग में परिजुषित (अनुभूत) कामभोगों से संयुक्त होने पर प्राणी को जो उनके अवियोगविषयक चिन्ता होती है उसे चतुर्थ आर्तध्यान कहा गया है । परन्तु ध्यानशतक में इन्द्र व चक्रवर्ती आदि की गुणऋद्धियों की प्रार्थनारूप निदान को चौथा आर्तध्यान कहा गया है ।
इस परिवर्तन का कारण यह प्रतीत होता है कि स्थानांगगत उक्त चतुर्थ आर्तध्यान का लक्षण द्वितीय आर्तध्यान से भिन्न नहीं दिखता । स्थानांग के टीकाकार अभयदेव सूरि ने अपनी टीका में इसे स्पष्ट करते यह कहा है कि द्वितीय आर्तध्यान अभीष्ट धनादि से जहां सम्बद्ध है वहां चतुर्थ आर्तध्यान उस धनाद
१. अमणुन्नसंपओगसंपत्ते तस्स विप्पओगसतिसमण्णागते यावि भवति । स्थाना. ४-२४७, पृ. १८७ ।
२. ध्या. श. ६ |
३. मणुन्नसंपओगसंपत्ते तस्स अविप्पओगसतिसमण्णागते यावि भवति २, आयंकसंपओगसंपउत्ते तस्स विप्पओगसतिसमण्णागते यावि भवति ३ । स्थाना. पृ. १८७-८८; ध्या. श. ८ व ७ ।
४. परिजुसितकामभोगसंपओगसंपत्ते तस्स अविप्पओगसतिसमण्णागते यावि भवइ ४ । स्थाना. पृ. १८८ ।
५. ध्या. श. ९ ।
Jain Education International 2010_02
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org