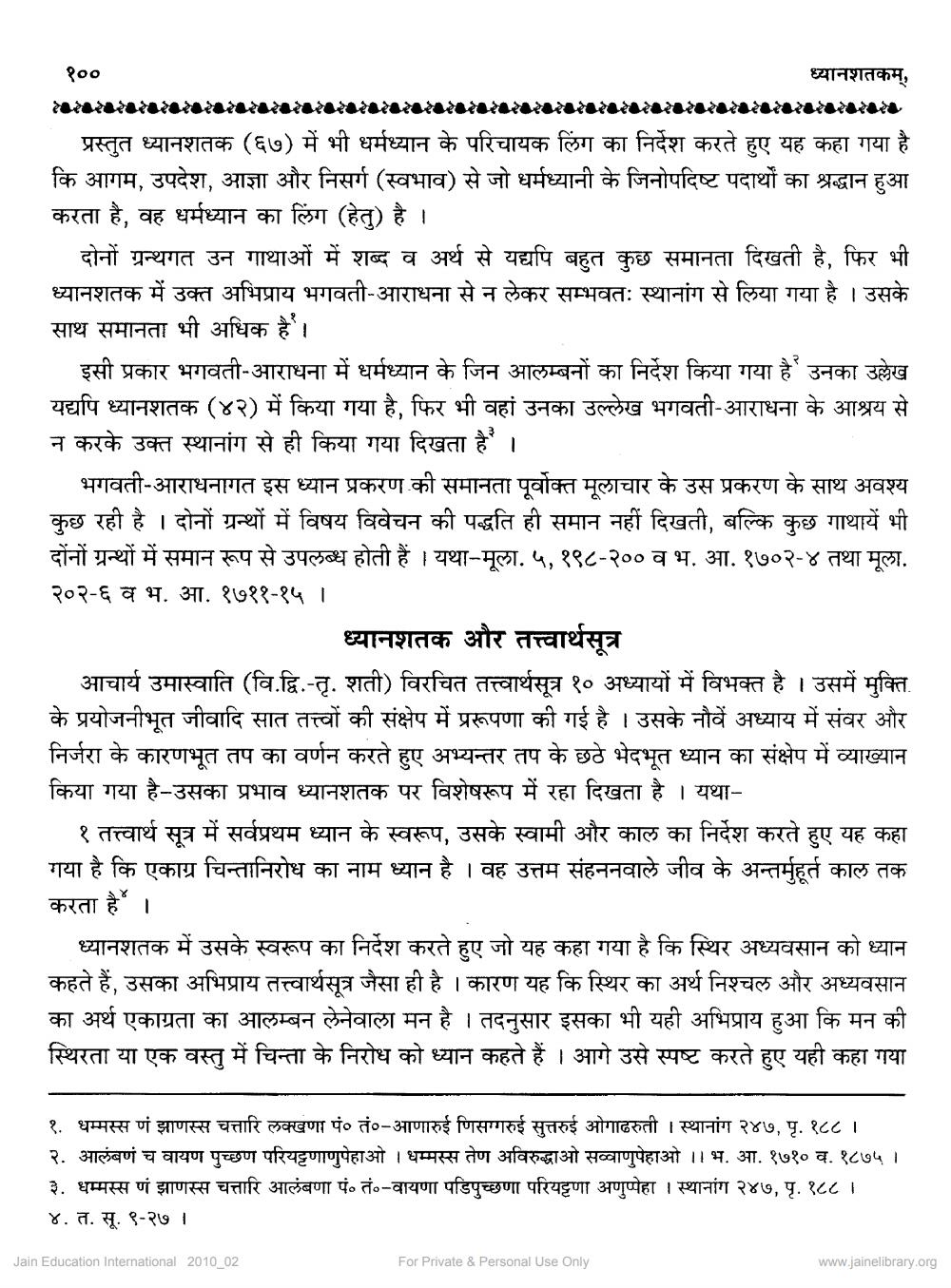________________
१००
ध्यानशतकम्,
प्रस्तुत ध्यानशतक (६७) में भी धर्मध्यान के परिचायक लिंग का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि आगम, उपदेश, आज्ञा और निसर्ग (स्वभाव) से जो धर्मध्यानी के जिनोपदिष्ट पदार्थों का श्रद्धान हुआ करता है, वह धर्मध्यान का लिंग (हेतु) है ।
दोनों ग्रन्थगत उन गाथाओं में शब्द व अर्थ से यद्यपि बहुत कुछ समानता दिखती है, फिर भी ध्यानशतक में उक्त अभिप्राय भगवती-आराधना से न लेकर सम्भवतः स्थानांग से लिया गया है । उसके साथ समानता भी अधिक है।
इसी प्रकार भगवती-आराधना में धर्मध्यान के जिन आलम्बनों का निर्देश किया गया है उनका उल्लेख यद्यपि ध्यानशतक (४२) में किया गया है, फिर भी वहां उनका उल्लेख भगवती-आराधना के आश्रय से न करके उक्त स्थानांग से ही किया गया दिखता है ।
भगवती-आराधनागत इस ध्यान प्रकरण की समानता पूर्वोक्त मूलाचार के उस प्रकरण के साथ अवश्य कुछ रही है । दोनों ग्रन्थों में विषय विवेचन की पद्धति ही समान नहीं दिखती, बल्कि कुछ गाथायें भी दोनों ग्रन्थों में समान रूप से उपलब्ध होती हैं । यथा-मूला. ५, १९८-२०० व भ. आ. १७०२-४ तथा मूला. २०२-६ व भ. आ. १७११-१५ ।।
__ध्यानशतक और तत्त्वार्थसूत्र आचार्य उमास्वाति (वि.द्वि.-तृ. शती) विरचित तत्त्वार्थसूत्र १० अध्यायों में विभक्त है । उसमें मुक्ति के प्रयोजनीभूत जीवादि सात तत्त्वों की संक्षेप में प्ररूपणा की गई है । उसके नौवें अध्याय में संवर और निर्जरा के कारणभूत तप का वर्णन करते हुए अभ्यन्तर तप के छठे भेदभूत ध्यान का संक्षेप में व्याख्यान किया गया है-उसका प्रभाव ध्यानशतक पर विशेषरूप में रहा दिखता है । यथा
१ तत्त्वार्थ सूत्र में सर्वप्रथम ध्यान के स्वरूप, उसके स्वामी और काल का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि एकाग्र चिन्तानिरोध का नाम ध्यान है । वह उत्तम संहननवाले जीव के अन्तर्मुहूर्त काल तक करता है ।
ध्यानशतक में उसके स्वरूप का निर्देश करते हुए जो यह कहा गया है कि स्थिर अध्यवसान को ध्यान कहते हैं, उसका अभिप्राय तत्त्वार्थसूत्र जैसा ही है । कारण यह कि स्थिर का अर्थ निश्चल और अध्यवसान का अर्थ एकाग्रता का आलम्बन लेनेवाला मन है । तदनुसार इसका भी यही अभिप्राय हुआ कि मन की स्थिरता या एक वस्तु में चिन्ता के निरोध को ध्यान कहते हैं । आगे उसे स्पष्ट करते हुए यही कहा गया
१. धम्मस्स णं झाणस्स चत्तारि लक्खणा पं० तं०-आणारुई णिसग्गरुई सुत्तरुई ओगाढरुती । स्थानांग २४७, पृ. १८८ । २. आलंबणं च वायण पुच्छण परियट्टणाणुपेहाओ । धम्मस्स तेण अविरुद्धाओ सव्वाणुपेहाओ ।। भ. आ. १७१० व. १८७५ । ३. धम्मस्स णं झाणस्स चत्तारि आलंबणा पं० तं०-वायणा पडिपुच्छणा परियट्टणा अणुप्पेहा । स्थानांग २४७, पृ. १८८ । ४. त. सू. ९-२७ ।
Jain Education International 2010_02
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org