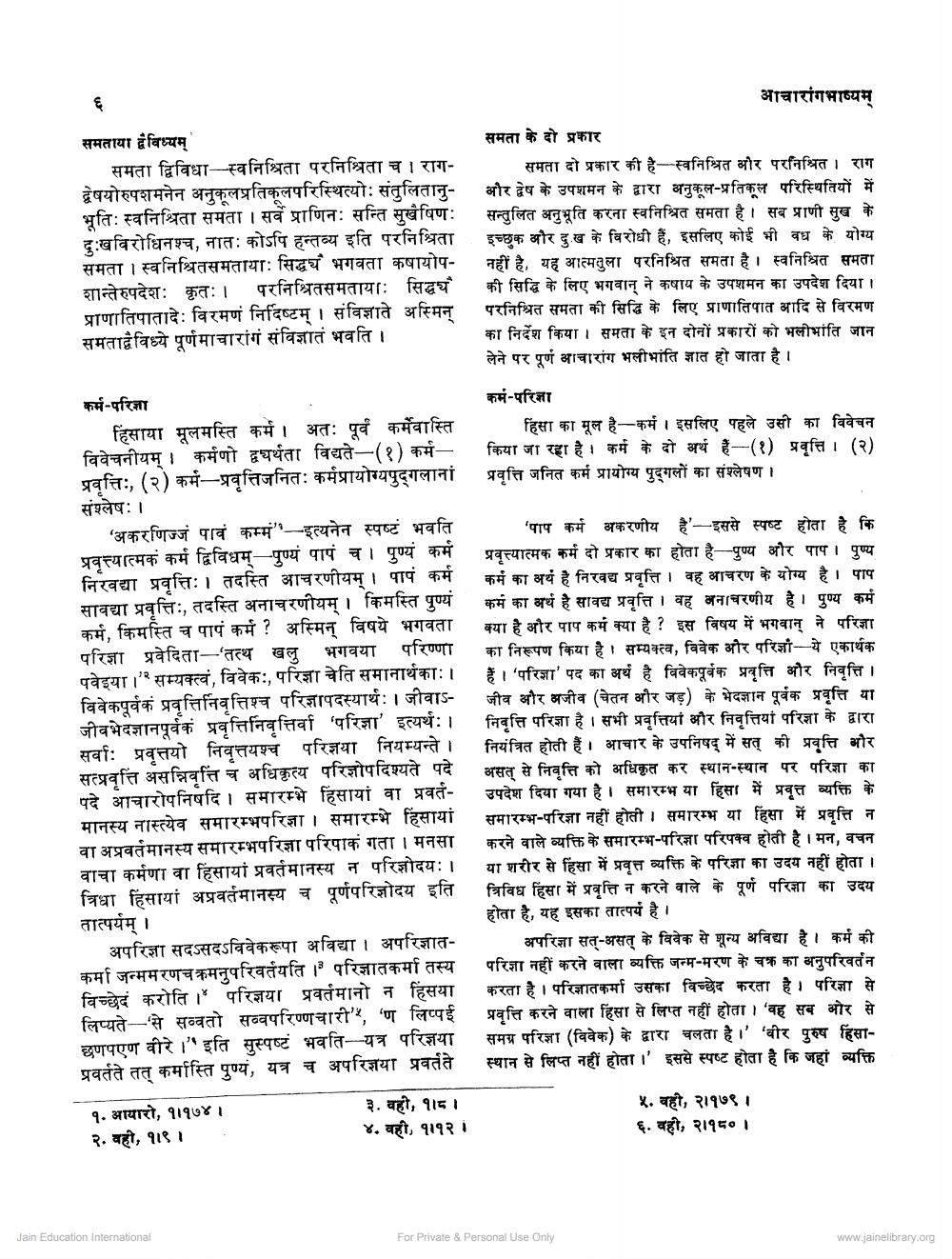________________
समताया द्वैविध्यम्'
समता द्विविधा स्वनिश्रिता परनिश्रिता च । रागद्वेषयोपशमनेन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थित्योः संतुलितानुभूतिः स्वनिश्रिता समता । सर्वे प्राणिनः सन्ति सुखैषिण: दुःखविरोधिनश्च नातः कोऽपि हन्तव्य इति परनिचिता समता। स्वनिधितसमताया: सिद्ध भगवता कषायोप शान्तेरुपदेशः कृतः । परनिधितसमताया: सिद्धर्ष प्राणातिपातादेः विरमणं निर्दिष्टम्। संविज्ञाते अस्मिन् समताईविध्ये पूर्णमाचारांग संविज्ञातं भवति ।
कर्म - परिज्ञा
।
हिंसाया मूलमस्ति कर्म अतः पूर्व कर्मेवास्ति विवेचनीयम् । कर्मणो द्वघर्थता विद्यते - (१) कर्मप्रवृत्तिः, (२) कर्म-प्रवृत्तिजनितः कर्मप्रायोग्यपुद्गलानां संश्लेषः ।
1
'अकरणिज्जं पावं कम्म" इत्यनेन स्पष्टं भवति प्रवृत्यात्मकं कर्म द्विविधम् पुण्यं पापं च पुण्यं कर्म निरवद्या प्रवृत्तिः । तदस्ति आचरणीयम् । पाप कर्म सावद्या प्रवृत्तिः, तदस्ति अनाचरणीयम् । किमस्ति पुण्यं कर्म, किमस्ति च पापं कर्म ? अस्मिन् विषये भगवता भगवया परिणा परिक्षा प्रवेदिता-तरथ खलु पवेश्या" सम्यक्त्वं, विवेक, परिक्षा चेति समानार्थकाः । विवेकपूर्वक प्रवृत्तिनिवृत्तिएव परिज्ञापदस्यार्थः । जीवाजीवभेदज्ञानपूर्वकं प्रवृत्तिनिवृत्तिर्वा 'परिक्षा' इत्यर्थः । सर्वाः प्रवृत्तयो निवृत्तयएवं परिशया नियम्यन्ते । सत्प्रवृत्ति असन्निवृत्ति च अधिकृत्य परिज्ञोपदिश्यते पदे पदे आचारोपनिषदि समारम्भे हिंसायां वा प्रवर्त मानस्य नास्त्येव समारम्भपरिक्षा समारम्भे हिंसायां वा अप्रवर्तमानस्य समारम्भपरिज्ञा परिपाकं गता मनसा बाचा कर्मणा वा हिंसायां प्रवर्तमानस्य न परिज्ञोदमः । विधा हिंसायां अप्रवर्तमानस्य च पूर्णपरिज्ञोदय इति तात्पर्यम् ।
1
अपरिज्ञा सदसदविवेकरुपा अविद्या। अपरिज्ञातकर्मा जन्ममरणच कमनुपरिवर्तयति । परिशातकर्मा तस्य विच्छेदं करोति । परिज्ञया प्रवर्तमानो न हिंसया लिप्यते-से सम्यतो सम्वपरिष्णवारी 'ण लिप्पई छणपण वीरे ।" इति सुस्पष्टं भवति-यत्र परिज्ञया प्रवर्तते तत् कर्मास्ति पुण्यं यत्र च अपरिज्ञया प्रवर्तते
१. आयारो, १।१७४ । २. वही, १९ ॥
Jain Education International
३. वही, ११८ ॥
४. वही, १३१२ ।
समता के दो प्रकार
समता दो प्रकार की है-स्वनिश्रित और परनिश्रित । राग और द्वेष के उपशमन के द्वारा अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में सन्तुलित अनुभूति करना स्वनिश्रित समता है । सब प्राणी सुख के इच्छुक और दुःख के विरोधी है, इसलिए कोई भी वध के योग्य नहीं है, यह आत्मतुला परनिश्रित समता है। स्वनिश्रित समता की सिद्धि के लिए भगवान् ने कषाय के उपशमन का उपदेश दिया । परनिश्रित समता की सिद्धि के लिए प्राणातिपात आदि से विरमण का निर्देश किया। समता के इन दोनों प्रकारों को भलीभांति जान लेने पर पूर्ण आचारांग भलीभांति ज्ञात हो जाता है ।
आचारांगभाष्यम्
कर्म - परिज्ञा
हिंसा का मूल है-कर्म इसलिए पहले उसी का विवेचन किया जा रहा है। कर्म के दो अर्थ है– (१) प्रवृत्ति (२) प्रवृत्ति जनित कर्म प्रायोग्य पुद्गलों का संश्लेषण ।
'पाप कर्म अकरणीय है' — इससे स्पष्ट होता है कि कर्म दो प्रकार का होता है—पुण्य और पाप पुण्य प्रवृत्त्यात्मक कर्म का अर्थ है निरवद्य प्रवृत्ति। वह आचरण के योग्य है । पाप कर्म का अर्थ है सावद्य प्रवृत्ति । वह अनाचरणीय है । पुण्य कर्म क्या है और पाप कर्म क्या है ? इस विषय में भगवान् ने परिज्ञा का निरूपण किया है। सम्यक्त्व, विवेक और परिज्ञां-ये एकार्थक हैं। 'परिज्ञा' पद का अर्थ है विवेकपूर्वक प्रवृत्ति और निवृत्ति । जीव और अजीव (चेतन और जड़) के भेदज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति परिक्षा है। सभी प्रवृत्तियां और निवृत्तियां परिज्ञा के द्वारा नियंत्रित होती है। आचार के उपनिषद् में सत् की प्रवृत्ति और असत् से निवृत्ति को अधिकृत कर स्थान-स्थान पर परिज्ञा का उपदेश दिया गया है। समारम्भ या हिंसा में प्रवृत्त व्यक्ति के समारम्भ-परिज्ञा नहीं होती। समारम्भ या हिंसा में प्रवृत्ति न करने वाले व्यक्ति के समारम्भ-परिज्ञा परिपक्व होती है। मन, वचन या शरीर से हिंसा में प्रवृत्त व्यक्ति के परिज्ञा का उदय नहीं होता । त्रिविध हिंसा में प्रवृत्ति न करने वाले के पूर्ण परिज्ञा का उदय होता है, यह इसका तात्पर्य है ।
अपरिज्ञा सत् असत् के विवेक से शून्य अविद्या है। कर्म की परिज्ञा नहीं करने वाला व्यक्ति जन्म-मरण के चक्र का अनुपरिवर्तन करता है। परिज्ञातकर्मा उसका विच्छेद करता है। परिज्ञा से प्रवृत्ति करने वाला हिंसा से लिप्त नहीं होता। यह सब जोर से समग्र परिज्ञा (विवेक) के द्वारा चलता है।' 'वीर पुरुष हिंसास्थान से लिप्त नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि जहाँ व्यक्ति
For Private & Personal Use Only
५. वही, २।१७९ ।
६. वही, २।१५० ।
www.jainelibrary.org