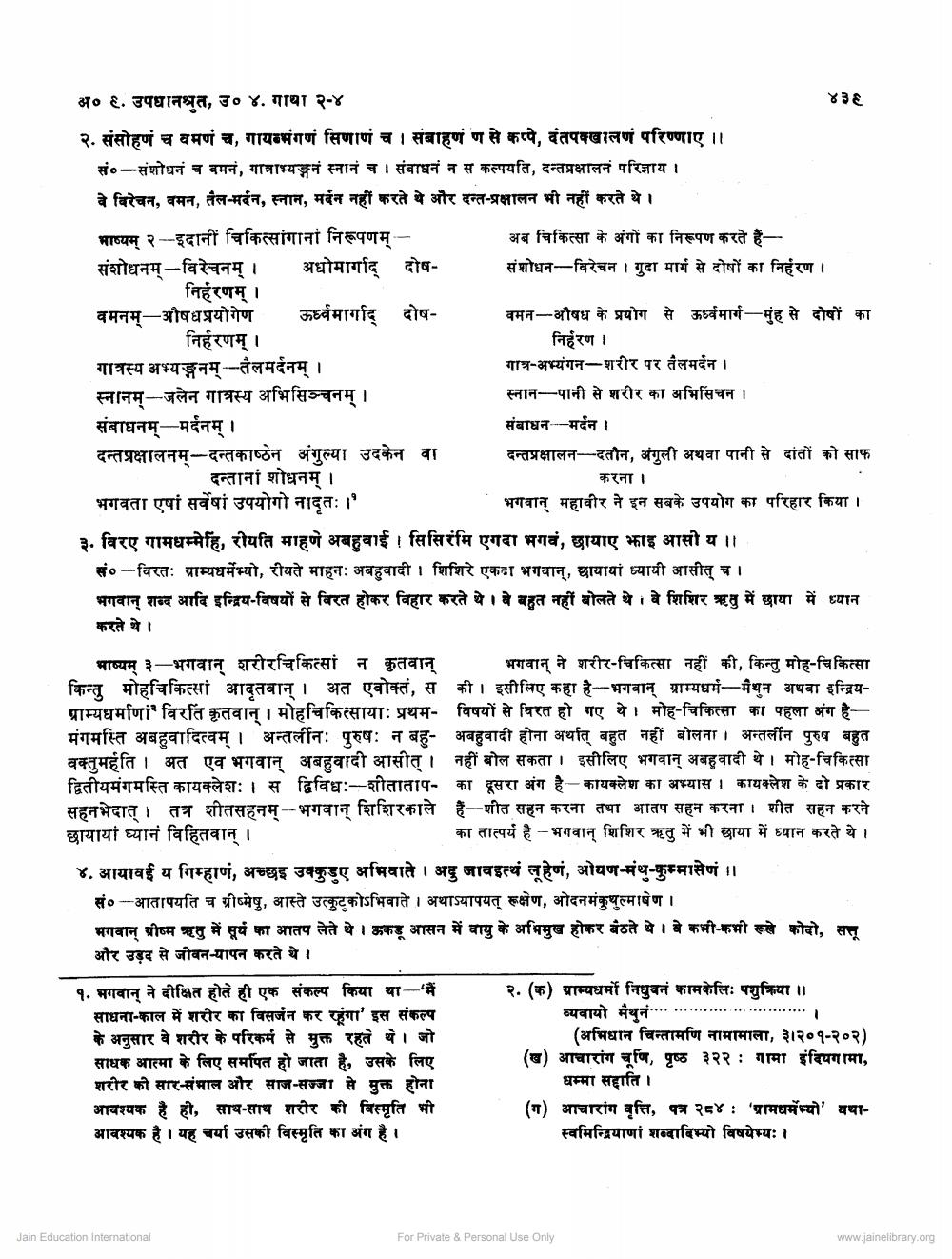________________
अ० ६. उपधानश्रुत, उ० ४. गाथा २-४
२. संसोहणं च वमणं च, गाय मंगणं सिणाणं च । संबाहणं ण से कप्पे, वंतपक्खालणं परिण्णाए || सं० - संशोधनं च वमनं, गात्राभ्यङ्गनं स्नानं च संबाधनं न स कल्पयति, दन्तप्रक्षालनं परिज्ञाय । वे विरेचन, वमन, तैल-मर्दन, स्नान, मर्दन नहीं करते थे और दन्त-प्रक्षालन भी नहीं करते थे ।
भाष्यम् २ -- इदानीं चिकित्सांगानां निरूपणम्
संशोधनम् - विरेचनम् । निर्हरणम् । वमनम् - औषध प्रयोगेण
निर्हरणम् ।
गात्रस्य अभ्यङ्गनम् तैलमर्दनम् ।
स्नानम् - जलेन गात्रस्य अभिसिञ्चनम् ।
संबाधनम् —–मर्दनम् ।
अधोमार्गाद् दोष
ऊर्ध्वमार्गाद्
दोष
दन्तप्रक्षालनम् - दन्तकाष्ठेन अंगुल्या उदकेन वा
दन्तानां शोधनम् ।
भगवता एषां सर्वेषां उपयोगो नादृतः ।
P
1
भाष्यम् ३ – भगवान् शरीरचिकित्सां न कृतवान् किन्तु मोहचिकित्सां आवृतवान्। अत एवोक्तं स ग्राम्यधर्माणां विरति कृतवान् । मोहचिकित्सायाः प्रथम मंगमस्ति अबहुवादित्वम् अन्तर्लीनः पुरुषः न बहू वक्तुमर्हति । अत एव भगवान् अबहुवादी आसीत् । द्वितीयमंगमस्ति कायक्लेशः । स द्विविधः शीताताप सहनभेदात् । तत्र शीतसहनम् - भगवान् शिशिरकाले छायायां ध्यानं विहितवान् ।
अब चिकित्सा के अंगों का निरूपण करते हैंसंशोधन - विरेचन । गुदा मार्ग से दोषों का निर्हरण ।
३. विरए गामधम्मेहि, रोयति माहणे अबहुवाई । सिसिरंमि एगदा भगवं, छायाए भाइ आसी य ॥ सं० – विरतः ग्राम्यधर्मेभ्यो रीयते माहून अबहुवादी शिशिरे एकदा भगवान्, छायायां ध्यायी आसीत् च ।
भगवान् शब्द आदि इन्द्रिय-विषयों से विरत होकर विहार करते थे। वे बहुत नहीं बोलते थे। वे शिशिर ऋतु में छाया में ध्यान करते थे ।
Jain Education International
१. भगवान् ने दीक्षित होते ही एक संकल्प किया था-'मैं साधना काल में शरीर का विसर्जन कर रहूंगा' इस संकल्प के अनुसार वे शरीर के परिकर्म से मुक्त रहते थे। जो साधक आत्मा के लिए समर्पित हो जाता है, उसके लिए शरीर की सार-संभाल और साज-सज्जा से मुक्त होना आवश्यक है ही, साथ-साथ शरीर की विस्मृति भी आवश्यक है। यह चर्या उसकी विस्मृति का अंग है ।
वमन – औषध के प्रयोग से ऊर्ध्वमार्ग- मुंह से दोषों का निर्हरण |
गात्र - अभ्यंगन - शरीर पर तैलमर्दन ।
स्नान—पानी से शरीर का अभिसिंचन ।
संबाधन मर्दन ।
दन्तप्रक्षालन - दतीन, अंगुली अथवा पानी से दांतों को साफ
करना ।
भगवान् महावीर ने इन सबके उपयोग का परिहार किया ।
४. आयावई य गिम्हाणं, अच्छइ उक्कुडुए अभिवाते । अदु जावइत्थं लूहेणं, ओयण-मंथु कुम्मासेणं ॥ सं० - आतापयति च ग्रीष्मेषु, आस्ते उत्कुटुकोऽभिवाते । अथाऽयापयत् रूक्षेण, ओदनमंकुथुल्माषेण ।
भगवान् ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का आतप लेते थे । ठकडू आसन में वायु के अभिमुख होकर बैठते थे । वे कभी-कभी रूले कोदो, और उड़द से जीवन-यापन करते थे ।
की
भगवान् ने शरीर चिकित्सा नहीं की, किन्तु मोह - चिकित्सा इसीलिए कहा है भगवान् ग्राम्यधर्म-मैथुन अथवा इन्द्रियविषयों से विरत हो गए थे मोह-चिकित्सा का पहला अंग हैअबहुवादी होना अर्थात् बहुत नहीं बोलना अन्तलींग पुरुष बहुत नहीं बोल सकता। इसीलिए भगवान् अबहुवादी थे । मोह-चिकित्सा का दूसरा अंग है— कायक्लेश का अभ्यास कायक्लेश के दो प्रकार हैं—शीत सहन करना तथा आतप सहन करना। शीत सहन करने का तात्पर्य है - भगवान् शिशिर ऋतु में भी छाया में ध्यान करते थे ।
૪૩૨
२. (क) ग्राम्यधर्मो निधुवनं कामकेलिः पशुक्रिया ॥ व्यवायो मैथुन.....
HONOURINORING ME ----
For Private & Personal Use Only
सत्तू
( अभिधान चिन्तामणि नामामाला, ३।२०१-२०२ ) (ख) आचारांग चूणि, पृष्ठ ३२२ : गामा इंदियगामा, धम्मा सद्दाति ।
(ग) आचारांग वृत्ति, पत्र २८४ : 'ग्रामधर्मेभ्यो' यथास्वमिन्द्रियाणां शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः ।
www.jainelibrary.org