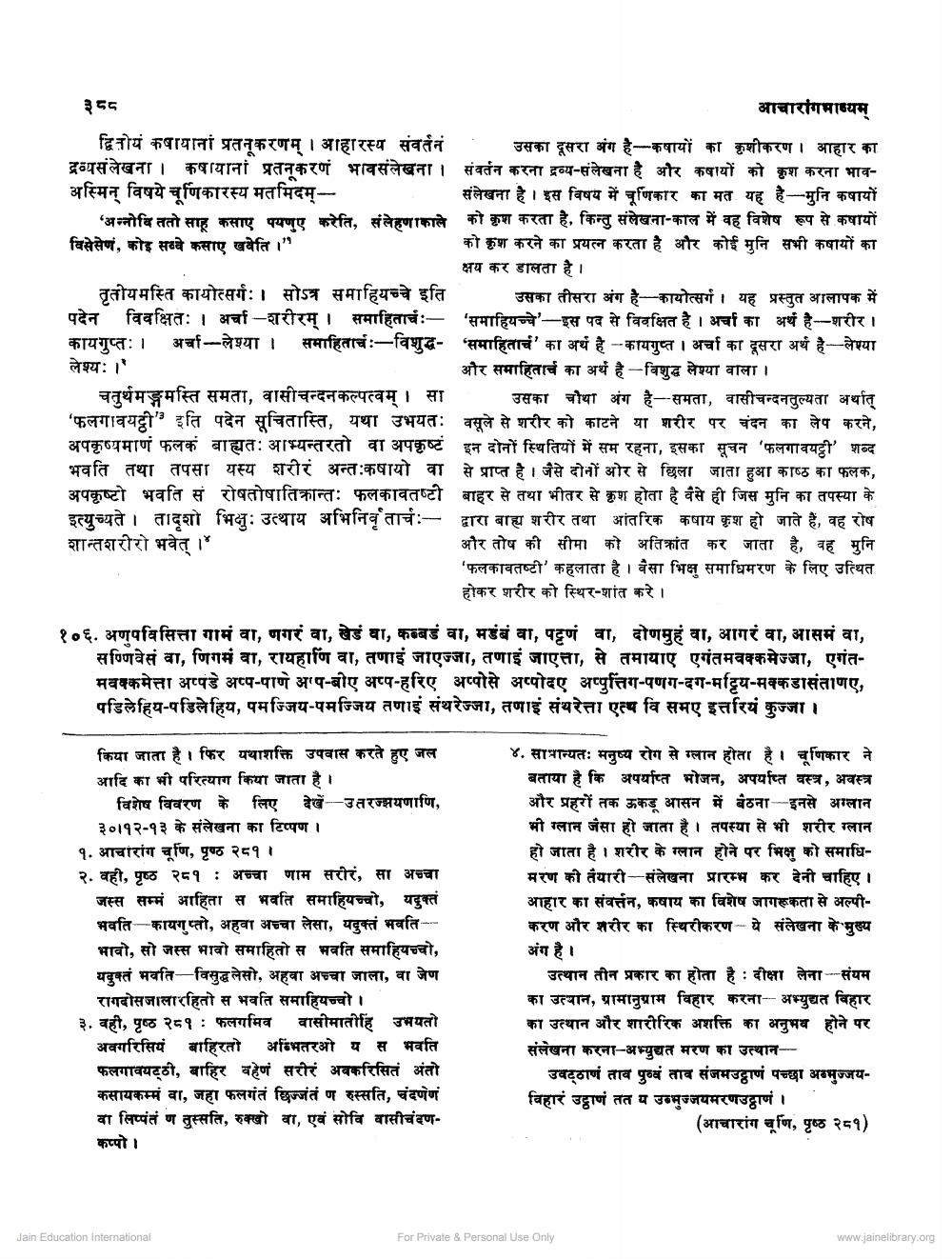________________
३८८
आचारांगभाष्यम् द्वितीयं कषायानां प्रतनूकरणम् । आहारस्य संवर्तनं उसका दूसरा अंग है-कषायों का कृशीकरण । आहार का द्रव्यसंलेखना। कषायानां प्रतनकरणं भावसंलेखना। संवर्तन करना द्रव्य-संलेखना है और कषायों को कृश करना भावअस्मिन् विषये चुणिकारस्य मतमिदम्-
संलेखना है । इस विषय में चूर्णिकार का मत यह है-मुनि कषायों 'अन्नोवि ततो साहू कसाए पयणुए करेति, संलेहणाकाले को कृश करता है, किन्तु संलेखना-काल में वह विशेष रूप से कषायों विसेसेणं, कोइ सब्वे कसाए खवेति ।"
को कृश करने का प्रयत्न करता है और कोई मुनि सभी कषायों का
क्षय कर डालता है। तृतीयमस्ति कायोत्सर्गः। सोऽत्र समाहियच्चे इति उसका तीसरा अंग है-कायोत्सर्ग। यह प्रस्तुत आलापक में पदेन विवक्षितः । अर्चा -शरीरम् । समाहितार्चः- 'समाहियच्चे'-इस पद से विवक्षित है । अर्चा का अर्थ है-शरीर । कायगुप्तः । अर्चा-लेश्या । समाहितार्च:-विशुद्ध- 'समाहितार्च' का अर्थ है --कायगुप्त । अर्चा का दूसरा अर्थ है-लेश्या लेश्यः ।
और समाहितार्च का अर्थ है -विशुद्ध लेश्या वाला। __ चतुर्थमङ्गमस्ति समता, वासीचन्दनकल्पत्वम् । सा उसका चौथा अंग है-समता, वासीचन्दनतुल्यता अर्थात् 'फलगावयट्ठी' इति पदेन सूचितास्ति, यथा उभयतः वसूले से शरीर को काटने या शरीर पर चंदन का लेप करने, अपकृष्यमाणं फलकं बाह्यत: आभ्यन्तरतो वा अपकृष्टं इन दोनों स्थितियों में सम रहना, इसका सूचन 'फलगावयट्ठी' शब्द भवति तथा तपसा यस्य शरीरं अन्त:कषायो वा से प्राप्त है। जैसे दोनों ओर से छिला जाता हुआ काष्ठ का फलक, अपकृष्टो भवति सं रोषतोषातिक्रान्तः फलकावतष्टी बाहर से तथा भीतर से कृश होता है वैसे ही जिस मुनि का तपस्या के इत्युच्यते। तादृशो भिक्षुः उत्थाय अभिनितार्चः- द्वारा बाह्य शरीर तथा आंतरिक कषाय कृश हो जाते हैं, वह रोष शान्तशरीरो भवेत् ।
और तोष की सीमा को अतिक्रांत कर जाता है, वह मुनि 'फलकावतष्टी' कहलाता है। वैसा भिक्षु समाधिमरण के लिए उत्थित होकर शरीर को स्थिर-शांत करे।
१०६. अणपविसित्ता गाम वा, जगरं वा, खेडं वा, कब्बडं वा, मडंबं वा, पट्टणं वा, दोणमुहं वा, आगरं वा, आसमं वा,
सण्णिवेसं वा, णिगमं वा, रायहाणि वा, तणाई जाएज्जा, तणाई जाएत्ता, से तमायाए एगंतमवक्कमेज्जा, एगंतमवक्कमेत्ता अप्पडे अप्प-पाणे अप-बीए अप्प-हरिए अप्पोसे अप्पोदए अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडासंताणए, पडिलेहिय-पडिलेहिय, पमज्जिय-पमज्जिय तणाई संथरेज्जा, तणाई संयरेत्ता एत्य वि समए इत्तरियं कुज्जा।
किया जाता है। फिर यथाशक्ति उपवास करते हुए जल आदि का भी परित्याग किया जाता है ।
विशेष विवरण के लिए देखें-उतरज्झयणाणि, ३०१२-१३ के संलेखना का टिप्पण । १. आचारांग चूणि, पृण्ठ २८१ । २. वही, पृष्ठ २८१ : अच्चा णाम सरीरं, सा अच्चा
जस्स सम्मं आहिता स भवति समाहियच्चो, यदुक्तं भवति-कायगुप्तो, अहवा अच्चा लेसा, यदुक्तं भवतिभावो, सो जस्स भावो समाहितो स भवति समाहियच्चो, यदुक्तं भवति–विसुद्धलेसो, अहवा अच्चा जाला, वा जेण
रागदोसजालारहितो स भवति समाहियच्चो। ३. वही, पृष्ठ २८१ : फलगमिव वासीमातीहि उभयतो
अवगरिसियं बाहिरतो अम्भितरओ य स भवति फलगावयट्ठी, बाहिर बहेणं सरीरं अवकरिसितं अंतो कसायकम्मं बा, जहा फलगंतं छिज्जतं ण रुस्सति, चंदणेणं वा लिप्पंतं ग तुस्सति, रुक्खो वा, एवं सोवि वासीचंदणकप्पो।
४. सामान्यतः मनुष्य रोग से ग्लान होता है। चूणिकार ने बताया है कि अपर्याप्त भोजन, अपर्याप्त वस्त्र, अवस्त्र और प्रहरों तक ऊकड़ आसन में बैठना-इनसे अग्लान भी ग्लान जैसा हो जाता है। तपस्या से भी शरीर ग्लान हो जाता है। शरीर के ग्लान होने पर भिक्षु को समाधिमरण की तैयारी-संलेखना प्रारम्भ कर देनी चाहिए। आहार का संवर्तन, कषाय का विशेष जागरूकता से अल्पीकरण और शरीर का स्थिरीकरण- ये संलेखना के मुख्य अंग है।
उत्थान तीन प्रकार का होता है : दीक्षा लेना--संयम का उत्थान, प्रामानुग्राम विहार करना-- अभ्युद्यत विहार का उत्थान और शारीरिक अशक्ति का अनुभव होने पर संलेखना करना-अभ्युद्यत मरण का उत्थान
उवट्ठाणं ताव पुव्वं ताव संजमउट्ठाणं पच्छा अग्भुज्जयविहारं उट्ठाणं तत य उम्भुज्जयमरणउट्ठाणं ।
(आचारांग चूणि, पृष्ठ २८१)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org