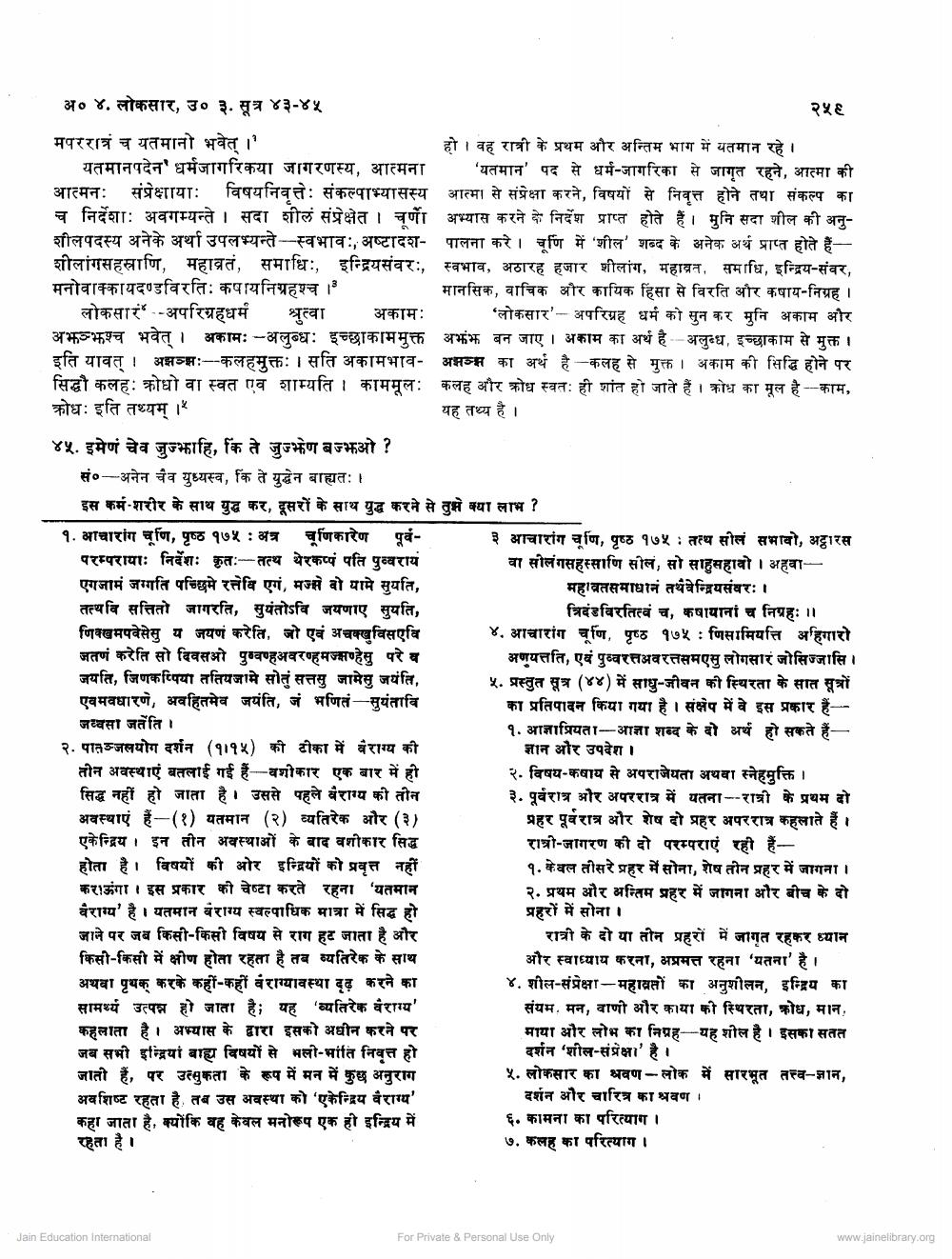________________
अ०४. लोकसार, उ० ३. सूत्र ४३-४५
२५६ मपररात्रं च यतमानो भवेत् ।'
हो । वह रात्री के प्रथम और अन्तिम भाग में यतमान रहे। यतमानपदेन' धर्मजागरिकया जागरणस्य, आत्मना 'यतमान' पद से धर्म-जागरिका से जागृत रहने, आत्मा की आत्मनः संप्रेक्षायाः विषयनिवृत्तेः संकल्पाभ्यासस्य आत्मा से संप्रेक्षा करने, विषयों से निवृत्त होने तथा संकल्प का च निर्देशा: अवगम्यन्ते । सदा शीलं संप्रेक्षेत । चूर्णी अभ्यास करने के निर्देश प्राप्त होते हैं। मुनि सदा शील की अनुशीलपदस्य अनेके अर्था उपलभ्यन्ते-स्वभावः, अष्टादश- पालना करे। चूणि में 'शील' शब्द के अनेक अर्थ प्राप्त होते हैंशीलांगसहस्राणि, महाव्रतं, समाधिः, इन्द्रियसंवरः, स्वभाव, अठारह हजार शीलांग, महाव्रत, समाधि, इन्द्रिय-संवर, मनोवाक्कायदण्डविरतिः कषायनिग्रहश्च ।
मानसिक, वाचिक और कायिक हिंसा से विरति और कषाय-निग्रह । ___ लोकसारं -अपरिग्रहधर्म श्रुत्वा अकामः 'लोकसार'- अपरिग्रह धर्म को सुन कर मुनि अकाम और अझञ्झश्च भवेत् । अकामः -अलुब्धः इच्छाकाममुक्त अझझ बन जाए। अकाम का अर्थ है - अलुब्ध, इच्छाकाम से मुक्त । इति यावत् । अझनः--कलहमुक्तः । सति अकामभाव- अझञ्झ का अर्थ है-कलह से मुक्त । अकाम की सिद्धि होने पर सिद्धौ कलहः क्रोधो वा स्वत एव शाम्यति । काममूलः कलह और क्रोध स्वतः ही शांत हो जाते हैं । क्रोध का मूल है-काम, क्रोधः इति तथ्यम् ।
यह तथ्य है। ४५. इमेणं चेव जुज्झाहि, कि ते जुझण बज्झओ?
सं०-अनेन चैव युध्यस्व, किं ते युद्धेन बाह्यतः । इस कर्म-शरीर के साथ युद्ध कर, दूसरों के साथ युद्ध करने से तुझे क्या लाभ ? १. आचारांग चूणि, पृष्ठ १७५ : अत्र चूणिकारेण पूर्व- ३ आचारांग चूणि, पृष्ठ १७५ : तत्थ सील सभावो, अट्ठारस परम्परायाः निर्देशः कृतः-तत्थ थेरकप्पं पति पुव्वराय
वा सोलंगसहस्साणि सील, सो साहुसहावो । अहवाएगजामं जग्गति पच्छिमे रत्तेवि एगं, मज्झे वो यामे सुयति,
महावतसमाधानं तथैवेन्द्रियसंवरः। तत्थवि सत्तितो जागरति, सुयंतोऽवि जयणाए सुयति,
त्रिदंडविरतित्वं च, कषायानां च निग्रहः ।। णिक्खमपवेसेसु य जयणं करेति, जो एवं अचक्खुविसएवि ४. आचारांग चूणि, पृष्ठ १७५ : णिसामियत्ति अहिगारो जतणं करेति सो दिवसओ पुग्वण्हअवरोहममण्हेसु परे व
अणुयत्तति, एवं पुश्वरत्तअवरत्तसमएसु लोगसार जोसिज्जासि । जयति, जिणकप्पिया ततियजामे सोतुं सत्तसु जामेसु जयंति, ५. प्रस्तुत सूत्र (४४) में साधु-जीवन की स्थिरता के सात सूत्रों एवमवधारणे, अवहितमेव जयंति, जं भणितं-सुयंतावि
का प्रतिपादन किया गया है । संक्षेप में वे इस प्रकार हैं--- जव्वसा जतेंति।
१. आज्ञाप्रियता-आज्ञा शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं२. पातञ्जलयोग दर्शन (१।१५) की टीका में वैराग्य की
ज्ञान और उपदेश। तीन अवस्थाएं बतलाई गई हैं-वशीकार एक बार में ही
२. विषय-कषाय से अपराजेयता अथवा स्नेहमुक्ति । सिद्ध नहीं हो जाता है। उससे पहले वैराग्य की तीन
३. पूर्वरात्र और अपररात्र में यतना--रात्री के प्रथम दो अवस्थाएं हैं-(१) यतमान (२) व्यतिरेक और (३)
प्रहर पूर्वरात्र और शेष दो प्रहर अपररात्र कहलाते हैं। एकेन्द्रिय। इन तीन अवस्थाओं के बाद वशीकार सिद्ध
रात्री-जागरण की दो परम्पराएं रही हैंहोता है। विषयों की ओर इन्द्रियों को प्रवृत्त नहीं
१. केवल तीसरे प्रहर में सोना, शेष तीन प्रहर में जागना । कराऊंगा। इस प्रकार की चेष्टा करते रहना 'यतमान
२. प्रथम और अन्तिम प्रहर में जागना और बीच के दो वैराग्य' है । यतमान वैराग्य स्वल्पाधिक मात्रा में सिद्ध हो
प्रहरों में सोना। जाने पर जब किसी-किसी विषय से राग हट जाता है और
रात्री के दो या तीन प्रहरों में जागृत रहकर ध्यान किसी-किसी में क्षीण होता रहता है तब व्यतिरेक के साथ
और स्वाध्याय करना, अप्रमत्त रहना 'यतना' है। अथवा पृथक् करके कहीं-कहीं वैराग्यावस्था दृढ़ करने का
४. शील-संप्रेक्षा-महावतों का अनुशीलन, इन्द्रिय का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। यह 'व्यतिरेक वैराग्य'
संयम, मन, वाणी और काया की स्थिरता, क्रोध, मान, कहलाता है। अभ्यास के द्वारा इसको अधीन करने पर
माया और लोभ का निग्रह-यह शील है। इसका सतत जब सभी इन्द्रियां बाह्य विषयों से भली-भांति निवृत्त हो
दर्शन 'शील-संप्रेक्षा' है। जाती हैं, पर उत्सुकता के रूप में मन में कुछ अनुराग
५. लोकसार का श्रवण-लोक में सारभूत तत्त्व-ज्ञान, अवशिष्ट रहता है, तब उस अवस्था को 'एकेन्द्रिय वैराग्य'
दर्शन और चारित्र का श्रवण । कहा जाता है, क्योंकि वह केवल मनोरूप एक ही इन्द्रिय में
६. कामना का परित्याग । रहता है।
७. कलह का परित्याग ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org