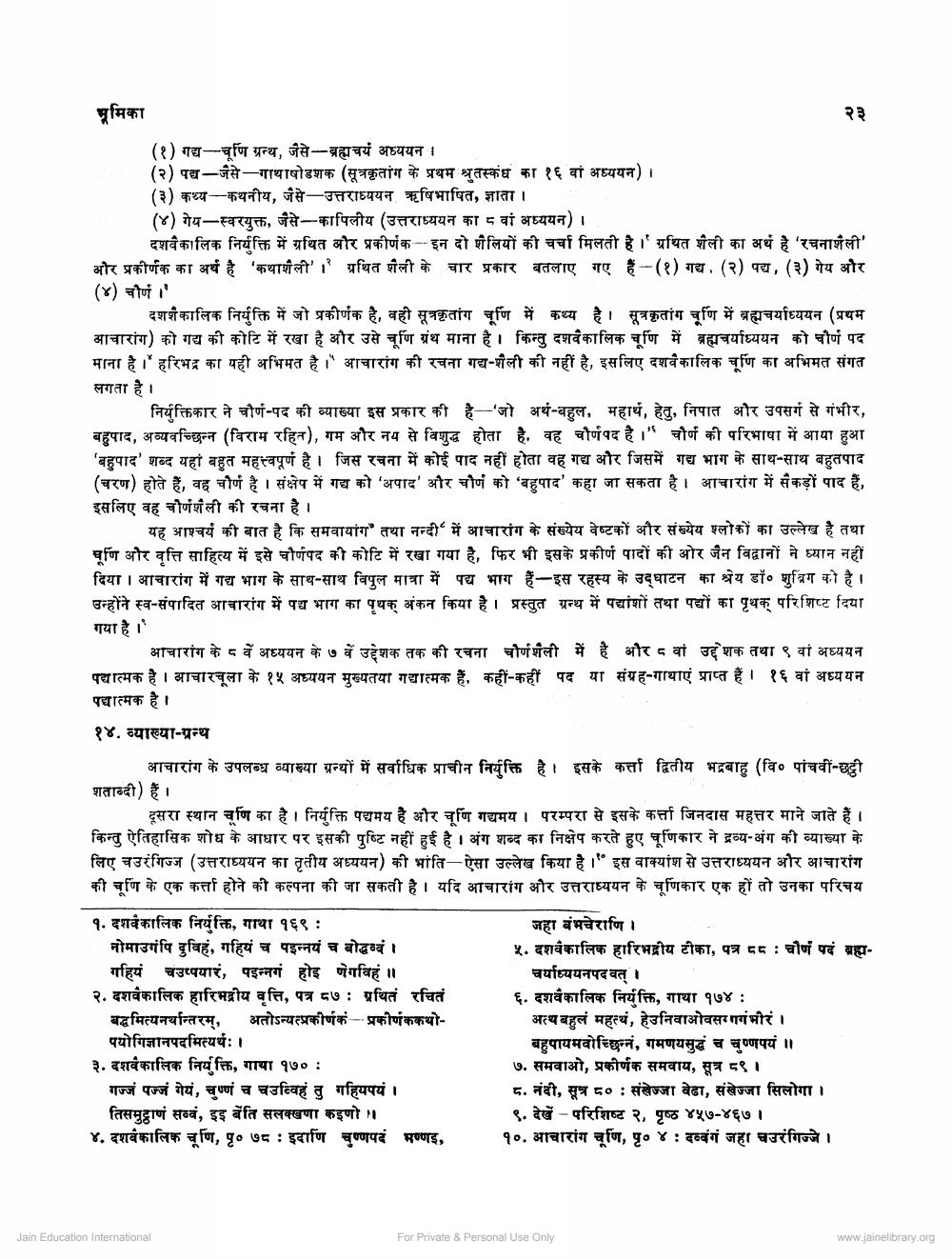________________
३
भूमिका
(१) गद्य-चूणि ग्रन्थ, जैसे-ब्रह्मचर्य अध्ययन । (२) पद्य-जैसे-गाथाषोडशक (सूत्रकृतांग के प्रथम श्रुतस्कंध का १६ वां अध्ययन)। (३) कथ्य-कथनीय, जैसे-उत्तराध्ययन ऋषिभाषित, ज्ञाता । (४) गेय-स्वरयुक्त, जैसे- कापिलीय (उत्तराध्ययन का ८ वां अध्ययन) ।
दशवकालिक नियुक्ति में ग्रथित और प्रकीर्णक --- इन दो शैलियों की चर्चा मिलती है। ग्रथित शैली का अर्थ है 'रचनाशैली' और प्रकीर्णक का अर्थ है 'कथाशैली'।' अथित शैली के चार प्रकार बतलाए गए हैं-(१) गद्य , (२) पद्य , (३) गेय और (४) चौर्ण ।
दशर्शकालिक नियुक्ति में जो प्रकीर्णक है, वही सूत्रकृतांग चूणि में कथ्य है। सूत्रकृतांग चूणि में ब्रह्मचर्याध्ययन (प्रथम आचारांग) को गद्य की कोटि में रखा है और उसे चूणि ग्रंथ माना है। किन्तु दशवकालिक चूणि में ब्रह्मचर्याध्ययन को चौर्ण पद माना है। हरिभद्र का यही अभिमत है।' आचारांग की रचना गद्य-शैली की नहीं है, इसलिए दशवकालिक चूणि का अभिमत संगत लगता है।
नियुक्तिकार ने चौर्ण-पद की व्याख्या इस प्रकार की है-'जो अर्थ-बहुल, महार्थ, हेतु, निपात और उपसर्ग से गंभीर, बहुपाद, अव्यवच्छिन्न (विराम रहित), गम और नय से विशुद्ध होता है, वह चौर्णपद है। चौर्ण की परिभाषा में आया हुआ 'बहुपाद' शब्द यहां बहुत महत्त्वपूर्ण है। जिस रचना में कोई पाद नहीं होता वह गद्य और जिसमें गद्य भाग के साथ-साथ बहुतपाद (चरण) होते हैं, वह चौर्ण है । संक्षेप में गद्य को 'अपाद' और चौर्ण को 'बहुपाद' कहा जा सकता है। आचारांग में सैकड़ों पाद हैं, इसलिए वह चौर्णशैली की रचना है।
यह आश्चर्य की बात है कि समवायांग तथा नन्दी में आचारांग के संख्येय वेष्टकों और संख्येय श्लोकों का उल्लेख है तथा घूणि और वृत्ति साहित्य में इसे चौर्णपद की कोटि में रखा गया है, फिर भी इसके प्रकीर्ण पादों की ओर जैन विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया । आचारांग में गद्य भाग के साथ-साथ विपुल मात्रा में पद्य भाग हैं-इस रहस्य के उद्घाटन का श्रेय डॉ० शुब्रिग को है। उन्होंने स्व-संपादित आचारांग में पद्य भाग का पृथक् अंकन किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में पद्यांशों तथा पद्यों का पृथक् परिशिष्ट दिया गया है।
आचारांग के ८ वें अध्ययन के ७ वें उद्देशक तक की रचना चौर्णशैली में है और ८ वां उद्देशक तथा ९ वां अध्ययन पद्यात्मक है । आचारचूला के १५ अध्ययन मुख्यतया गद्यात्मक हैं, कहीं-कहीं पद या संग्रह-गाथाएं प्राप्त हैं। १६ वां अध्ययन पद्यात्मक है। १४. व्याख्या-ग्रन्थ
आचारांग के उपलब्ध व्याख्या ग्रन्थों में सर्वाधिक प्राचीन नियुक्ति है। इसके कर्ता द्वितीय भद्रबाहु (वि० पांचवीं-छट्ठी शताब्दी) हैं।
दूसरा स्थान चुणि का है। नियुक्ति पद्यमय है और चूणि गद्यमय । परम्परा से इसके कर्ता जिनदास महत्तर माने जाते हैं। किन्तु ऐतिहासिक शोध के आधार पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है । अंग शब्द का निक्षेप करते हुए चूणिकार ने द्रव्य-अंग की व्याख्या के लिए चउरंगिज्ज (उत्तराध्ययन का तृतीय अध्ययन) की भांति-ऐसा उल्लेख किया है। इस वाक्यांश से उत्तराध्ययन और आचारांग की चूणि के एक कर्ता होने की कल्पना की जा सकती है। यदि आचारांग और उत्तराध्ययन के चूर्णिकार एक हों तो उनका परिचय १. दशवकालिक नियुक्ति, गाथा १६९ :
जहा बंभचेराणि । नोमाउगंपि दुविहं, गहियं च पइन्नयं च बोद्धव्वं ।
५. दशवकालिक हारिभद्रीय टीका, पत्र८८ : चौर्ण पदं ब्रह्मगहियं चउप्पयारं, पइन्नगं होइ गविहं ।
चर्याध्ययनपद वत् । २. दशवकालिक हारिभद्रीय वृत्ति, पत्र ८७ : प्रथितं रचितं ६. दशवैकालिक नियुक्ति, गाथा १७४ : बद्धमित्यनन्तरम्, अतोऽन्यत्प्रकीर्णक-प्रकीर्णककथो
अत्थ बहुलं महत्थं, हेउनिवाओवसरगगंभीरं । पयोगिज्ञानपदमित्यर्थः।
बहुपायमवोच्छिन्नं, गमणयसुद्धं च चुण्णपयं ॥ ३. दशवकालिक नियुक्ति, गाथा १७० :
७. समवाओ, प्रकीर्णक समवाय, सूत्र ८९ । गज्ज पज्जं गेयं, चुण्णं च चउन्विहं तु गहियपयं ।
८. नंदी, सूत्र ८० : संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा। तिसमुट्ठाणं सव्वं, इइ बेंति सलक्खणा कइणो।
९. देखें-परिशिष्ट २, पृष्ठ ४५७-४६७ । ४. दशवकालिक चूणि, पृ० ७८ : इदाणि चुण्णपदं मण्णइ, १०. आचारांग चूणि, पृ० ४ : दव्वंगं जहा चउरंगिज्जे ।
Jain Education international
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org