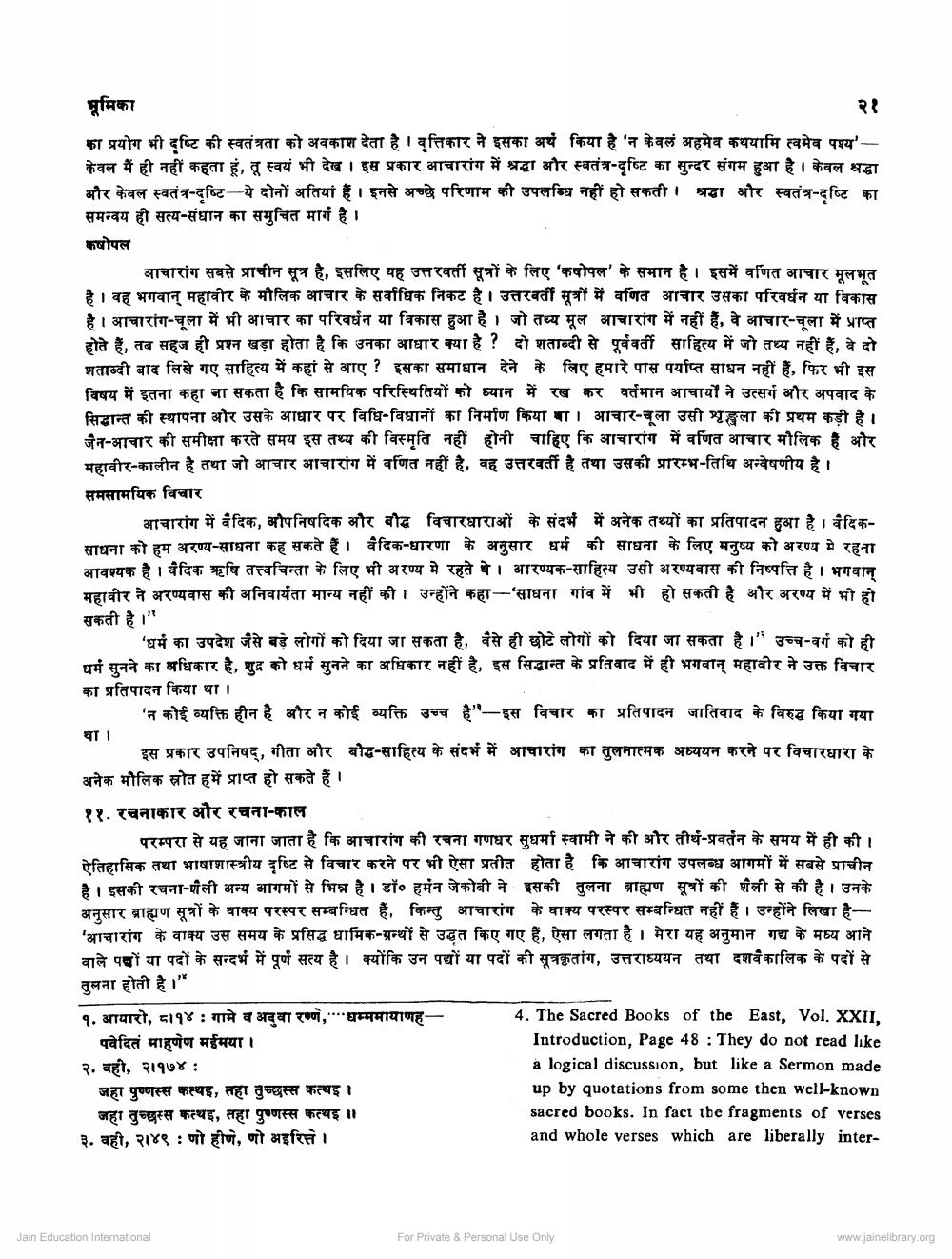________________
२१
भूमिका का प्रयोग भी दृष्टि की स्वतंत्रता को अवकाश देता है । वृत्तिकार ने इसका अर्थ किया है 'न केवलं अहमेव कथयामि त्वमेव पश्य'केवल मैं ही नहीं कहता हूं, तू स्वयं भी देख । इस प्रकार आचारांग में श्रद्धा और स्वतंत्र-दृष्टि का सुन्दर संगम हुआ है। केवल श्रद्धा
और केवल स्वतंत्र-दृष्टि-ये दोनों अतियां हैं। इनसे अच्छे परिणाम की उपलब्धि नहीं हो सकती। श्रद्धा और स्वतंत्र-दष्टि का समन्वय ही सत्य-संधान का समुचित मार्ग है। कषोपल
आचारांग सबसे प्राचीन सूत्र है, इसलिए यह उत्तरवर्ती सूत्रों के लिए 'कषोपल' के समान है। इसमें वर्णित आचार मूलभूत है। वह भगवान् महावीर के मौलिक आचार के सर्वाधिक निकट है। उत्तरवर्ती सूत्रों में वर्णित आचार उसका परिवर्धन या विकास है। आचारांग-चूला में भी आचार का परिवर्धन या विकास हुआ है । जो तथ्य मूल आचारांग में नहीं हैं, वे आचार-चूला में प्राप्त होते हैं, तब सहज ही प्रश्न खड़ा होता है कि उनका आधार क्या है ? दो शताब्दी से पूर्ववर्ती साहित्य में जो तथ्य नहीं हैं, वे दो शताब्दी बाद लिखे गए साहित्य में कहां से आए? इसका समाधान देने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, फिर भी इस विषय में इतना कहा जा सकता है कि सामयिक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर वर्तमान आचार्यों ने उत्सर्ग और अपवाद के सिद्धान्त की स्थापना और उसके आधार पर विधि-विधानों का निर्माण किया था। आचार-चूला उसी शृङ्खला की प्रथम कड़ी है। जैन-आचार की समीक्षा करते समय इस तथ्य की विस्मृति नहीं होनी चाहिए कि आचारांग में वर्णित आचार मौलिक है और महावीर-कालीन है तथा जो आचार आचारांग में वणित नहीं है, वह उत्तरवर्ती है तथा उसकी प्रारम्भ-तिथि अन्वेषणीय है। समसामयिक विचार
आचारांग में वैदिक, औपनिषदिक और बौद्ध विचारधाराओं के संदर्भ में अनेक तथ्यों का प्रतिपादन हुआ है । वैदिकसाधना को हम अरण्य-साधना कह सकते हैं। वैदिक-धारणा के अनुसार धर्म की साधना के लिए मनुष्य को अरण्य मे रहना आवश्यक है। वैदिक ऋषि तत्त्वचिन्ता के लिए भी अरण्य मे रहते थे। आरण्यक-साहित्य उसी अरण्यवास की निष्पत्ति है। भगवान महावीर ने अरण्यवास की अनिवार्यता मान्य नहीं की। उन्होंने कहा-'साधना गांव में भी हो सकती है और अरण्य में भी हो सकती है।"
'धर्म का उपदेश जैसे बड़े लोगों को दिया जा सकता है, वैसे ही छोटे लोगों को दिया जा सकता है।" उच्च-वर्ग को ही धर्म सुनने का अधिकार है, शुद्र को धर्म सुनने का अधिकार नहीं है, इस सिद्धान्त के प्रतिवाद में ही भगवान् महावीर ने उक्त विचार का प्रतिपादन किया था।
न कोई व्यक्ति हीन है और न कोई व्यक्ति उच्च है"-इस विचार का प्रतिपादन जातिवाद के विरुद्ध किया गया था।
इस प्रकार उपनिषद्, गीता और बौद्ध-साहित्य के संदर्भ में आचारांग का तुलनात्मक अध्ययन करने पर विचारधारा के अनेक मौलिक स्रोत हमें प्राप्त हो सकते हैं । ११. रचनाकार और रचना-काल
परम्परा से यह जाना जाता है कि आचारांग की रचना गणधर सुधर्मा स्वामी ने की और तीर्थ-प्रवर्तन के समय में ही की। ऐतिहासिक तथा भाषाशास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि आचारांग उपलब्ध आगमों में सबसे प्राचीन है। इसकी रचना-शैली अन्य आगमों से भिन्न है । डॉ. हर्मन जेकोबी ने इसकी तुलना ब्राह्मण सूत्रों की शैली से की है। उनके अनुसार ब्राह्मण सूत्रों के वाक्य परस्पर सम्बन्धित हैं, किन्तु आचारांग के वाक्य परस्पर सम्बन्धित नहीं हैं। उन्होंने लिखा है'आचारांग के वाक्य उस समय के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रन्थों से उद्धृत किए गए हैं, ऐसा लगता है। मेरा यह अनुमान गद्य के मध्य आने वाले पद्यों या पदों के सन्दर्भ में पूर्ण सत्य है। क्योंकि उन पद्यों या पदों की सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन तथा दशवकालिक के पदों से तुलना होती है।" १. आयारो, ८.१४ : गामे व अदुवा रण्णे,"धम्ममायाणह
4. The Sacred Books of the East, Vol. XXII, पवेदितं माहणेण मईमया।
Introduction, Page 48 : They do not read like २. वही, २।१७४:
a logical discussion, but like a Sermon made जहा पुण्णस्स कत्थइ, तहा तुच्छस्स कत्थई ।
up by quotations from some then well-known जहा तुच्छस्स कत्थइ, तहा पुण्णस्स कत्थइ।
sacred books. In fact the fragments of verses ३. वही, २०४९ : णो होणे, णो अइरित्ते ।
and whole verses which are liberally inter
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org