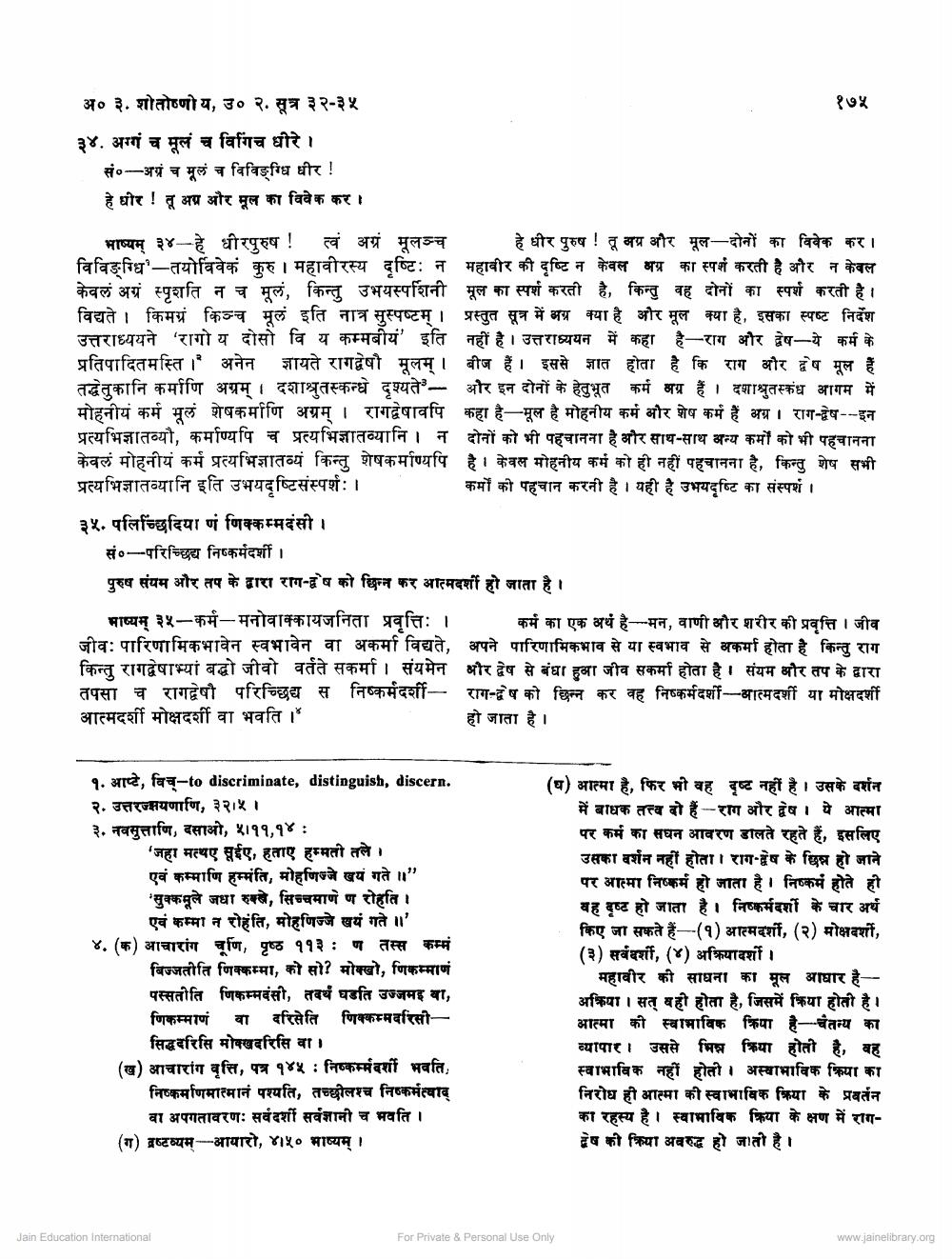________________
१७५
अ० ३. शोतोष्णो य, उ० २. सूत्र ३२-३५ ३४. अग्गं च मूलं च विगिच धीरे ।
सं०-अग्रं च मूलं च विविङ्ग्धि धीर ! हे धीर ! तू अन और मूल का विवेक कर।
भाष्यम् ३४-हे धीरपुरुष! त्वं अग्रं मूलञ्च हे धीर पुरुष ! तू अग्र और मूल-दोनों का विवेक कर । विविग्धि '-तयोविवेकं कुरु । महावीरस्य दृष्टि: न महावीर की दृष्टि न केवल अग्र का स्पर्श करती है और न केवल केवलं अग्रं स्पृशति न च मूलं, किन्तु उभयस्पर्शिनी मूल का स्पर्श करती है, किन्तु वह दोनों का स्पर्श करती है। विद्यते। किमग्रं किञ्च मूलं इति नात्र सुस्पष्टम् । प्रस्तुत सूत्र में अग्र क्या है और मूल क्या है, इसका स्पष्ट निर्देश उत्तराध्ययने 'रागो य दोसो वि य कम्मबीयं' इति नहीं है । उत्तराध्ययन में कहा है-राग और द्वेष-ये कर्म के प्रतिपादितमस्ति। अनेन ज्ञायते रागद्वेषौ मूलम् । बीज हैं। इससे ज्ञात होता है कि राग और द्वेष मूल हैं तद्धतकानि कर्माणि अग्रम् । दशाश्रुतस्कन्धे दृश्यते - और इन दोनों के हेतुभूत कर्म अग्र हैं । दशाश्रुतस्कंध आगम में मोहनीयं कर्म मूलं शेषकर्माणि अग्रम् । रागद्वेषावपि कहा है-मूल है मोहनीय कर्म और शेष कर्म हैं अन । राग-द्वेष--इन प्रत्यभिज्ञातव्यौ, कर्माण्यपि च प्रत्यभिज्ञातव्यानि । न दोनों को भी पहचानना है और साथ-साथ अन्य कर्मों को भी पहचानना केवलं मोहनीयं कर्म प्रत्यभिज्ञातव्यं किन्तु शेषकर्माण्यपि है। केवल मोहनीय कर्म को ही नहीं पहचानना है, किन्तु शेष सभी प्रत्यभिज्ञातव्यानि इति उभयदृष्टिसंस्पर्शः ।
कर्मों को पहचान करनी है । यही है उभयदृष्टि का संस्पर्श । ३५. पलिच्छिदिया णं णिक्कम्मदंसी।
सं०-परिच्छिद्य निष्कर्मदर्शी । पुरुष संयम और तप के द्वारा राग-द्वष को छिन्न कर आत्मदर्शी हो जाता है।
भाष्यम ३५-कर्म-मनोवाक्कायजनिता प्रवृत्तिः । कर्म का एक अर्थ है-मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति । जीव जीवः पारिणामिकभावेन स्वभावेन वा अकर्मा विद्यते, अपने पारिणामिकभाव से या स्वभाव से अकर्मा होता है किन्तु राग किन्तु रागद्वेषाभ्यां बद्धो जीवो वर्तते सकर्मा। संयमेन और द्वेष से बंधा हुवा जीव सकर्मा होता है। संयम और तप के द्वारा तपसा च रागद्वेषौ परिच्छिद्य स निष्कर्मदर्शी- राग-द्वेष को छिन्न कर वह निष्कर्मदर्शी-आत्मदर्शी या मोक्षदर्शी आत्मदर्शी मोक्षदर्शी वा भवति ।
हो जाता है।
१. आप्टे, विच्-to discriminate, distinguish, discern. २. उत्तरज्मयणाणि, ३२।५। ३. नवसुत्ताणि, दसाओ, ५।११,१४:
'जहा मत्थए सूईए, हताए हम्मती तले। एवं कम्माणि हम्मंति, मोहणिज्जे खयं गते ॥" 'सुक्कमूले जधा रक्खे, सिच्चमाणे ण रोहति ।
एवं कम्मा न रोहंति, मोहणिज्जे खयं गते ॥' ४. (क) आचारांग चूणि, पृष्ठ ११३ : ण तस्स कम्म
बिज्जतीति णिक्कम्मा, को सो? मोक्खो, णिकम्माणं पस्सतीति णिकम्मवंसी, तदर्थ घडति उज्जमइ वा, णिकम्माणं वा दरिसेति णिक्कम्मदरिसी
सिद्धदरिसि मोक्खदरिसि वा। (ख) आचारांग वृत्ति, पत्र १४५ : निष्कर्मवी भवति,
निष्कर्माणमात्मानं पश्यति, तच्छोलश्च निष्कर्मत्वाद्
वा अपगतावरणः सर्वदर्शी सर्वज्ञानी च भवति । (ग) द्रष्टव्यम-आयारो, ४५० भाष्यम् ।
(घ) आत्मा है, फिर भी वह दृष्ट नहीं है । उसके दर्शन
में बाधक तत्त्व दो हैं-राग और द्वेष । ये आत्मा पर कर्म का सघन आवरण डालते रहते हैं, इसलिए उसका वर्शन नहीं होता। राग-द्वेष के छिन्न हो जाने पर आत्मा निष्कर्म हो जाता है। निष्कर्म होते ही वह दृष्ट हो जाता है। निष्कर्मदर्शी के चार अर्थ किए जा सकते हैं-(१) आत्मदर्शी, (२) मोक्षदर्शी, (३) सर्वदर्शी, (४) अक्रियादी ।
महावीर की साधना का मूल आधार हैअक्रिया । सत् वही होता है, जिसमें क्रिया होती है। आत्मा की स्वाभाविक क्रिया है-चैतन्य का व्यापार। उससे भिन्न क्रिया होती है, वह स्वाभाविक नहीं होती। अस्वाभाविक क्रिया का निरोध ही आत्मा की स्वाभाविक क्रिया के प्रवर्तन का रहस्य है। स्वाभाविक क्रिया के क्षण में रागद्वेष की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org