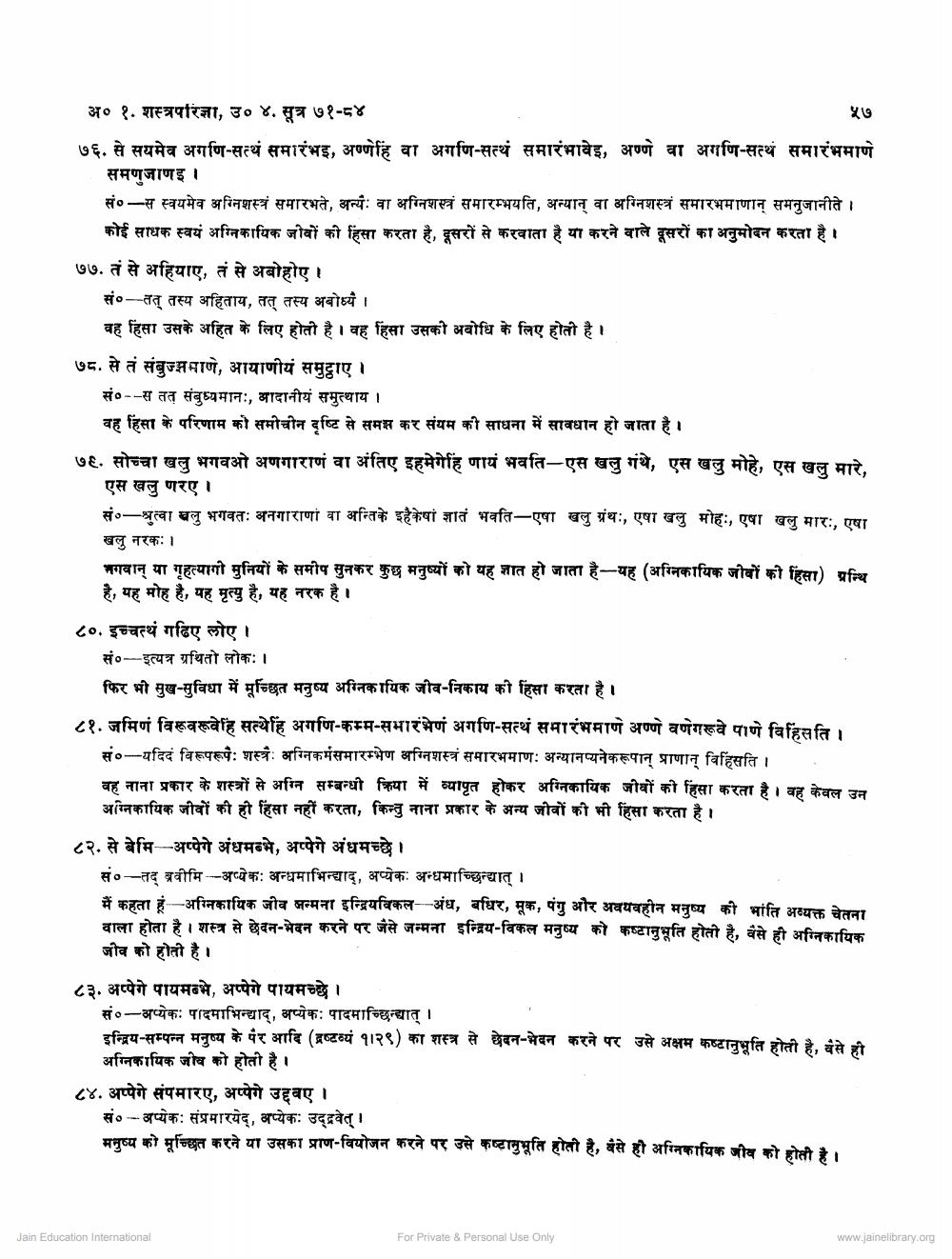________________
अ० १. शस्त्रपरिज्ञा, उ० ४. सूत्र ७१-८४ ७६. से सयमेव अगणि-सत्थं समारंभइ, अण्णेहिं वा अगणि-सत्थं समारंभावेइ, अण्णे वा अगणि-सत्थं समारंभमाणे
समणुजाणइ। सं०-स स्वयमेव अग्निशस्त्रं समारभते, अन्यः वा अग्निशस्त्र समारम्भयति, अन्यान् वा अग्निशस्त्रं समारभमाणान् समनुजानीते ।
कोई साधक स्वयं अग्निकायिक जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से करवाता है या करने वाले दूसरों का अनुमोदन करता है। ७७. तं से अहियाए, तं से अबोहोए।
सं०--तत् तस्य अहिताय, तत् तस्य अबोध्य ।
वह हिंसा उसके अहित के लिए होती है। वह हिसा उसको अबोधि के लिए होती है। ७८. से तं संबुज्झमाणे, आयाणीयं समुट्टाए ।
सं०--स तत संबुध्यमानः, आदानीयं समुत्थाय । वह हिंसा के परिणाम को समीचीन दृष्टि से समझ कर संयम को साधना में सावधान हो जाता है।
७६. सोच्चा खलु भगवओ अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेहिं णायं भवति-एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे,
एस खलु णरए। सं०-श्रुत्वा चलू भगवतः अनगाराणा वा अन्तिके इहैकेषां ज्ञातं भवति-एषा खलु ग्रंथः, एषा खलु मोहः, एषा खलु मारः, एषा खलु नरकः । भगवान् या गृहत्यागी मुनियों के समीप सुनकर कुछ मनुष्यों को यह ज्ञात हो जाता है-यह (अग्निकायिक जीवों की हिसा) प्रथि है, यह मोह है, यह मृत्यु है, यह नरक है।
८०. इच्चत्थं गढिए लोए।
सं०-इत्यत्र ग्रथितो लोकः । फिर भी सुख-सुविधा में मूच्छित मनुष्य अग्निकायिक जीव-निकाय की हिंसा करता है।
८१. जमिणं विरूवरूवेहि सत्थेहि अगणि-कम्म-समारंभेणं अगणि-सत्थं समारंभमाणे अण्णे वणेगरूवे पाणे विसति।
सं०-यदिदं विरूपरूपैः शस्त्रः अग्निकर्मसमारम्भेण अग्निशस्त्रं समारभमाणः अन्यानप्यनेकरूपान् प्राणान् विहिंसति । वह नाना प्रकार के शस्त्रों से अग्नि सम्बन्धी क्रिया में व्याप्त होकर अग्निकायिक जीवों की हिंसा करता है। वह केवल उन
अग्निकायिक जीवों की ही हिंसा नहीं करता, किन्तु नाना प्रकार के अन्य जीवों की भी हिंसा करता है। ८२. से बेमि--अप्पेगे अंधमब्भे, अप्पेगे अंधमच्छे।
सं०-तद् ब्रवीमि --अप्येक: अन्धमाभिन्द्याद्, अप्येकः अन्धमाच्छिन्द्यात् । मैं कहता हूं-अग्निकायिक जीव जन्मना इन्द्रियविकल-अंध, बधिर, मूक, पंगु और अवयवहीन मनुष्य की भांति अव्यक्त चेतना वाला होता है। शस्त्र से छेदन-भेवन करने पर जैसे जन्मना इन्द्रिय-विकल मनुष्य को कष्टानुभूति होती है, वैसे ही अग्निकायिक
जीव को होती है। ८३. अप्पेगे पायमन्भे, अप्पेगे पायमच्छे ।
सं०-अप्येकः पादमाभिन्द्याद्, अप्येकः पादमाच्छिन्द्यात् । इन्द्रिय-सम्पन्न मनुष्य के पैर आदि (द्रष्टव्यं १।२९) का शस्त्र से छेदन-भेदन करने पर उसे अक्षम कष्टानुभूति होती है, वैसे ही
अग्निकायिक जीव को होती है। ८४. अप्पेगे संपमारए, अप्पेगे उद्दवए ।
सं०-अप्येकः संप्रमारयेद्, अप्येकः उद्भवेत् । मनष्य को मच्छित करने या उसका प्राण-वियोजन करने पर उसे कष्टानुभूति होती है, वैसे ही अग्निकायिक जीव को होती है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org