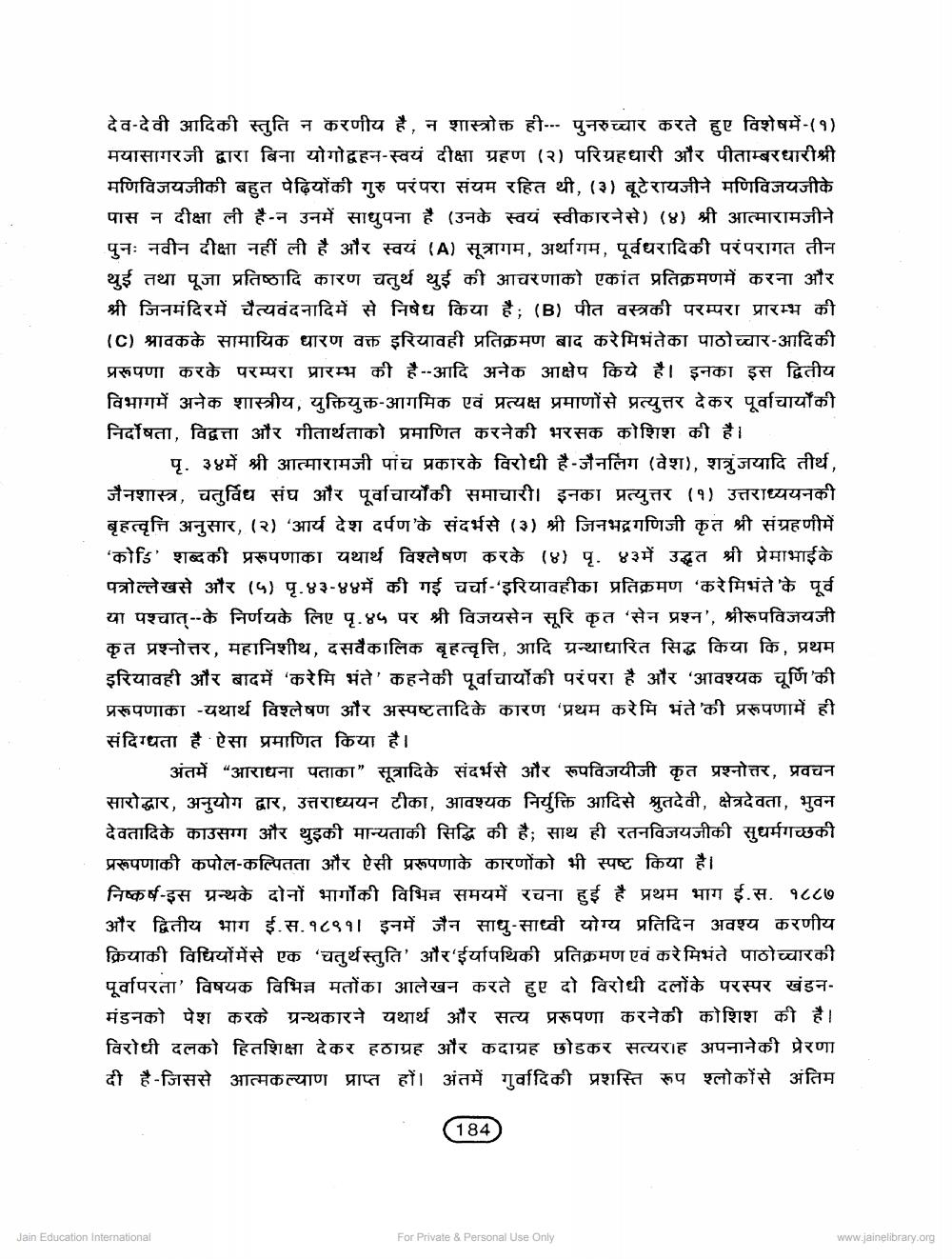________________
देव-देवी आदिकी स्तुति न करणीय है, न शास्त्रोक्त ही--- पुनरुच्चार करते हुए विशेषमें-(१) मयासागरजी द्वारा बिना योगोद्वहन-स्वयं दीक्षा ग्रहण (२) परिग्रहधारी और पीताम्बरधारीश्री मणिविजयजीकी बहुत पेढ़ियोंकी गुरु परंपरा संयम रहित थी, (३) बूटेरायजीने मणिविजयजीके पास न दीक्षा ली है-न उनमें साधुपना है (उनके स्वयं स्वीकारनेसे) (४) श्री आत्मारामजीने पुनः नवीन दीक्षा नहीं ली है और स्वयं (A) सूत्रागम, अर्थागम, पूर्वधरादिकी परंपरागत तीन थुई तथा पूजा प्रतिष्ठादि कारण चतुर्थ थुई की आचरणाको एकांत प्रतिक्रमणमें करना और श्री जिनमंदिरमें चैत्यवंदनादिमें से निषेध किया है; (B) पीत वस्त्रकी परम्परा प्रारम्भ की (C) श्रावकके सामायिक धारण वक्त इरियावही प्रतिक्रमण बाद करे मिभंतेका पाठोच्चार-आदिकी प्ररूपणा करके परम्परा प्रारम्भ की है --आदि अनेक आक्षेप किये है। इनका इस द्वितीय विभागमें अनेक शास्त्रीय, युक्तियुक्त-आगमिक एवं प्रत्यक्ष प्रमाणों से प्रत्युत्तर देकर पूर्वाचार्यों की निर्दोषता, विद्वत्ता और गीतार्थताको प्रमाणित करने की भरसक कोशिश की है।
पृ. ३४में श्री आत्मारामजी पांच प्रकार के विरोधी है-जैनलिंग (वेश), शत्रुजयादि तीर्थ, जैनशास्त्र, चतुर्विध संघ और पूर्वाचार्यों की समाचारी। इनका प्रत्युत्तर (१) उत्तरा बृहत्वृत्ति अनुसार, (२) 'आर्य देश दर्पण'के संदर्भसे (३) श्री जिनभद्रगणिजी कृत श्री संग्रहणीमें 'कोडि' शब्दकी प्ररूपणाका यथार्थ विश्लेषण करके (४) पृ. ४३में उद्धृत श्री प्रेमाभाईके पत्रोल्लेखसे और (५) पृ.४३-४४में की गई चर्चा- 'इरियावहीका प्रतिक्रमण 'करे मिभंते 'के पूर्व या पश्चात्-के निर्णयके लिए पृ.४५ पर श्री विजयसेन सूरि कृत 'सेन प्रश्न', श्रीरूपविजयजी कत प्रश्नोत्तर. महानिशीथ, दसवैकालिक बहत्त्वत्ति, आदि ग्रन्थाधारित सिद्ध किया कि, प्रथम इरियावही और बादमें 'करेमि भंते' कहने की पूर्वाचार्यों की परंपरा है और 'आवश्यक चूर्णि'की प्ररूपणाका -यथार्थ विश्लेषण और अस्पष्टतादिके कारण 'प्रथम करे मि भंते 'की प्ररूपणामें ही संदिग्धता है ऐसा प्रमाणित किया है।
अंतमें “आराधना पताका" सूत्रादिके संदर्भसे और रूपविजयीजी कृत प्रश्नोत्तर, प्रवचन सारोद्धार, अनुयोग द्वार, उत्तराध्ययन टीका, आवश्यक नियुक्ति आदिसे श्रुतदेवी, क्षेत्रदेवता, भुवन देवतादिके काउसग्ग और थुइकी मान्यताकी सिद्धि की है। साथ ही रतनविजयजीकी सुधर्मगच्छकी प्ररूपणाकी कपोल-कल्पितता और ऐसी प्ररूपणाके कारणोंको भी स्पष्ट किया है। निष्कर्ष-इस ग्रन्थके दोनों भार्गोकी विभिन्न समयमें रचना हुई है प्रथम भाग ई.स. १८८७
और द्वितीय भाग ई.स.१८९१। इनमें जैन साधु-साध्वी योग्य प्रतिदिन अवश्य करणीय क्रियाकी विधियों में से एक 'चतुर्थस्तुति' और ईर्यापथिकी प्रतिक्रमण एवं करे मिभंते पाठोच्चारकी पूर्वापरता' विषयक विभिन्न मतोंका आलेखन करते हुए दो विरोधी दलों के परस्पर खंडनमंडनको पेश करके ग्रन्थकारने यथार्थ और सत्य प्ररूपणा करने की कोशिश की है। विरोधी दलको हितशिक्षा देकर हठाग्रह और कदाग्रह छोडकर सत्यराह अपनाने की प्रेरणा दी है-जिससे आत्मकल्याण प्राप्त हों। अंतमें गुर्वादिकी प्रशस्ति रूप श्लोकोंसे अंतिम
(184
Jain Education international
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org