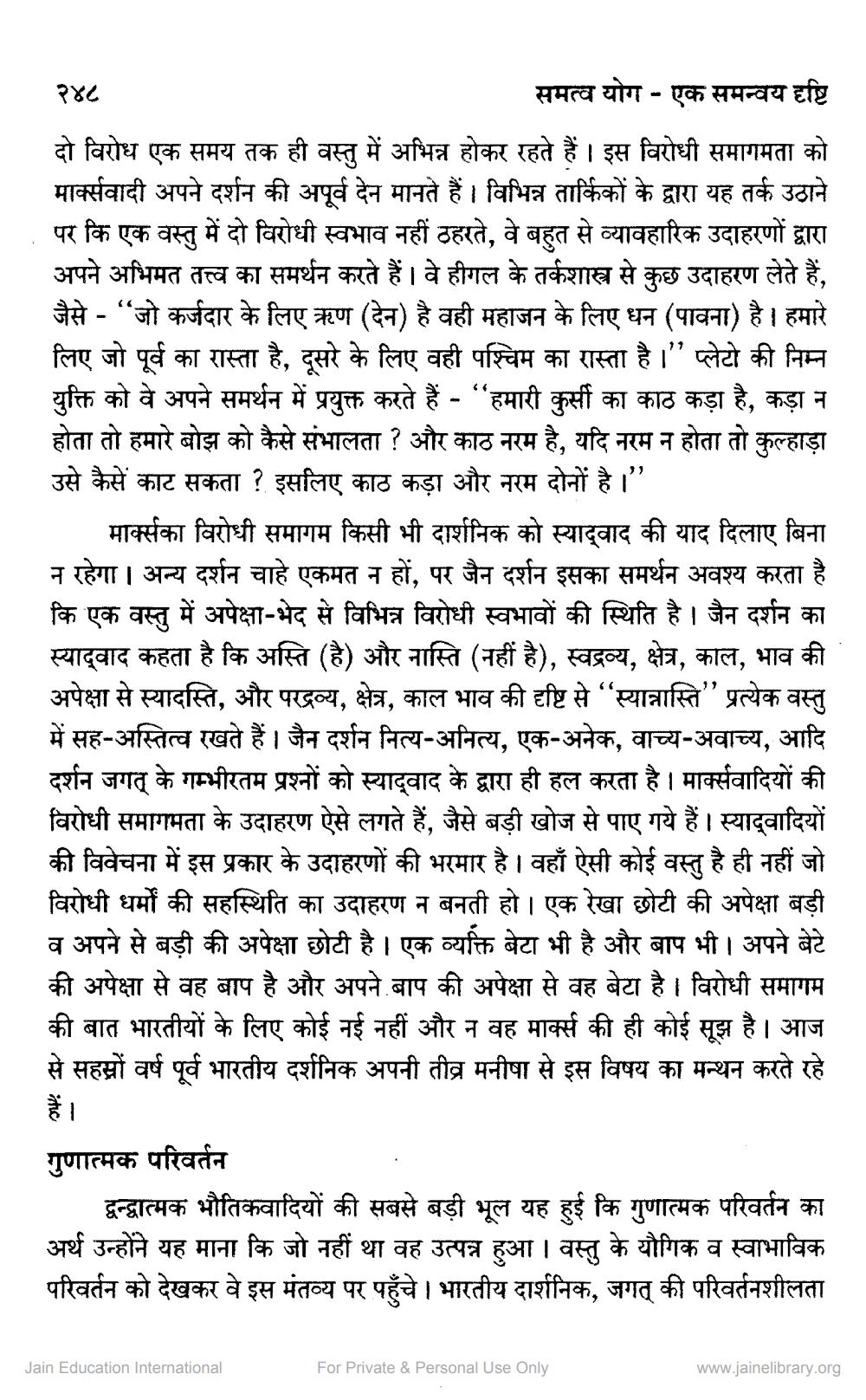________________
२४८
समत्व योग - एक समन्वय दृष्टि दो विरोध एक समय तक ही वस्तु में अभिन्न होकर रहते हैं । इस विरोधी समागमता को मार्क्सवादी अपने दर्शन की अपूर्व देन मानते हैं। विभिन्न तार्किकों के द्वारा यह तर्क उठाने पर कि एक वस्तु में दो विरोधी स्वभाव नहीं ठहरते, वे बहुत से व्यावहारिक उदाहरणों द्वारा अपने अभिमत तत्त्व का समर्थन करते हैं। वे हीगल के तर्कशास्त्र से कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे - “जो कर्जदार के लिए ऋण (देन) है वही महाजन के लिए धन (पावना) है। हमारे लिए जो पूर्व का रास्ता है, दूसरे के लिए वही पश्चिम का रास्ता है ।" प्लेटो की निम्न युक्ति को वे अपने समर्थन में प्रयुक्त करते हैं- “हमारी कुर्सी का काठ कड़ा है, कड़ा न होता तो हमारे बोझ को कैसे संभालता ? और काठ नरम है, यदि नरम न होता तो कुल्हाड़ा उसे कैसे काट सकता ? इसलिए काठ कड़ा और नरम दोनों है । "
मार्क्सका विरोधी समागम किसी भी दार्शनिक को स्याद्वाद की याद दिलाए बिना न रहेगा । अन्य दर्शन चाहे एकमत न हों, पर जैन दर्शन इसका समर्थन अवश्य करता है कि एक वस्तु में अपेक्षा भेद से विभिन्न विरोधी स्वभावों की स्थिति है। जैन दर्शन का स्याद्वाद कहता है कि अस्ति (है) और नास्ति (नहीं है), स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से स्यादस्ति, और परद्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की दृष्टि से " स्यान्नास्ति” प्रत्येक वस्तु में सह-अस्तित्व रखते हैं । जैन दर्शन नित्य- अनित्य, एक-अनेक, वाच्य - अवाच्य, आदि दर्शन जगत् के गम्भीरतम प्रश्नों को स्याद्वाद के द्वारा ही हल करता है। मार्क्सवादियों की विरोधी समागमता के उदाहरण ऐसे लगते हैं, जैसे बड़ी खोज से पाए गये हैं । स्याद्वादियों की विवेचना में इस प्रकार के उदाहरणों की भरमार है । वहाँ ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो विरोधी धर्मों की सहस्थिति का उदाहरण न बनती हो । एक रेखा छोटी की अपेक्षा बड़ी व अपने से बड़ी की अपेक्षा छोटी है । एक व्यक्ति बेटा भी है और बाप भी। अपने बेटे की अपेक्षा से वह बाप है और अपने बाप की अपेक्षा से वह बेटा है । विरोधी समागम की बात भारतीयों के लिए कोई नई नहीं और न वह मार्क्स की ही कोई सूझ है । आज से सहस्रों वर्ष पूर्व भारतीय दर्शनिक अपनी तीव्र मनीषा से इस विषय का मन्थन करते रहे हैं ।
गुणात्मक परिवर्तन
द्वन्द्वात्मक भौतिकवादियों की सबसे बड़ी भूल यह हुई कि गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ उन्होंने यह माना कि जो नहीं था वह उत्पन्न हुआ । वस्तु के यौगिक व स्वाभाविक परिवर्तन को देखकर वे इस मंतव्य पर पहुँचे । भारतीय दार्शनिक, जगत् की परिवर्तनशीलता
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org