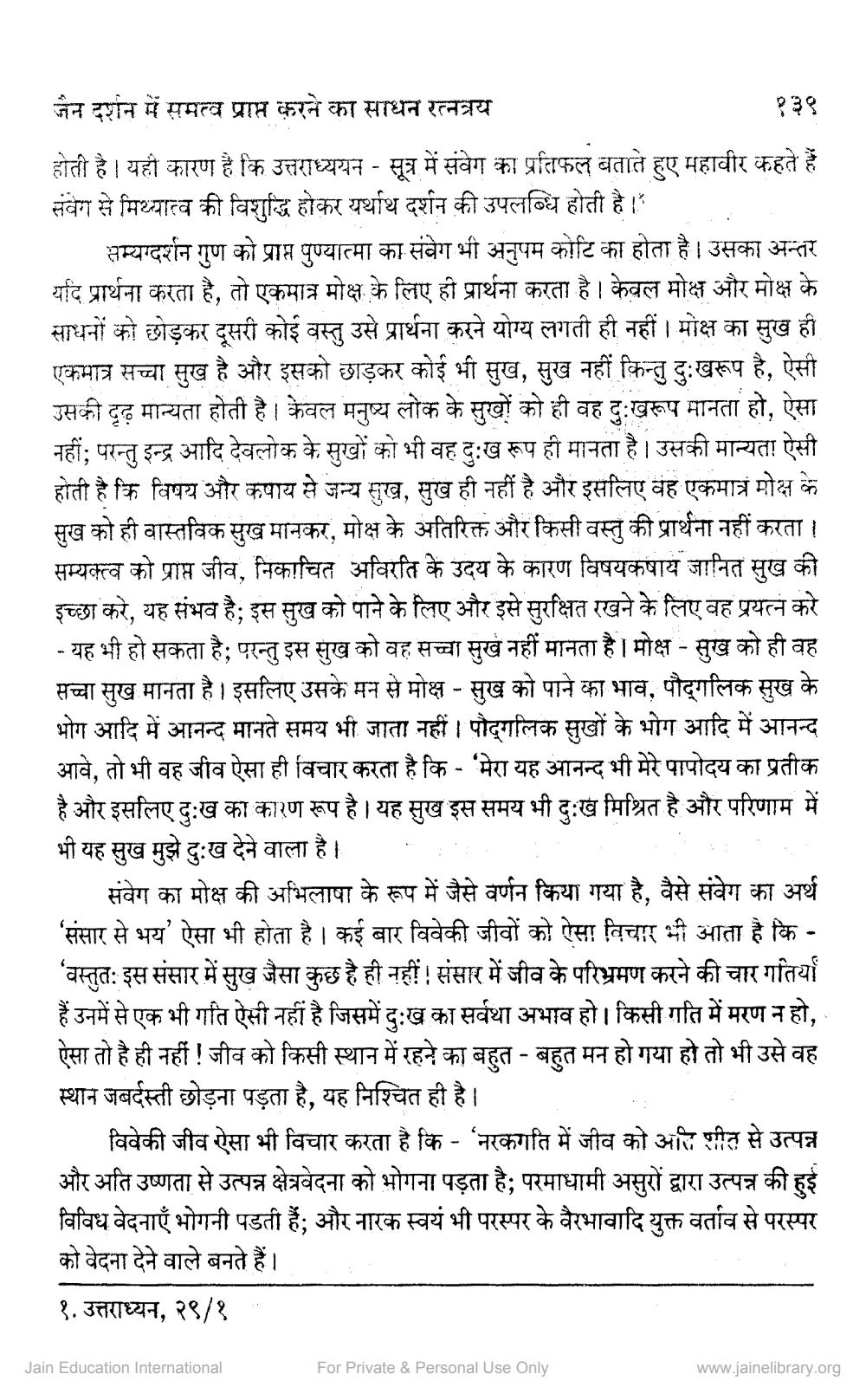________________
जैन दर्शन में समत्व प्राप्त करने का साधन रत्नत्रय
१३९
होती है। यही कारण है कि उत्तराध्ययन - सूत्र में संवेग का प्रतिफल बताते हुए महावीर कहते हैं संवेग से मिथ्यात्व की विशुद्धि होकर यर्थाथ दर्शन की उपलब्धि होती है।
सम्यग्दर्शन गुण को प्राप्त पुण्यात्मा का संवेग भी अनुपम कोटि का होता है। उसका अन्तर यदि प्रार्थना करता है, तो एकमात्र मोक्ष के लिए ही प्रार्थना करता है। केवल मोक्ष और मोक्ष के साधनों को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु उसे प्रार्थना करने योग्य लगती ही नहीं। मोक्ष का सुख ही एकमात्र सच्चा सुख है और इसको छाड़कर कोई भी सुख, सुख नहीं किन्तु दुःखरूप है, ऐसी उसकी दृढ़ मान्यता होती है। केवल मनुष्य लोक के सुखों को ही वह दुःखरूप मानता हो, ऐसा नहीं; परन्तु इन्द्र आदि देवलोक के सुखों को भी वह दुःख रूप ही मानता है। उसकी मान्यता ऐसी होती है कि विषय और कषाय से जन्य सख, सुख ही नहीं है और इसलिए वह एकमात्र मोक्ष के सुख को ही वास्तविक सुख मानकर, मोक्ष के अतिरिक्त और किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करता। सम्यक्त्व को प्राप्त जीव, निकाचित अविरति के उदय के कारण विषयकषाय जानित सुख की इच्छा करे, यह संभव है; इस सुख को पाने के लिए और इसे सुरक्षित रखने के लिए वह प्रयत्न करे - यह भी हो सकता है; परन्तु इस सुख को वह सच्चा सुख नहीं मानता है। मोक्ष - सुख को ही वह सच्चा सुख मानता है। इसलिए उसके मन से मोक्ष - सुख को पाने का भाव, पौद्गलिक सुख के भोग आदि में आनन्द मानते समय भी जाता नहीं। पौद्गलिक सुखों के भोग आदि में आनन्द आवे, तो भी वह जीव ऐसा ही विचार करता है कि - 'मेरा यह आनन्द भी मेरे पापोदय का प्रतीक है और इसलिए दु:ख का कारण रूप है। यह सुख इस समय भी दुःख मिश्रित है और परिणाम में भी यह सुख मुझे दुःख देने वाला है। __संवेग का मोक्ष की अभिलाषा के रूप में जैसे वर्णन किया गया है, वैसे संवेग का अर्थ 'संसार से भय' ऐसा भी होता है। कई बार विवेकी जीवों को ऐसा विचार भी आता है कि - 'वस्तुत: इस संसार में सुख जैसा कुछ है ही नहीं ! संसार में जीव के परिभ्रमण करने की चार गतियाँ हैं उनमें से एक भी गति ऐसी नहीं है जिसमें दुःख का सर्वथा अभाव हो। किसी गति में मरण न हो, ऐसा तो है ही नहीं ! जीव को किसी स्थान में रहने का बहुत - बहुत मन हो गया हो तो भी उसे वह स्थान जबर्दस्ती छोड़ना पड़ता है, यह निश्चित ही है।
विवेकी जीव ऐसा भी विचार करता है कि - ‘नरकगति में जीव को अति शीत से उत्पन्न और अति उष्णता से उत्पन्न क्षेत्रवेदना को भोगना पड़ता है; परमाधामी असुरों द्वारा उत्पन्न की हुई विविध वेदनाएँ भोगनी पडती हैं; और नारक स्वयं भी परस्पर के वैरभावादि युक्त वर्ताव से परस्पर को वेदना देने वाले बनते हैं। १. उत्तराध्यन, २९/१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org