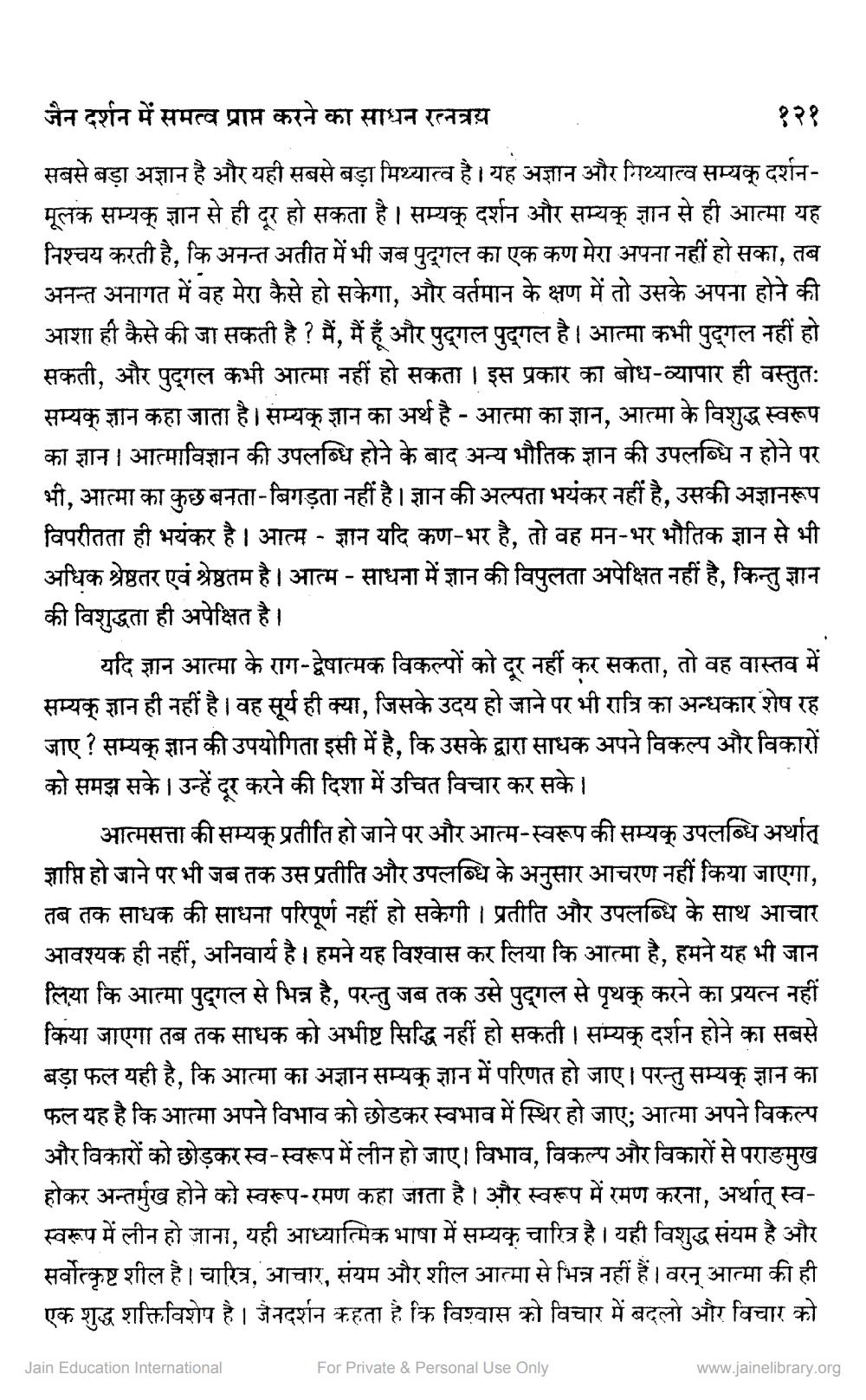________________
जैन दर्शन में समत्व प्राप्त करने का साधन रत्नत्रय
१२१ सबसे बड़ा अज्ञान है और यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। यह अज्ञान और गिथ्यात्व सम्यक् दर्शनमूलक सम्यक् ज्ञान से ही दूर हो सकता है। सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान से ही आत्मा यह निश्चय करती है, कि अनन्त अतीत में भी जब पुद्गल का एक कण मेरा अपना नहीं हो सका, तब अनन्त अनागत में वह मेरा कैसे हो सकेगा, और वर्तमान के क्षण में तो उसके अपना होने की आशा ही कैसे की जा सकती है ? मैं, मैं हूँ और पुद्गल पुद्गल है। आत्मा कभी पुद्गल नहीं हो सकती, और पुद्गल कभी आत्मा नहीं हो सकता । इस प्रकार का बोध-व्यापार ही वस्तुतः सम्यक् ज्ञान कहा जाता है। सम्यक् ज्ञान का अर्थ है - आत्मा का ज्ञान, आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान । आत्माविज्ञान की उपलब्धि होने के बाद अन्य भौतिक ज्ञान की उपलब्धि न होने पर भी, आत्मा का कुछ बनता-बिगड़ता नहीं है। ज्ञान की अल्पता भयंकर नहीं है, उसकी अज्ञानरूप विपरीतता ही भयंकर है। आत्म - ज्ञान यदि कण-भर है, तो वह मन-भर भौतिक ज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठतर एवं श्रेष्ठतम है। आत्म - साधना में ज्ञान की विपुलता अपेक्षित नहीं है, किन्तु ज्ञान की विशुद्धता ही अपेक्षित है।
यदि ज्ञान आत्मा के राग-द्वेषात्मक विकल्पों को दूर नहीं कर सकता, तो वह वास्तव में सम्यक् ज्ञान ही नहीं है। वह सूर्य ही क्या, जिसके उदय हो जाने पर भी रात्रि का अन्धकार शेष रह जाए ? सम्यक् ज्ञान की उपयोगिता इसी में है, कि उसके द्वारा साधक अपने विकल्प और विकारों को समझ सके। उन्हें दूर करने की दिशा में उचित विचार कर सके।
आत्मसत्ता की सम्यक् प्रतीति हो जाने पर और आत्म-स्वरूप की सम्यक् उपलब्धि अर्थात् ज्ञाप्ति हो जाने पर भी जब तक उस प्रतीति और उपलब्धि के अनुसार आचरण नहीं किया जाएगा, तब तक साधक की साधना परिपूर्ण नहीं हो सकेगी। प्रतीति और उपलब्धि के साथ आचार
आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हमने यह विश्वास कर लिया कि आत्मा है, हमने यह भी जान लिया कि आत्मा पुद्गल से भिन्न है, परन्तु जब तक उसे पुद्गल से पृथक् करने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तब तक साधक को अभीष्ट सिद्धि नहीं हो सकती। सम्यक् दर्शन होने का सबसे बड़ा फल यही है, कि आत्मा का अज्ञान सम्यक् ज्ञान में परिणत हो जाए। परन्तु सम्यक् ज्ञान का फल यह है कि आत्मा अपने विभाव को छोडकर स्वभाव में स्थिर हो जाए; आत्मा अपने विकल्प
और विकारों को छोड़कर स्व-स्वरूप में लीन हो जाए। विभाव, विकल्प और विकारों से पराङमख होकर अन्तर्मुख होने को स्वरूप-रमण कहा जाता है। और स्वरूप में रमण करना, अर्थात् स्वस्वरूप में लीन हो जाना, यही आध्यात्मिक भाषा में सम्यक् चारित्र है। यही विशुद्ध संयम है और सर्वोत्कृष्ट शील है। चारित्र, आचार, संयम और शील आत्मा से भिन्न नहीं हैं। वरन् आत्मा की ही एक शुद्ध शक्तिविशेष है। जैनदर्शन कहता है कि विश्वास को विचार में बदलो और विचार को
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org