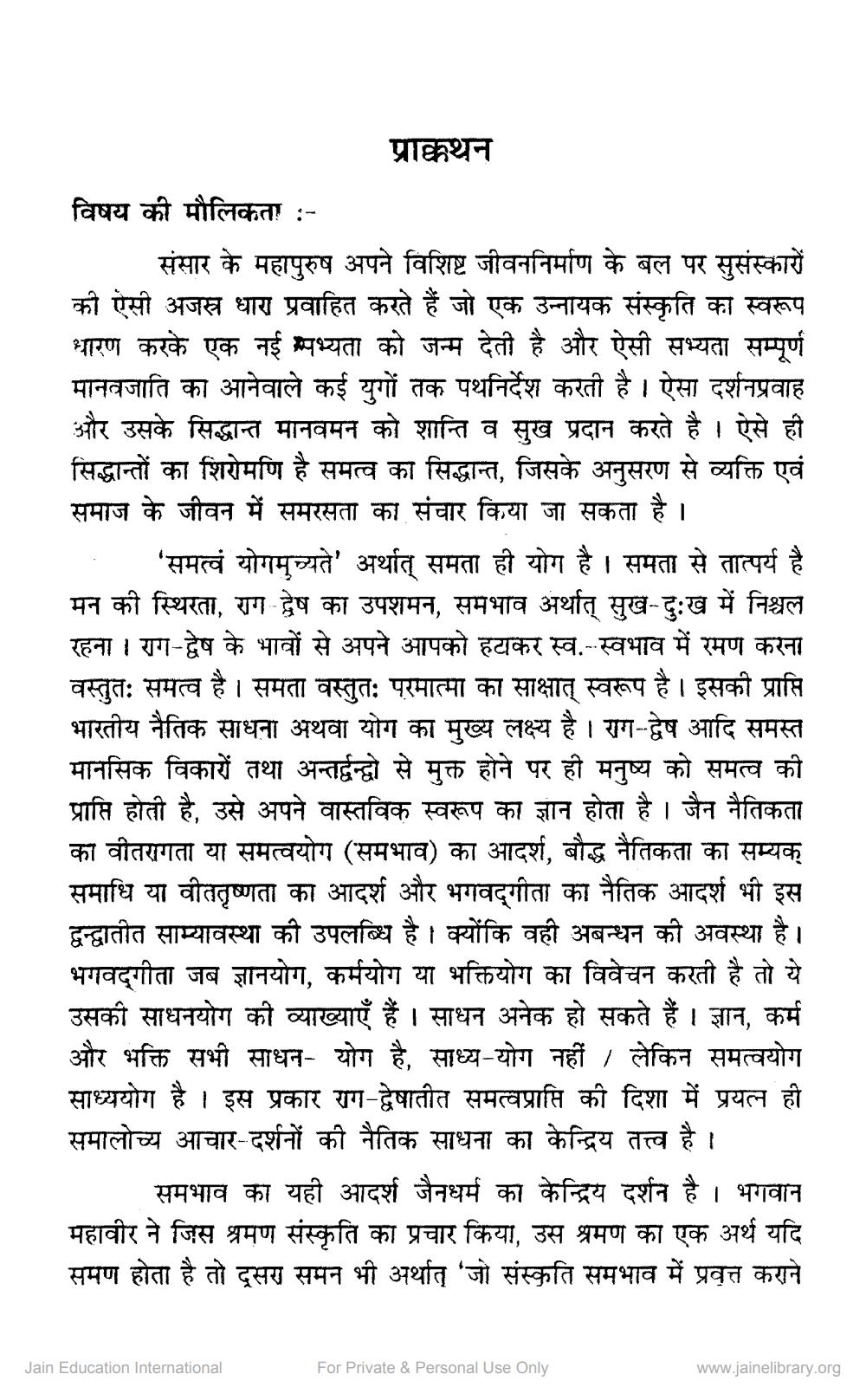________________
प्राक्कथन
विषय की मौलिकता :
संसार के महापुरुष अपने विशिष्ट जीवननिर्माण के बल पर सुसंस्कारों की ऐसी अजस्र धारा प्रवाहित करते हैं जो एक उन्नायक संस्कृति का स्वरूप धारण करके एक नई सभ्यता को जन्म देती है और ऐसी सभ्यता सम्पूर्ण मानवजाति का आनेवाले कई युगों तक पथनिर्देश करती है । ऐसा दर्शनप्रवाह
और उसके सिद्धान्त मानवमन को शान्ति व सुख प्रदान करते है । ऐसे ही सिद्धान्तों का शिरोमणि है समत्व का सिद्धान्त, जिसके अनुसरण से व्यक्ति एवं समाज के जीवन में समरसता का संचार किया जा सकता है।
'समत्वं योगमुच्यते' अर्थात् समता ही योग है । समता से तात्पर्य है मन की स्थिरता, राग द्वेष का उपशमन, समभाव अर्थात् सुख-दुःख में निश्चल रहना । राग-द्वेष के भावों से अपने आपको हटाकर स्व.- स्वभाव में रमण करना वस्तुतः समत्व है। समता वस्तुत: परमात्मा का साक्षात् स्वरूप है । इसकी प्राप्ति भारतीय नैतिक साधना अथवा योग का मुख्य लक्ष्य है। राग-द्वेष आदि समस्त मानसिक विकारों तथा अन्तर्द्वन्द्वो से मुक्त होने पर ही मनुष्य को समत्व की प्राप्ति होती है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है । जैन नैतिकता का वीतरागता या समत्वयोग (समभाव) का आदर्श, बौद्ध नैतिकता का सम्यक समाधि या वीततष्णता का आदर्श और भगवदगीता का नैतिक आदर्श भी इस द्वन्द्वातीत साम्यावस्था की उपलब्धि है। क्योंकि वही अबन्धन की अवस्था है। भगवद्गीता जब ज्ञानयोग, कर्मयोग या भक्तियोग का विवेचन करती है तो ये उसकी साधनयोग की व्याख्याएँ हैं । साधन अनेक हो सकते हैं । ज्ञान, कर्म
और भक्ति सभी साधन- योग है, साध्य-योग नहीं । लेकिन समत्वयोग साध्ययोग है । इस प्रकार राग-द्वेषातीत समत्वप्राप्ति की दिशा में प्रयत्न ही समालोच्य आचार-दर्शनों की नैतिक साधना का केन्द्रिय तत्त्व है।
समभाव का यही आदर्श जैनधर्म का केन्द्रिय दर्शन है। भगवान महावीर ने जिस श्रमण संस्कृति का प्रचार किया, उस श्रमण का एक अर्थ यदि समण होता है तो दूसरा समन भी अर्थात् 'जो संस्कृति समभाव में प्रवत्त कराने
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org