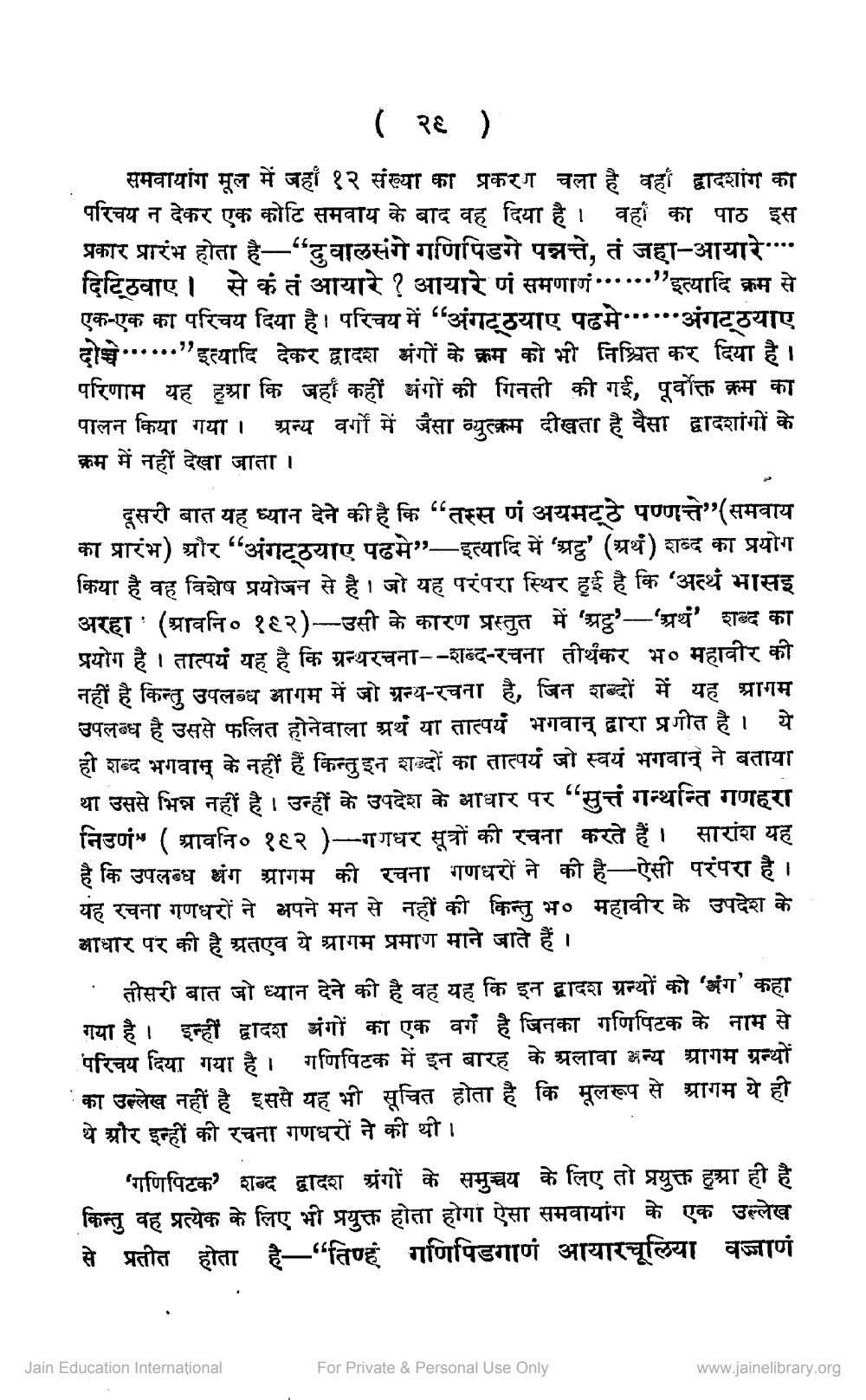________________
( २६ ) समवायांग मूल में जहाँ १२ संख्या का प्रकरण चला है वहाँ द्वादशांग का परिचय न देकर एक कोटि समवाय के बाद वह दिया है। वहीं का पाठ इस प्रकार प्रारंभ होता है—“दुवालसंगे गणिपिडगे पन्नत्ते, तं जहा-आयारे" दिठिवाए। से कं तं आयारे ? आयारे णं समणागं......."इत्यादि क्रम से एक-एक का परिचय दिया है। परिचय में "अंगठ्ठयाए पढमे...."अंगठ्ठयाए दोच्चे......" इत्यादि देकर द्वादश अंगों के क्रम को भी निश्चित कर दिया है। परिणाम यह हुआ कि जहाँ कहीं अंगों की गिनती की गई, पूर्वोक्त क्रम का पालन किया गया। अन्य वर्गों में जैसा व्युत्क्रम दीखता है वैसा द्वादशांगों के क्रम में नहीं देखा जाता।
दूसरी बात यह ध्यान देने की है कि "तस्स णं अयमठे पण्णत्ते"(समवाय का प्रारंभ) और "अंगठ्ठयाए पढमे"- इत्यादि में 'अट्ठ' (अर्थ) शब्द का प्रयोग किया है वह विशेष प्रयोजन से है । जो यह परंपरा स्थिर हुई है कि 'अत्थं भासइ अरहा' (आवनि० १६२)-उसी के कारण प्रस्तुत में 'अट्ट'-'अर्थ' शब्द का प्रयोग है । तात्पर्य यह है कि ग्रन्यरचना--शब्द-रचना तीर्थंकर भ० महावीर की नहीं है किन्तु उपलब्ध आगम में जो ग्रन्य-रचना है, जिन शब्दों में यह प्रागम उपलब्ध है उससे फलित होनेवाला अर्थ या तात्पर्य भगवान् द्वारा प्रगीत है। ये ही शब्द भगवान् के नहीं हैं किन्तु इन शब्दों का तात्पर्य जो स्वयं भगवान ने बताया था उससे भिन्न नहीं है। उन्हीं के उपदेश के आधार पर “सुत्तं गन्थन्ति गणहरा निउणं" ( पावनि० १९२ )-गगधर सूत्रों की रचना करते हैं। सारांश यह है कि उपलब्ध अंग आगम की रचना गणधरों ने की है-ऐसी परंपरा है । यह रचना गणधरों ने अपने मन से नहीं की किन्तु भ० महावीर के उपदेश के आधार पर की है अतएव ये पागम प्रमाण माने जाते हैं। - तीसरी बात जो ध्यान देने की है वह यह कि इन द्वादश ग्रन्थों को 'अंग' कहा गया है। इन्हीं द्वादश अंगों का एक वर्ग है जिनका गणिपिटक के नाम से परिचय दिया गया है। गणिपिटक में इन बारह के अलावा अन्य आगम ग्रन्थों का उल्लेख नहीं है इससे यह भी सूचित होता है कि मूलरूप से आगम ये ही थे और इन्हीं की रचना गणधरों ने की थी।
_ 'गणिपिटक' शब्द द्वादश अंगों के समुच्चय के लिए तो प्रयुक्त हुआ ही है किन्तु वह प्रत्येक के लिए भी प्रयुक्त होता होगा ऐसा समवायांग के एक उल्लेख से प्रतीत होता है-"तिण्हं गणिपिडगाणं आयारचूलिया वजाणं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org