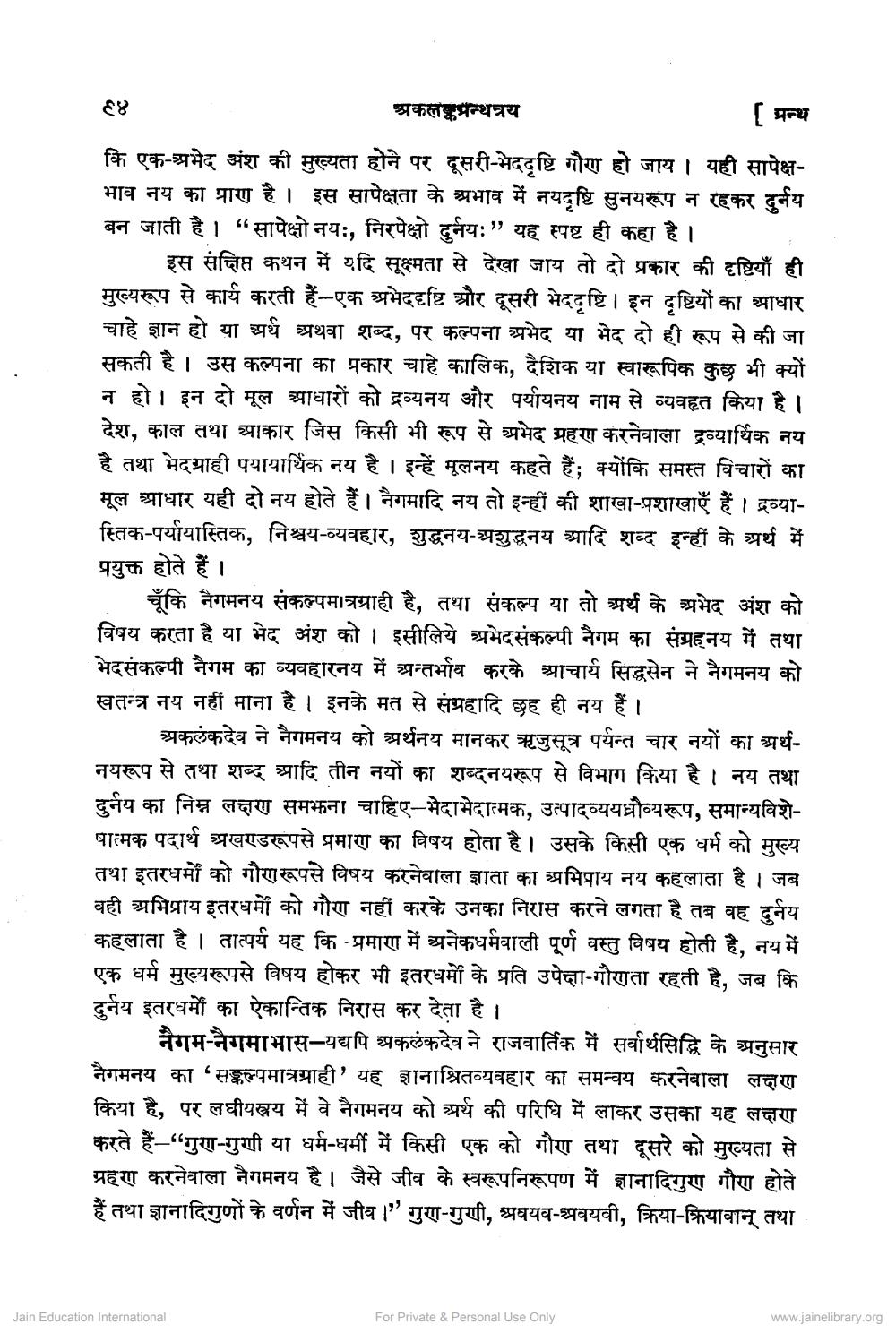________________
अकलङ्कप्रन्थत्रय
[ ग्रन्थ
कि एक-अभेद अंश की मुख्यता होने पर दूसरी-भेददृष्टि गौण हो जाय । यही सापेक्षभाव नय का प्राण है । इस सापेक्षता के अभाव में नयदृष्टि सुनयरूप न रहकर दुर्नय बन जाती है । "सापेक्षो नयः, निरपेक्षो दुर्नयः" यह स्पष्ट ही कहा है।
इस संक्षिप्त कथन में यदि सूक्ष्मता से देखा जाय तो दो प्रकार की दृष्टियाँ ही मुख्यरूप से कार्य करती हैं-एक अभेददृष्टि और दूसरी भेददृष्टि । इन दृष्टियों का आधार चाहे ज्ञान हो या अर्थ अथवा शब्द, पर कल्पना अभेद या भेद दो ही रूप से की जा सकती है। उस कल्पना का प्रकार चाहे कालिक, दैशिक या स्वारूपिक कुछ भी क्यों न हो। इन दो मूल आधारों को द्रव्यनय और पर्यायनय नाम से व्यवहृत किया है । देश, काल तथा आकार जिस किसी भी रूप से अभेद ग्रहण करनेवाला द्रव्यार्थिक नय है तथा भेदग्राही पयायार्थिक नय है। इन्हें मूलनय कहते हैं। क्योंकि समस्त विचारों का मूल आधार यही दो नय होते हैं। नैगमादि नय तो इन्हीं की शाखा-प्रशाखाएँ हैं। द्रव्यास्तिक-पर्यायास्तिक, निश्चय-व्यवहार, शुद्धनय-अशुद्धनय आदि शब्द इन्हीं के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।
चूँकि नैगमनय संकल्पमात्रग्राही है, तथा संकल्प या तो अर्थ के अभेद अंश को विषय करता है या भेद अंश को। इसीलिये अभेदसंकल्पी नैगम का संग्रहनय में तथा भेदसंकल्पी नैगम का व्यवहारनय में अन्तर्भाव करके आचार्य सिद्धसेन ने नैगमनय को खतन्त्र नय नहीं माना है । इनके मत से संग्रहादि छह ही नय हैं।
अकलंकदेव ने नैगमनय को अर्थनय मानकर ऋजुसूत्र पर्यन्त चार नयों का अर्थनयरूप से तथा शब्द आदि तीन नयों का शब्दनयरूप से विभाग किया है । नय तथा दुर्नय का निम्न लक्षण समझना चाहिए-भेदाभेदात्मक, उत्पादव्ययध्रौव्यरूप, समान्यविशेषात्मक पदार्थ अखण्डरूपसे प्रमाण का विषय होता है। उसके किसी एक धर्म को मुख्य तथा इतरधर्मों को गौण रूपसे विषय करनेवाला ज्ञाता का अभिप्राय नय कहलाता है । जब वही अभिप्राय इतरधर्मो को गौण नहीं करके उनका निरास करने लगता है तब वह दुर्नय कहलाता है । तात्पर्य यह कि -प्रमाण में अनेकधर्मवाली पूर्ण वस्तु विषय होती है, नय में एक धर्म मुख्यरूपसे विषय होकर भी इतरधर्मों के प्रति उपेक्षा-गौणता रहती है, जब कि दुर्नय इतरधर्मों का ऐकान्तिक निरास कर देता है।
नैगम-नैगमाभास-यद्यपि अकलंकदेव ने राजवार्तिक में सर्वार्थसिद्धि के अनुसार नैगमनय का 'सङ्कल्पमात्रग्राही' यह ज्ञानाश्रितव्यवहार का समन्वय करनेवाला लक्षण किया है, पर लघीयस्त्रय में वे नैगमनय को अर्थ की परिधि में लाकर उसका यह लक्षण करते हैं-"गुण-गुणी या धर्म-धर्मी में किसी एक को गौण तथा दूसरे को मुख्यता से ग्रहण करनेवाला नैगमनय है। जैसे जीव के स्वरूपनिरूपण में ज्ञानादिगुण गौण होते हैं तथा ज्ञानादिगुणों के वर्णन में जीव ।" गुण-गुणी, अवयव-अवयवी, क्रिया-क्रियावान् तथा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org