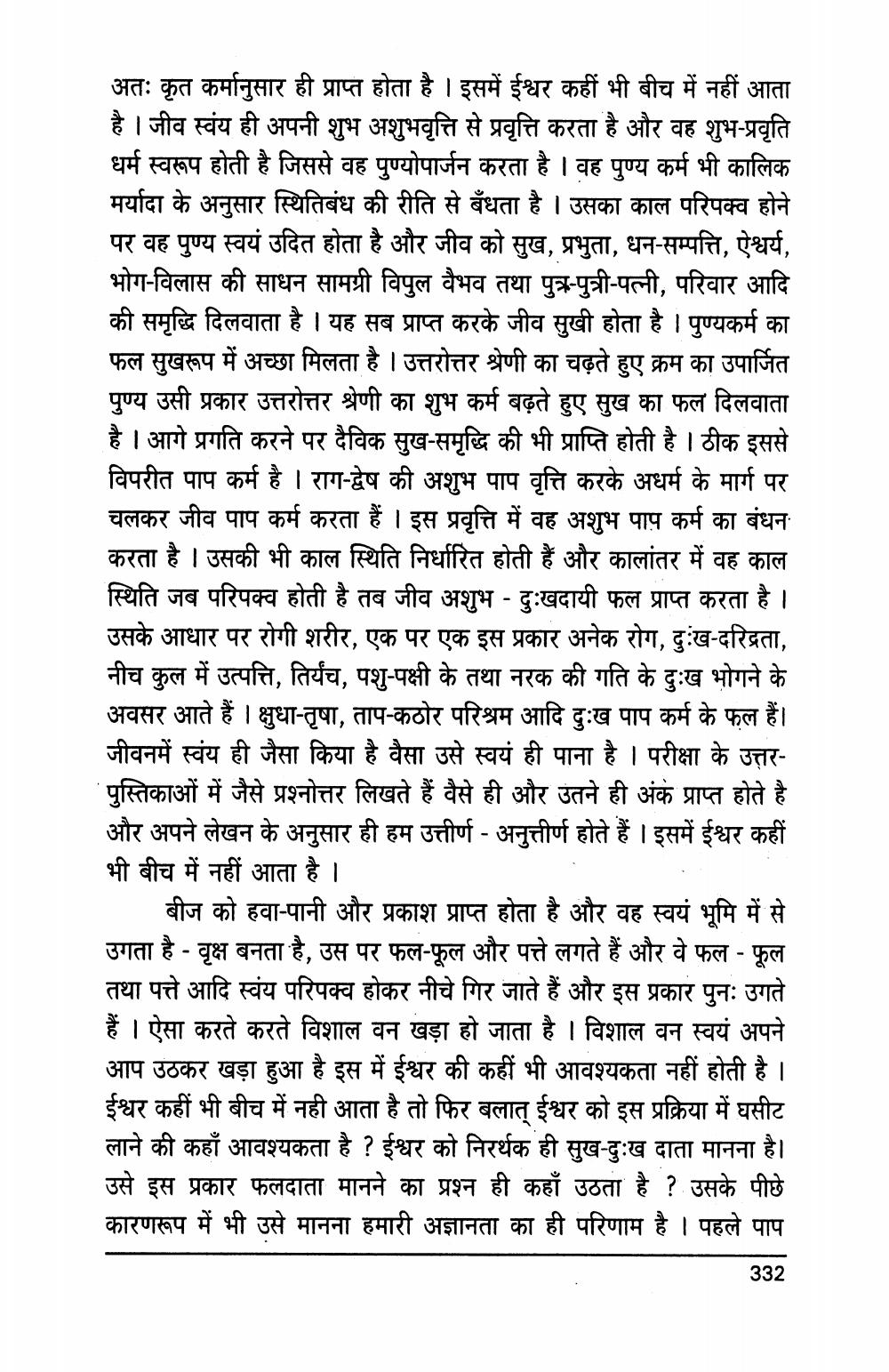________________
अतः कृत कर्मानुसार ही प्राप्त होता है । इसमें ईश्वर कहीं भी बीच में नहीं आता है । जीव स्वंय ही अपनी शुभ अशुभवृत्ति से प्रवृत्ति करता है और वह शुभ-प्रवृति धर्म स्वरूप होती है जिससे वह पुण्योपार्जन करता है । वह पुण्य कर्म भी कालिक मर्यादा के अनुसार स्थितिबंध की रीति से बँधता है । उसका काल परिपक्व होने पर वह पुण्य स्वयं उदित होता है और जीव को सुख, प्रभुता, धन-सम्पत्ति, ऐश्वर्य, भोग-विलास की साधन सामग्री विपुल वैभव तथा पुत्र-पुत्री-पत्नी, परिवार आदि की समृद्धि दिलवाता है । यह सब प्राप्त करके जीव सुखी होता है । पुण्यकर्म का फल सुखरूप में अच्छा मिलता है । उत्तरोत्तर श्रेणी का चढ़ते हुए क्रम का उपार्जित पुण्य उसी प्रकार उत्तरोत्तर श्रेणी का शुभ कर्म बढ़ते हुए सुख का फल दिलवाता है। आगे प्रगति करने पर दैविक सुख-समृद्धि की भी प्राप्ति होती है । ठीक इससे विपरीत पाप कर्म है । राग-द्वेष की अशुभ पाप वृत्ति करके अधर्म के मार्ग पर चलकर जीव पाप कर्म करता हैं । इस प्रवृत्ति में वह अशुभ पाप कर्म का बंधन करता है । उसकी भी काल स्थिति निर्धारित होती हैं और कालांतर में वह काल स्थिति जब परिपक्व होती है तब जीव अशुभ दुःखदायी फल प्राप्त करता है । उसके आधार पर रोगी शरीर, एक पर एक इस प्रकार अनेक रोग, दुःख- दरिद्रता, नीच कुल में उत्पत्ति, तिर्यंच, पशु-पक्षी के तथा नरक की गति के दुःख भोगने के अवसर आते हैं । क्षुधा-तृषा, ताप - कठोर परिश्रम आदि दुःख पाप कर्म के फल हैं। जीवनमें स्वंय ही जैसा किया है वैसा उसे स्वयं ही पाना है । परीक्षा के उत्तरपुस्तिकाओं में जैसे प्रश्नोत्तर लिखते हैं वैसे ही और उतने ही अंक प्राप्त होते है और अपने लेखन के अनुसार ही हम उत्तीर्ण - अनुत्तीर्ण होते हैं । इसमें ईश्वर कहीं भी बीच में नहीं आता है ।
बीज को हवा - पानी और प्रकाश प्राप्त होता है और वह स्वयं भूमि में से उगता है - वृक्ष बनता है, उस पर फल-फूल और पत्ते लगते हैं और वे फल - फूल तथा पत्ते आदि स्वंय परिपक्व होकर नीचे गिर जाते हैं और इस प्रकार पुनः उगते हैं । ऐसा करते करते विशाल वन खड़ा हो जाता है । विशाल वन स्वयं अपने आप उठकर खड़ा हुआ है इस में ईश्वर की कहीं भी आवश्यकता नहीं होती है । ईश्वर कहीं भी बीच में नही आता है तो फिर बलात् ईश्वर को इस प्रक्रिया में घसीट लाने की कहाँ आवश्यकता है ? ईश्वर को निरर्थक ही सुख-दुःख दाता मानना है। उसे इस प्रकार फलदाता मानने का प्रश्न ही कहाँ उठता है ? उसके पीछे कारणरूप में भी उसे मानना हमारी अज्ञानता का ही परिणाम है । पहले पाप
332
-