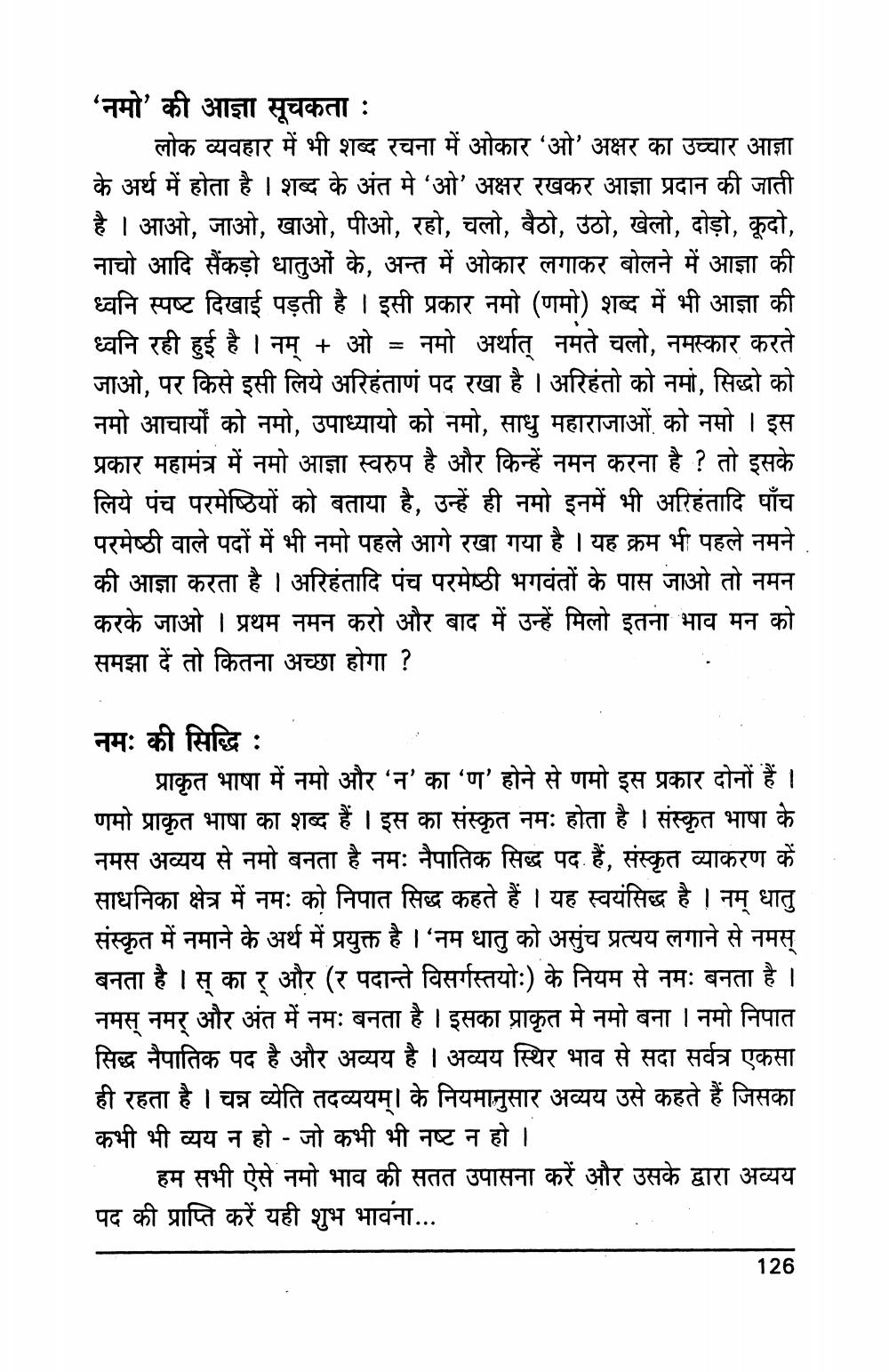________________
'नमो' की आज्ञा सूचकता :
लोक व्यवहार में भी शब्द रचना में ओकार 'ओ' अक्षर का उच्चार आज्ञा के अर्थ में होता है । शब्द के अंत में 'ओ' अक्षर रखकर आज्ञा प्रदान की जाती है । आओ, जाओ, खाओ, पीओ, रहो, चलो, बैठो, उठो, खेलो, दोड़ो, कुदो, नाचो आदि सैंकड़ो धातुओं के, अन्त में ओकार लगाकर बोलने में आज्ञा की ध्वनि स्पष्ट दिखाई पड़ती है । इसी प्रकार नमो (णमो) शब्द में भी आज्ञा की ध्वनि रही हुई है । नम् + ओ = नमो अर्थात् नमते चलो, नमस्कार करते जाओ, पर किसे इसी लिये अरिहंताणं पद रखा है । अरिहंतो को नमी, सिद्धो को नमो आचार्यों को नमो, उपाध्यायो को नमो, साधु महाराजाओं को नमो । इस प्रकार महामंत्र में नमो आज्ञा स्वरुप है और किन्हें नमन करना है ? तो इसके लिये पंच परमेष्ठियों को बताया है, उन्हें ही नमो इनमें भी अरिहंतादि पाँच परमेष्ठी वाले पदों में भी नमो पहले आगे रखा गया है । यह क्रम भी पहले नमने की आज्ञा करता है । अरिहंतादि पंच परमेष्ठी भगवंतों के पास जाओ तो नमन करके जाओ । प्रथम नमन करो और बाद में उन्हें मिलो इतना भाव मन को समझा दें तो कितना अच्छा होगा ?
नमः की सिद्धि :
__प्राकृत भाषा में नमो और 'न' का 'ण' होने से णमो इस प्रकार दोनों हैं । णमो प्राकृत भाषा का शब्द हैं । इस का संस्कृत नमः होता है । संस्कृत भाषा के नमस अव्यय से नमो बनता है नमः नैपातिक सिद्ध पद हैं, संस्कृत व्याकरण के साधनिका क्षेत्र में नमः को निपात सिद्ध कहते हैं । यह स्वयंसिद्ध है । नम् धातु संस्कृत में नमाने के अर्थ में प्रयुक्त है । ‘नम धातु को असुंच प्रत्यय लगाने से नमस् बनता है । स् का र् और (र पदान्ते विसर्गस्तयोः) के नियम से नमः बनता है । नमस् नमर् और अंत में नमः बनता है । इसका प्राकृत मे नमो बना । नमो निपात सिद्ध नैपातिक पद है और अव्यय है । अव्यय स्थिर भाव से सदा सर्वत्र एकसा ही रहता है । चन्न व्येति तदव्ययम्। के नियमानुसार अव्यय उसे कहते हैं जिसका कभी भी व्यय न हो - जो कभी भी नष्ट न हो ।
हम सभी ऐसे नमो भाव की सतत उपासना करें और उसके द्वारा अव्यय पद की प्राप्ति करें यही शुभ भावना...
126