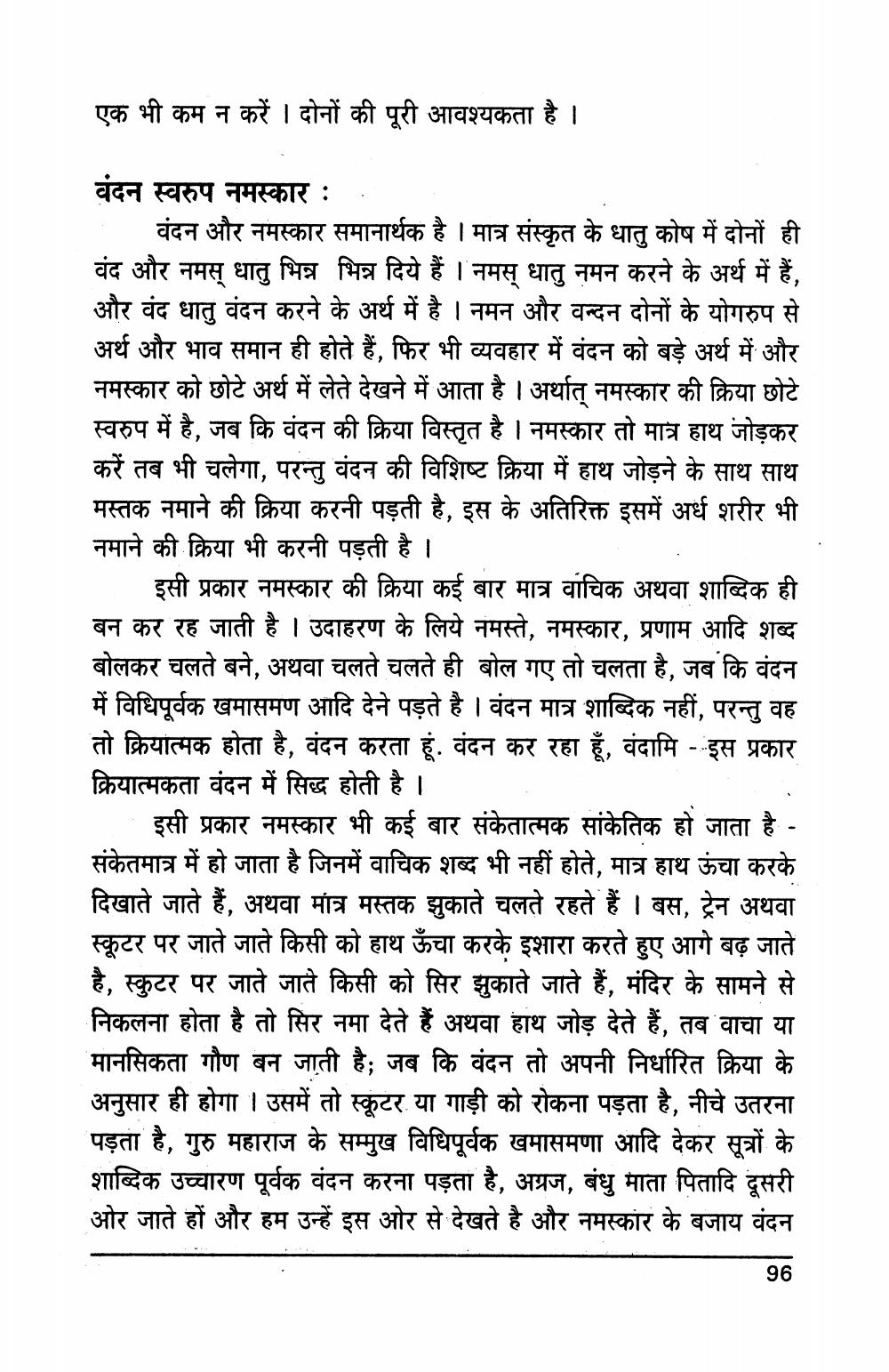________________
एक भी कम न करें । दोनों की पूरी आवश्यकता है ।
वंदन स्वरुप नमस्कार :
वंदन और नमस्कार समानार्थक है । मात्र संस्कृत के धातु कोष में दोनों ही वंद और नमस् धातु भिन्न भिन्न दिये हैं । नमस् धातु नमन करने के अर्थ में हैं, I और वंद धातु वंदन करने के अर्थ में है । नमन और वन्दन दोनों के योगरुप से अर्थ और भाव समान ही होते हैं, फिर भी व्यवहार में वंदन को बड़े अर्थ में और नमस्कार को छोटे अर्थ में लेते देखने में आता है । अर्थात् नमस्कार की क्रिया छोटे स्वरुप में है, जब कि वंदन की क्रिया विस्तृत है । नमस्कार तो मात्र हाथ जोड़कर करें तब भी चलेगा, परन्तु वंदन की विशिष्ट क्रिया में हाथ जोड़ने के साथ साथ मस्तक नमाने की क्रिया करनी पड़ती है, इस के अतिरिक्त इसमें अर्ध शरीर भी नमाने की क्रिया भी करनी पड़ती है ।
इसी प्रकार नमस्कार की क्रिया कई बार मात्र वाचिक अथवा शाब्दिक ही बन कर रह जाती है । उदाहरण के लिये नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम आदि शब्द बोलकर चलते बने, अथवा चलते चलते ही बोल गए तो चलता है, जब कि वंदन में विधिपूर्वक खमासमण आदि देने पड़ते है । वंदन मात्र शाब्दिक नहीं, परन्तु वह तक्रियात्मक होता है, वंदन करता हूं. वंदन कर रहा हूँ, वंदामि इस प्रकार क्रियात्मकता वंदन में सिद्ध होती है ।
-
इसी प्रकार नमस्कार भी कई बार संकेतात्मक सांकेतिक हो जाता है संकेतमात्र में हो जाता है जिनमें वाचिक शब्द भी नहीं होते, मात्र हाथ ऊंचा करके दिखाते जाते हैं, अथवा मात्र मस्तक झुकाते चलते रहते हैं । बस, ट्रेन अथवा स्कूटर पर जाते जाते किसी को हाथ ऊँचा करके इशारा करते हुए आगे बढ़ जाते है, स्कुटर पर जाते जाते किसी को सिर झुकाते जाते हैं, मंदिर के सामने से निकलना होता है तो सिर नमा देते हैं अथवा हाथ जोड़ देते हैं, तब वाचा या मानसिकता गौण बन जाती है; जब कि वंदन तो अपनी निर्धारित क्रिया के अनुसार ही होगा । उसमें तो स्कूटर या गाड़ी को रोकना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है, गुरु महाराज के सम्मुख विधिपूर्वक खमासमणा आदि देकर सूत्रों के शाब्दिक उच्चारण पूर्वक वंदन करना पड़ता है, अग्रज, बंधु माता पितादि दूसरी ओर जाते हों और हम उन्हें इस ओर से देखते है और नमस्कार के बजाय वंदन
-
96