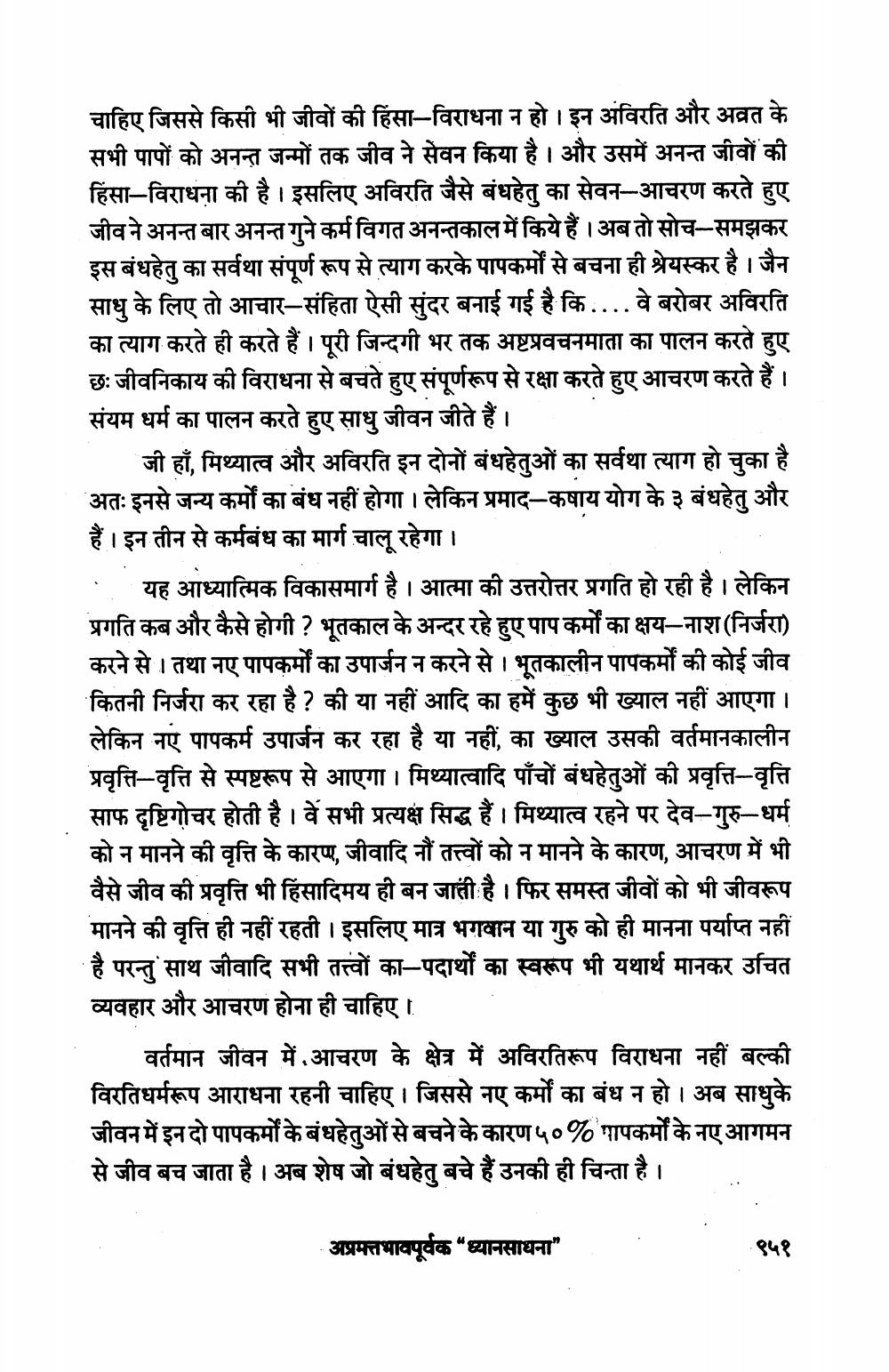________________
चाहिए जिससे किसी भी जीवों की हिंसा-विराधना न हो । इन अविरति और अव्रत के सभी पापों को अनन्त जन्मों तक जीव ने सेवन किया है । और उसमें अनन्त जीवों की हिंसा-विराधना की है। इसलिए अविरति जैसे बंधहेतु का सेवन-आचरण करते हुए जीवने अनन्त बार अनन्त गुने कर्म विगत अनन्तकाल में किये हैं । अब तो सोच-समझकर इस बंधहेतु का सर्वथा संपूर्ण रूप से त्याग करके पापकर्मों से बचना ही श्रेयस्कर है । जैन साधु के लिए तो आचार संहिता ऐसी सुंदर बनाई गई है कि.... वे बरोबर अविरति का त्याग करते ही करते हैं । पूरी जिन्दगी भर तक अष्टप्रवचनमाता का पालन करते हुए छः जीवनिकाय की विराधना से बचते हुए संपूर्णरूप से रक्षा करते हुए आचरण करते हैं। संयम धर्म का पालन करते हुए साधु जीवन जीते हैं।
जी हाँ, मिथ्यात्व और अविरति इन दोनों बंधहेतुओं का सर्वथा त्याग हो चुका है अतः इनसे जन्य कर्मों का बंध नहीं होगा। लेकिन प्रमाद-कषाय योग के ३ बंधहेतु और हैं। इन तीन से कर्मबंध का मार्ग चालू रहेगा। - यह आध्यात्मिक विकासमार्ग है । आत्मा की उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। लेकिन प्रगति कब और कैसे होगी? भूतकाल के अन्दर रहे हुए पाप कर्मों का क्षय-नाश(निर्जरा) करने से । तथा नए पापकर्मों का उपार्जन न करने से । भूतकालीन पापकर्मों की कोई जीव कितनी निर्जरा कर रहा है? की या नहीं आदि का हमें कुछ भी ख्याल नहीं आएगा। लेकिन नए पापकर्म उपार्जन कर रहा है या नहीं, का ख्याल उसकी वर्तमानकालीन प्रवृत्ति-वृत्ति से स्पष्टरूप से आएगा। मिथ्यात्वादि पाँचों बंधहेतुओं की प्रवृत्ति-वृत्ति साफ दृष्टिगोचर होती है। वे सभी प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। मिथ्यात्व रहने पर देव-गुरु-धर्म को न मानने की वृत्ति के कारण, जीवादि नौं तत्त्वों को न मानने के कारण, आचरण में भी वैसे जीव की प्रवृत्ति भी हिंसादिमय ही बन जाती है। फिर समस्त जीवों को भी जीवरूप मानने की वृत्ति ही नहीं रहती। इसलिए मात्र भगवान या गुरु को ही मानना पर्याप्त नहीं है परन्तु साथ जीवादि सभी तत्त्वों का-पदार्थों का स्वरूप भी यथार्थ मानकर उचित व्यवहार और आचरण होना ही चाहिए।
वर्तमान जीवन में आचरण के क्षेत्र में अविरतिरूप विराधना नहीं बल्की विरतिधर्मरूप आराधना रहनी चाहिए। जिससे नए कर्मों का बंध न हो । अब साधुके जीवन में इन दो पापकर्मों के बंधहेतुओं से बचने के कारण५०% पापकर्मों के नए आगमन से जीव बच जाता है। अब शेष जो बंधहेतु बचे हैं उनकी ही चिन्ता है।
अप्रमत्तभावपूर्वक "ध्यानसाधना"
९५१