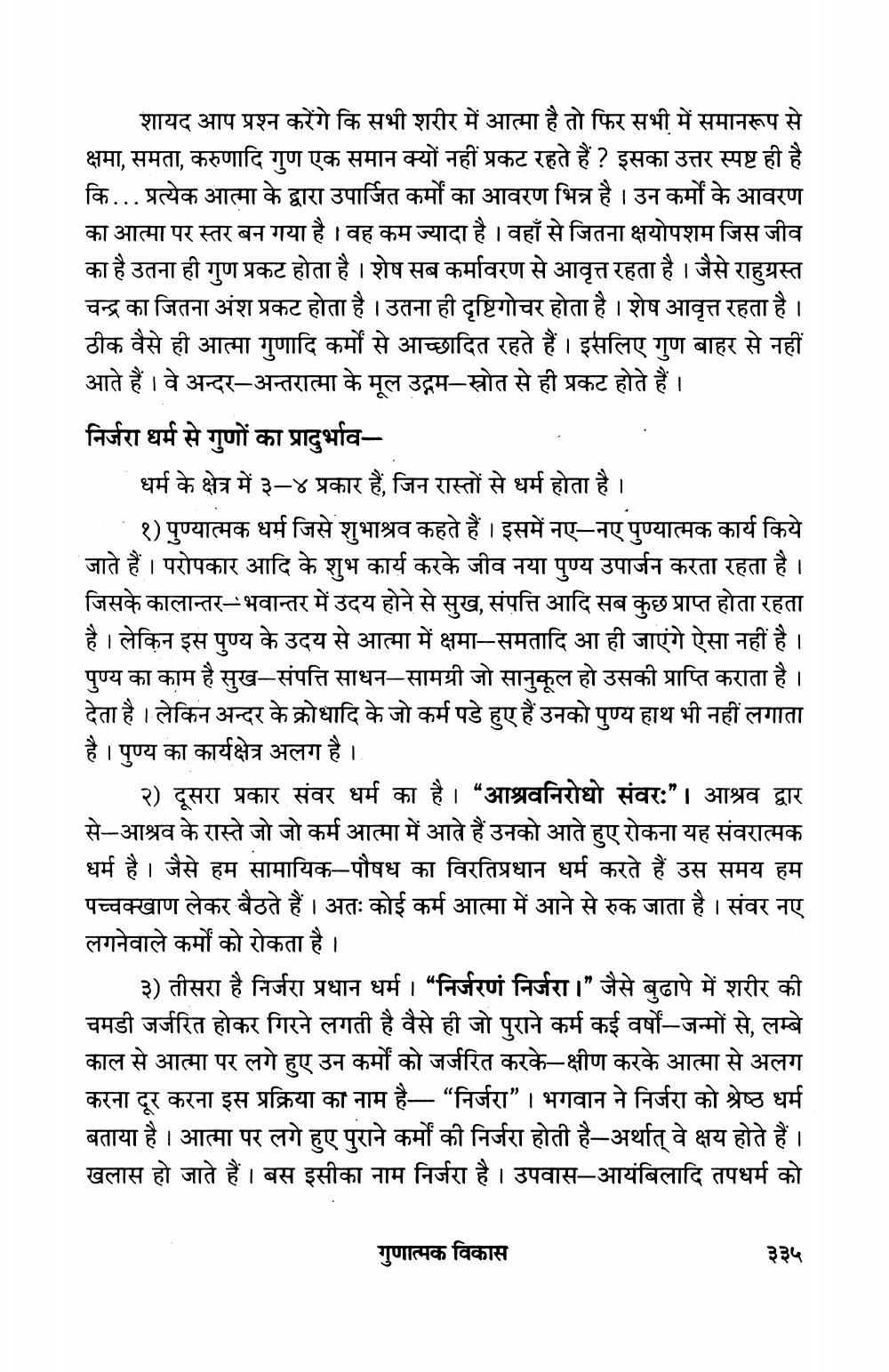________________
शायद आप प्रश्न करेंगे कि सभी शरीर में आत्मा है तो फिर सभी में समानरूप से क्षमा, समता, करुणादि गुण एक समान क्यों नहीं प्रकट रहते हैं ? इसका उत्तर स्पष्ट ही है कि... प्रत्येक आत्मा के द्वारा उपार्जित कर्मों का आवरण भिन्न है। उन कर्मों के आवरण का आत्मा पर स्तर बन गया है । वह कम ज्यादा है । वहाँ से जितना क्षयोपशम जिस जीव का है उतना ही गुण प्रकट होता है । शेष सब कर्मावरण से आवृत्त रहता है । जैसे राहुग्रस्त चन्द्र का जितना अंश प्रकट होता है । उतना ही दृष्टिगोचर होता है । शेष आवृत्त रहता है। ठीक वैसे ही आत्मा गुणादि कर्मों से आच्छादित रहते हैं। इसलिए गुण बाहर से नहीं आते हैं । वे अन्दर-अन्तरात्मा के मूल उद्गम-स्रोत से ही प्रकट होते हैं। निर्जरा धर्म से गुणों का प्रादुर्भाव
धर्म के क्षेत्र में ३-४ प्रकार हैं, जिन रास्तों से धर्म होता है।
१) पुण्यात्मक धर्म जिसे शुभाश्रव कहते हैं । इसमें नए-नए पुण्यात्मक कार्य किये जाते हैं । परोपकार आदि के शुभ कार्य करके जीव नया पुण्य उपार्जन करता रहता है। जिसके कालान्तर-भवान्तर में उदय होने से सुख, संपत्ति आदि सब कुछ प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस पुण्य के उदय से आत्मा में क्षमा-समतादि आ ही जाएंगे ऐसा नहीं है । पुण्य का काम है सुख-संपत्ति साधन-सामग्री जो सानुकूल हो उसकी प्राप्ति कराता है । देता है । लेकिन अन्दर के क्रोधादि के जो कर्म पडे हुए हैं उनको पुण्य हाथ भी नहीं लगाता है । पुण्य का कार्यक्षेत्र अलग है।
२) दूसरा प्रकार संवर धर्म का है। “आश्रवनिरोधो संवरः"। आश्रव द्वार से-आश्रव के रास्ते जो जो कर्म आत्मा में आते हैं उनको आते हुए रोकना यह संवरात्मक धर्म है। जैसे हम सामायिक–पौषध का विरतिप्रधान धर्म करते हैं उस समय हम पच्चक्खाण लेकर बैठते हैं । अतः कोई कर्म आत्मा में आने से रुक जाता है । संवर नए लगनेवाले कर्मों को रोकता है।
३) तीसरा है निर्जरा प्रधान धर्म । “निर्जरणं निर्जरा।" जैसे बुढापे में शरीर की चमडी जर्जरित होकर गिरने लगती है वैसे ही जो पुराने कर्म कई वर्षों-जन्मों से, लम्बे काल से आत्मा पर लगे हुए उन कर्मों को जर्जरित करके-क्षीण करके आत्मा से अलग करना दूर करना इस प्रक्रिया का नाम है- “निर्जरा" । भगवान ने निर्जरा को श्रेष्ठ धर्म बताया है । आत्मा पर लगे हुए पुराने कर्मों की निर्जरा होती है-अर्थात् वे क्षय होते हैं। खलास हो जाते हैं। बस इसीका नाम निर्जरा है। उपवास-आयंबिलादि तपधर्म को
गुणात्मक विकास
३३५