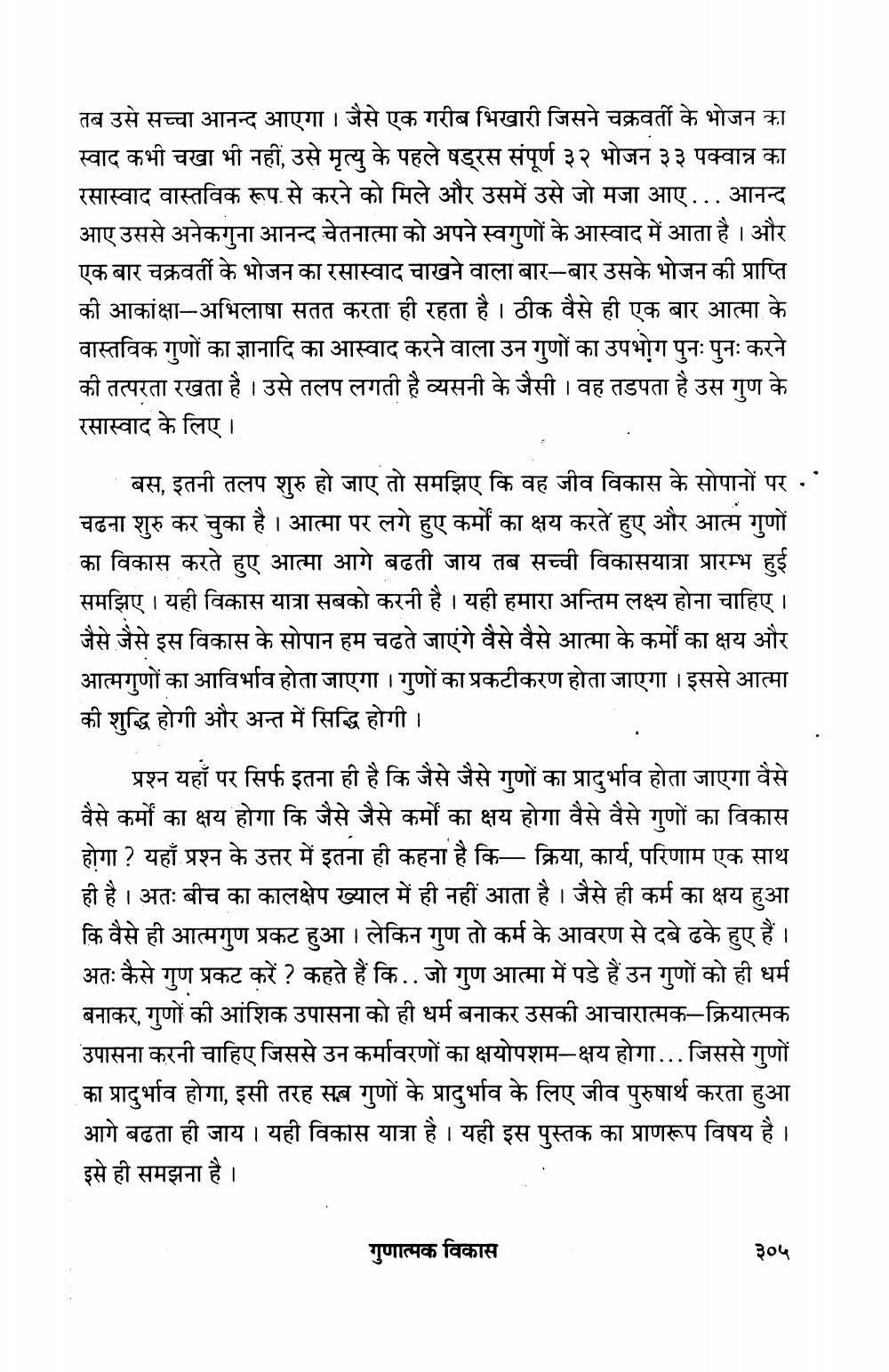________________
तब उसे सच्चा आनन्द आएगा। जैसे एक गरीब भिखारी जिसने चक्रवर्ती के भोजन का स्वाद कभी चखा भी नहीं, उसे मृत्यु के पहले षड्रस संपूर्ण ३२ भोजन ३३ पक्वान्न का रसास्वाद वास्तविक रूप से करने को मिले और उसमें उसे जो मजा आए... आनन्द आए उससे अनेकगुना आनन्द चेतनात्मा को अपने स्वगुणों के आस्वाद में आता है । और एक बार चक्रवर्ती के भोजन का रसास्वाद चाखने वाला बार-बार उसके भोजन की प्राप्ति की आकांक्षा-अभिलाषा सतत करता ही रहता है । ठीक वैसे ही एक बार आत्मा के वास्तविक गुणों का ज्ञानादि का आस्वाद करने वाला उन गुणों का उपभोग पुनः पुनः करने की तत्परता रखता है । उसे तलप लगती है व्यसनी के जैसी । वह तडपता है उस गुण के रसास्वाद के लिए।
बस, इतनी तलप शुरु हो जाए तो समझिए कि वह जीव विकास के सोपानों पर ... चढना शुरु कर चुका है । आत्मा पर लगे हुए कर्मों का क्षय करते हुए और आत्म गुणों का विकास करते हए आत्मा आगे बढती जाय तब सच्ची विकासयात्रा प्रारम्भ हुई समझिए । यही विकास यात्रा सबको करनी है । यही हमारा अन्तिम लक्ष्य होना चाहिए । जैसे जैसे इस विकास के सोपान हम चढते जाएंगे वैसे वैसे आत्मा के कर्मों का क्षय और आत्मगुणों का आविर्भाव होता जाएगा । गुणों का प्रकटीकरण होता जाएगा। इससे आत्मा की शुद्धि होगी और अन्त में सिद्धि होगी।
प्रश्न यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि जैसे जैसे गुणों का प्रादुर्भाव होता जाएगा वैसे वैसे कर्मों का क्षय होगा कि जैसे जैसे कर्मों का क्षय होगा वैसे वैसे गुणों का विकास होगा? यहाँ प्रश्न के उत्तर में इतना ही कहना है कि क्रिया, कार्य, परिणाम एक साथ ही है । अतः बीच का कालक्षेप ख्याल में ही नहीं आता है । जैसे ही कर्म का क्षय हुआ कि वैसे ही आत्मगुण प्रकट हुआ। लेकिन गुण तो कर्म के आवरण से दबे ढके हुए हैं। अतः कैसे गुण प्रकट करें? कहते हैं कि.. जो गुण आत्मा में पडे हैं उन गुणों को ही धर्म बनाकर, गुणों की आंशिक उपासना को ही धर्म बनाकर उसकी आचारात्मक क्रियात्मक उपासना करनी चाहिए जिससे उन कर्मावरणों का क्षयोपशम–क्षय होगा... जिससे गणों का प्रादुर्भाव होगा, इसी तरह सब गुणों के प्रादुर्भाव के लिए जीव पुरुषार्थ करता हुआ आगे बढ़ता ही जाय । यही विकास यात्रा है । यही इस पुस्तक का प्राणरूप विषय है । इसे ही समझना है।
गुणात्मक विकास
३०५