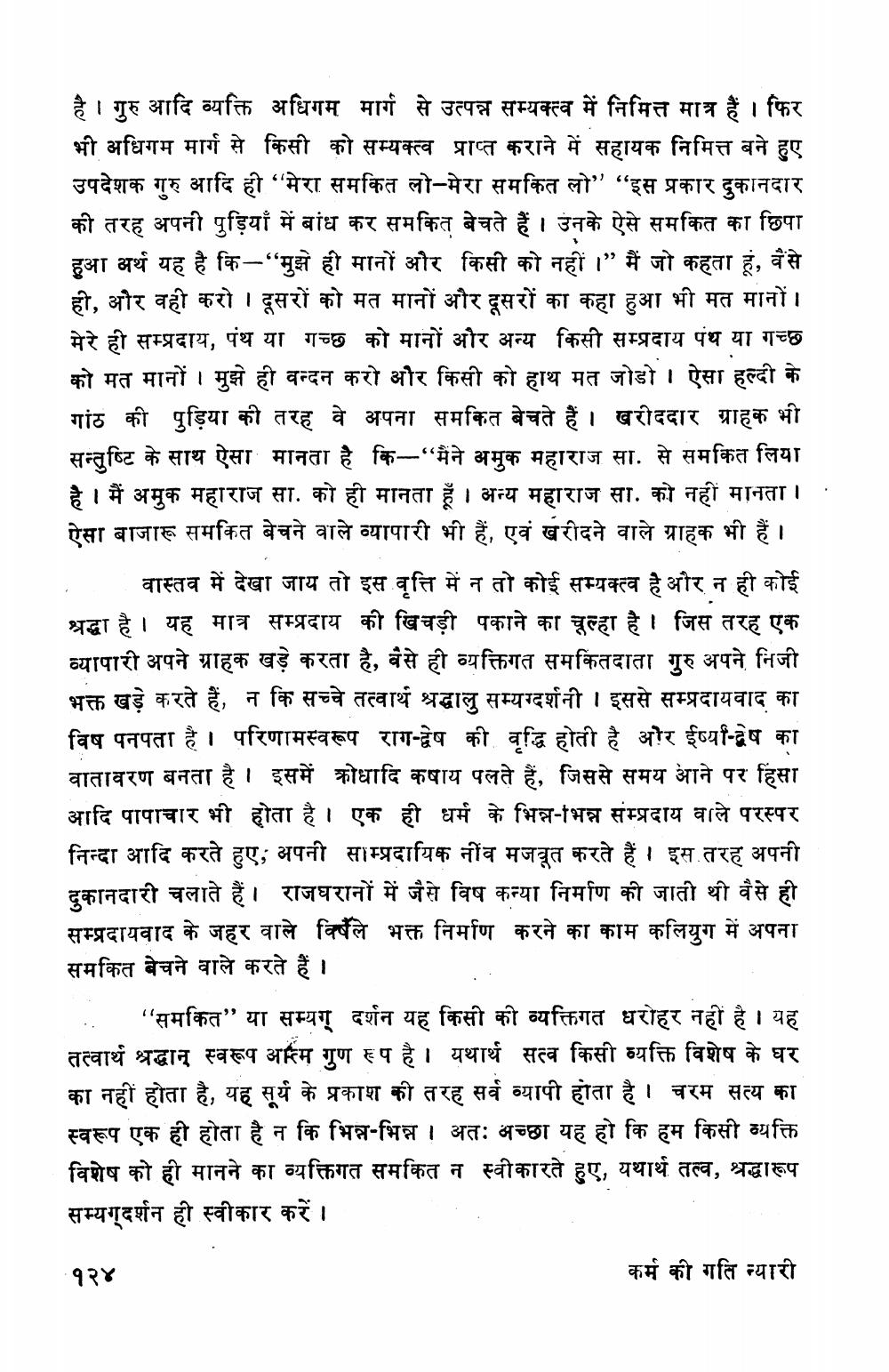________________
है | गुरु आदि व्यक्ति अधिगम मार्ग से उत्पन्न सम्यक्त्व में निमित्त मात्र । फिर भी अधिगम मार्ग से किसी को सम्यक्त्व प्राप्त कराने में सहायक निमित्त बने हुए उपदेशक गुरु आदि ही " मेरा समकित लो - मेरा समकित लो" "इस प्रकार दुकानदार की तरह अपनी पुड़ियाँ में बांध कर समकित बेचते हैं । उनके ऐसे समकित का छिपा हुआ अर्थ यह है कि - "मुझे ही मानों और किसी को नहीं ।" मैं जो कहता हूं, वैसे ही, और वही करो । दूसरों को मत मानों और दूसरों का कहा हुआ भी मत मानों । मेरे ही सम्प्रदाय, पंथ या गच्छ को मानों और अन्य किसी सम्प्रदाय पंथ या गच्छ को मत मानों । मुझे ही वन्दन करो और किसी को हाथ मत जोडो । ऐसा हल्दी के गांठ की पुड़िया की तरह वे अपना समकित बेचते हैं । खरीददार ग्राहक भी सन्तुष्टि के साथ ऐसा मानता है कि - " मैंने अमुक महाराज सा. से समकित लिया है । मैं अमुक महाराज सा. को ही मानता हूँ । अन्य महाराज सा. को नहीं मानता । ऐसा बाजारू समकित बेचने वाले व्यापारी भी हैं, एवं खरीदने वाले ग्राहक भी हैं ।
वास्तव में देखा जाय तो इस वृत्ति में न तो कोई सम्यक्त्व है और न ही कोई श्रद्धा है । यह मात्र सम्प्रदाय की खिचड़ी पकाने का चूल्हा है । जिस तरह एक व्यापारी अपने ग्राहक खड़े करता है, वैसे ही व्यक्तिगत समकितदाता गुरु अपने निजी भक्त खड़े करते हैं, न कि सच्चे तत्वार्थ श्रद्धालु सम्यग्दर्शनी । इससे सम्प्रदायवाद का विष पनपता है । परिणामस्वरूप राग-द्वेष की वृद्धि होती है और ईर्ष्या-द्वेष का वातावरण बनता है । इसमें क्रोधादि कषाय पलते हैं, जिससे समय आने पर हिंसा आदि पापाचार भी होता है । एक ही धर्म के भिन्न-भिन्न संम्प्रदाय वाले परस्पर निन्दा आदि करते हुए, अपनी साम्प्रदायिक नींव मजबूत करते हैं । इस तरह अपनी दुकानदारी चलाते हैं। राजघरानों में जैसे विष कन्या निर्माण की जाती थी वैसे ही सम्प्रदायवाद के जहर वाले विषैले भक्त निर्माण करने का काम कलियुग में अपना समकित बेचने वाले करते हैं ।
" समकित " या सम्यग् दर्शन यह किसी की व्यक्तिगत धरोहर नहीं है । यह तत्वार्थ श्रद्धान् स्वरूप आत्म गुण रूप है । यथार्थ सत्व किसी व्यक्ति विशेष के घर का नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश की तरह सर्व व्यापी होता है । चरम सत्य का स्वरूप एक ही होता है न कि भिन्न-भिन्न । अत: अच्छा यह हो कि हम किसी व्यक्ति विशेष को ही मानने का व्यक्तिगत समकित न स्वीकारते हुए, यथार्थ तत्व, श्रद्धारूप सम्यग्दर्शन ही स्वीकार करें ।
१२४
कर्म की गति न्यारी