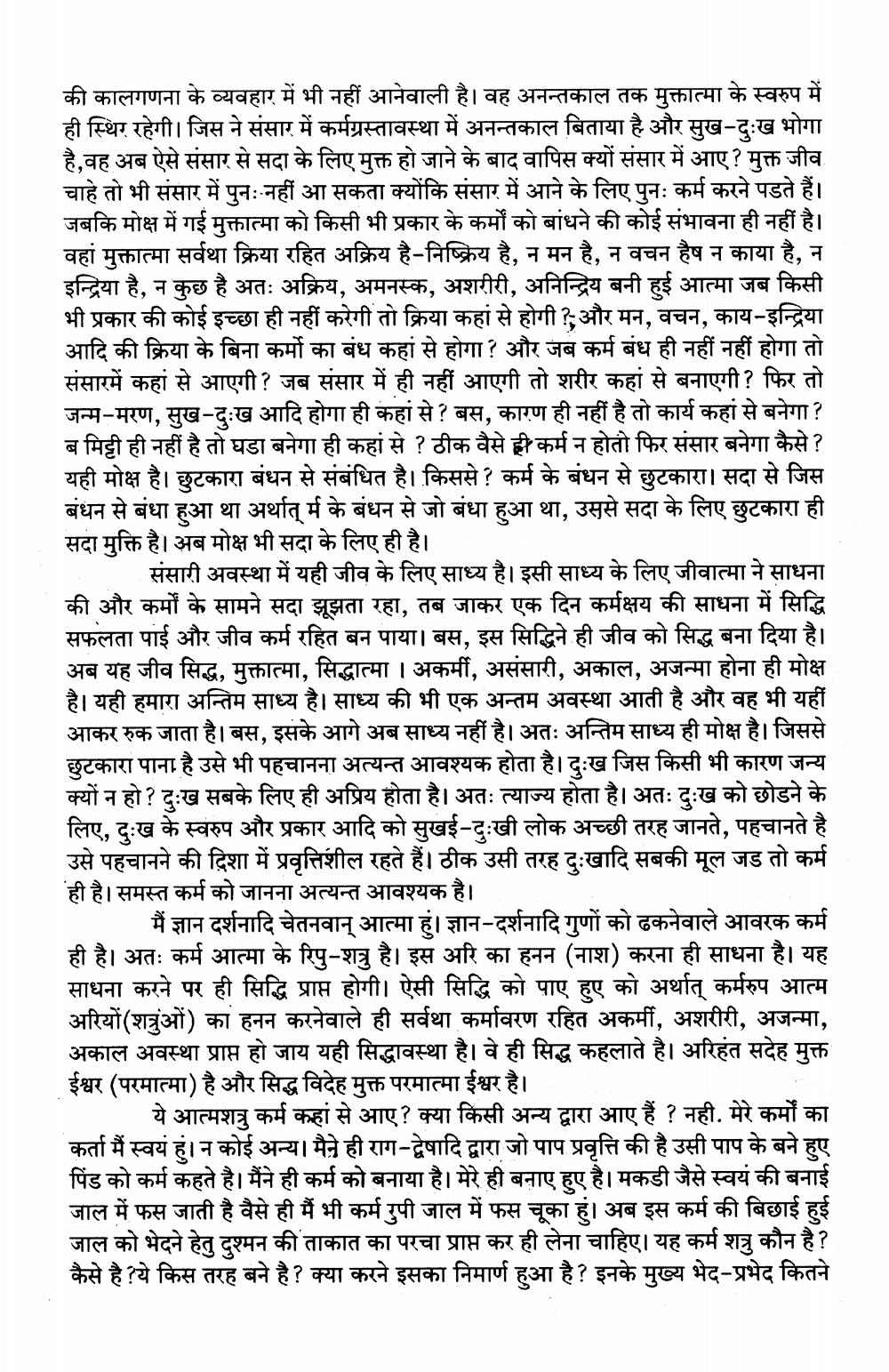________________
की कालगणना के व्यवहार में भी नहीं आनेवाली है। वह अनन्तकाल तक मुक्तात्मा के स्वरुप में ही स्थिर रहेगी। जिस ने संसार में कर्मग्रस्तावस्था में अनन्तकाल बिताया है और सुख-दुःख भोगा है,वह अब ऐसे संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाने के बाद वापिस क्यों संसार में आए? मुक्त जीव चाहे तो भी संसार में पुनः नहीं आ सकता क्योंकि संसार में आने के लिए पुनः कर्म करने पड़ते हैं। जबकि मोक्ष में गई मुक्तात्मा को किसी भी प्रकार के कर्मों को बांधने की कोई संभावना ही नहीं है। वहां मुक्तात्मा सर्वथा क्रिया रहित अक्रिय है-निष्क्रिय है, न मन है, न वचन हैष न काया है, न इन्द्रिया है, न कुछ है अतः अक्रिय, अमनस्क, अशरीरी, अनिन्द्रिय बनी हुई आत्मा जब किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं करेगी तो क्रिया कहां से होगी? और मन, वचन, काय-इन्द्रिया आदि की क्रिया के बिना कर्मो का बंध कहां से होगा? और जब कर्म बंध ही नहीं नहीं होगा तो संसारमें कहां से आएगी? जब संसार में ही नहीं आएगी तो शरीर कहां से बनाएगी? फिर तो जन्म-मरण, सुख-दुःख आदि होगा ही कहां से? बस, कारण ही नहीं है तो कार्य कहां से बनेगा? ब मिट्टी ही नहीं है तो घडा बनेगा ही कहां से ? ठीक वैसे ही कर्म न होतो फिर संसार बनेगा कैसे? यही मोक्ष है। छुटकारा बंधन से संबंधित है। किससे? कर्म के बंधन से छुटकारा। सदा से जिस बंधन से बंधा हुआ था अर्थात् म के बंधन से जो बंधा हुआ था, उससे सदा के लिए छुटकारा ही सदा मुक्ति है। अब मोक्ष भी सदा के लिए ही है।
___संसारी अवस्था में यही जीव के लिए साध्य है। इसी साध्य के लिए जीवात्मा ने साधना की और कर्मों के सामने सदा झूझता रहा, तब जाकर एक दिन कर्मक्षय की साधना में सिद्धि सफलता पाई और जीव कर्म रहित बन पाया। बस, इस सिद्धिने ही जीव को सिद्ध बना दिया है। अब यह जीव सिद्ध, मुक्तात्मा, सिद्धात्मा । अकर्मी, असंसारी, अकाल, अजन्मा होना ही मोक्ष है। यही हमारा अन्तिम साध्य है। साध्य की भी एक अन्तम अवस्था आती है और वह भी यहीं आकर रुक जाता है। बस, इसके आगे अब साध्य नहीं है। अतः अन्तिम साध्य ही मोक्ष है। जिससे छुटकारा पाना है उसे भी पहचानना अत्यन्त आवश्यक होता है। दुःख जिस किसी भी कारण जन्य क्यों न हो? दुःख सबके लिए ही अप्रिय होता है। अतः त्याज्य होता है। अतः दुःख को छोड़ने के लिए, दुःख के स्वरुप और प्रकार आदि को सुखई-दुःखी लोक अच्छी तरह जानते, पहचानते है उसे पहचानने की दिशा में प्रवृत्तिशील रहते हैं। ठीक उसी तरह दुःखादि सबकी मूल जड तो कर्म ही है। समस्त कर्म को जानना अत्यन्त आवश्यक है।
मैं ज्ञान दर्शनादि चेतनवान् आत्मा हुं। ज्ञान-दर्शनादि गुणों को ढकनेवाले आवरक कर्म ही है। अतः कर्म आत्मा के रिपु-शत्रु है। इस अरि का हनन (नाश) करना ही साधना है। यह साधना करने पर ही सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसी सिद्धि को पाए हुए को अर्थात् कर्मरुप आत्म अरियों(शत्रुओं) का हनन करनेवाले ही सर्वथा कर्मावरण रहित अकर्मी, अशरीरी, अजन्मा, अकाल अवस्था प्राप्त हो जाय यही सिद्धावस्था है। वे ही सिद्ध कहलाते है। अरिहंत सदेह मुक्त ईश्वर (परमात्मा) है और सिद्ध विदेह मुक्त परमात्मा ईश्वर है।
ये आत्मशत्रु कर्म कहां से आए? क्या किसी अन्य द्वारा आए हैं ? नही. मेरे कर्मों का कर्ता मैं स्वयं हु। न कोई अन्य। मैने ही राग-द्वेषादि द्वारा जो पाप प्रवृत्ति की है उसी पाप के बने हुए पिंड को कर्म कहते है। मैंने ही कर्म को बनाया है। मेरे ही बनाए हुए है। मकडी जैसे स्वयं की बनाई जाल में फस जाती है वैसे ही मैं भी कर्म रुपी जाल में फस चूका हुं। अब इस कर्म की बिछाई हुई जाल को भेदने हेतु दुश्मन की ताकात का परचा प्राप्त कर ही लेना चाहिए। यह कर्म शत्रु कौन है? कैसे है?ये किस तरह बने है? क्या करने इसका निमार्ण हुआ है? इनके मुख्य भेद-प्रभेद कितने