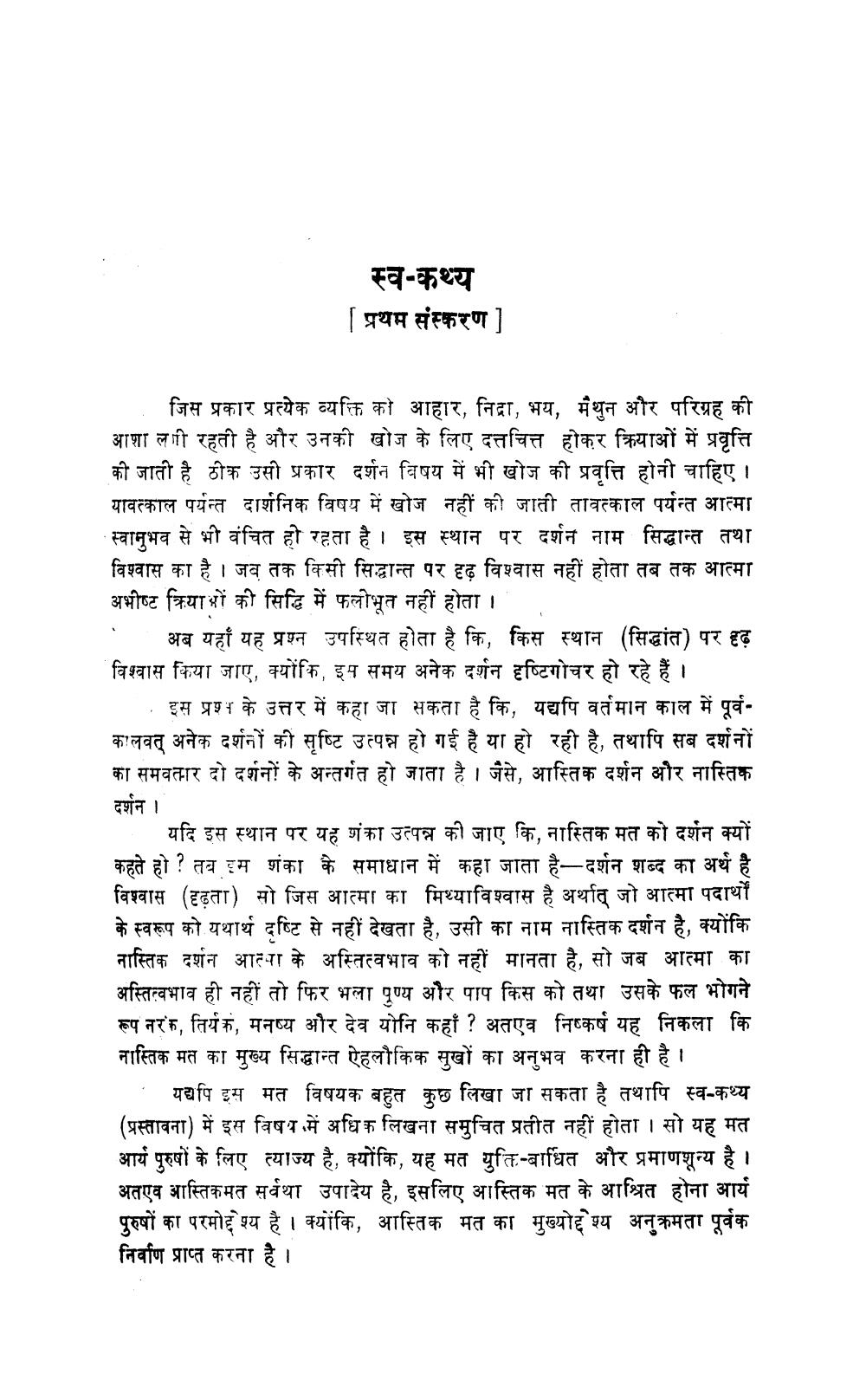________________
स्व-कथ्य [प्रथम संस्करण]
जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को आहार, निद्रा, भय, मैथुन और परिग्रह की आशा लगी रहती है और उनकी खोज के लिए दत्तचित्त होकर क्रियाओं में प्रवृत्ति की जाती है ठीक उसी प्रकार दर्शन विषय में भी खोज की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यावत्काल पर्यन्त दार्शनिक विषय में खोज नहीं की जाती तावत्काल पर्यन्त आत्मा स्वानुभव से भी वंचित हो रहता है। इस स्थान पर दर्शन नाम सिद्धान्त तथा विश्वास का है। जब तक किसी सिद्धान्त पर दृढ़ विश्वास नहीं होता तब तक आत्मा अभीष्ट क्रियाओं की सिद्धि में फलोभूत नहीं होता। ' अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, किस स्थान (सिद्धांत) पर दृढ़ विश्वास किया जाए, क्योंकि, इस समय अनेक दर्शन दृष्टिगोचर हो रहे हैं।
. इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि, यद्यपि वर्तमान काल में पूर्वकालवत् अनेक दर्शनों की सृष्टि उत्पन्न हो गई है या हो रही है, तथापि सब दर्शनों का समवतार दो दर्शनों के अन्तर्गत हो जाता है । जैसे, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन।
__यदि इस स्थान पर यह शंका उत्पन्न की जाए कि, नास्तिक मत को दर्शन क्यों कहते हो? तब हम शंका के समाधान में कहा जाता है-दर्शन शब्द का अर्थ है विश्वास (दृढ़ता) सो जिस आत्मा का मिथ्याविश्वास है अर्थात् जो आत्मा पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ दष्टि से नहीं देखता है, उसी का नाम नास्तिक दर्शन है, क्योंकि नास्तिक दर्शन आत्मा के अस्तित्वभाव को नहीं मानता है, सो जब आत्मा का अस्तित्वभाव ही नहीं तो फिर भला पुण्य और पाप किस को तथा उसके फल भोगने रूप नरक, तिर्यक, मनष्य और देव योनि कहाँ ? अतएव निष्कर्ष यह निकला कि नास्तिक मत का मुख्य सिद्धान्त ऐहलौकिक सुखों का अनुभव करना ही है ।
यद्यपि इस मत विषयक बहुत कुछ लिखा जा सकता है तथापि स्व-कथ्य (प्रस्तावना) में इस विषय में अधिक लिखना समुचित प्रतीत नहीं होता । सो यह मत आर्य पुरुषों के लिए त्याज्य है, क्योंकि, यह मत युक्ति-बाधित और प्रमाणशून्य है। अतएव आस्तिकमत सर्वथा उपादेय है, इसलिए आस्तिक मत के आश्रित होना आर्य पुरुषों का परमोद्देश्य है । क्योंकि, आस्तिक मत का मुख्योद्देश्य अनुक्रमता पूर्वक निर्वाण प्राप्त करना है।