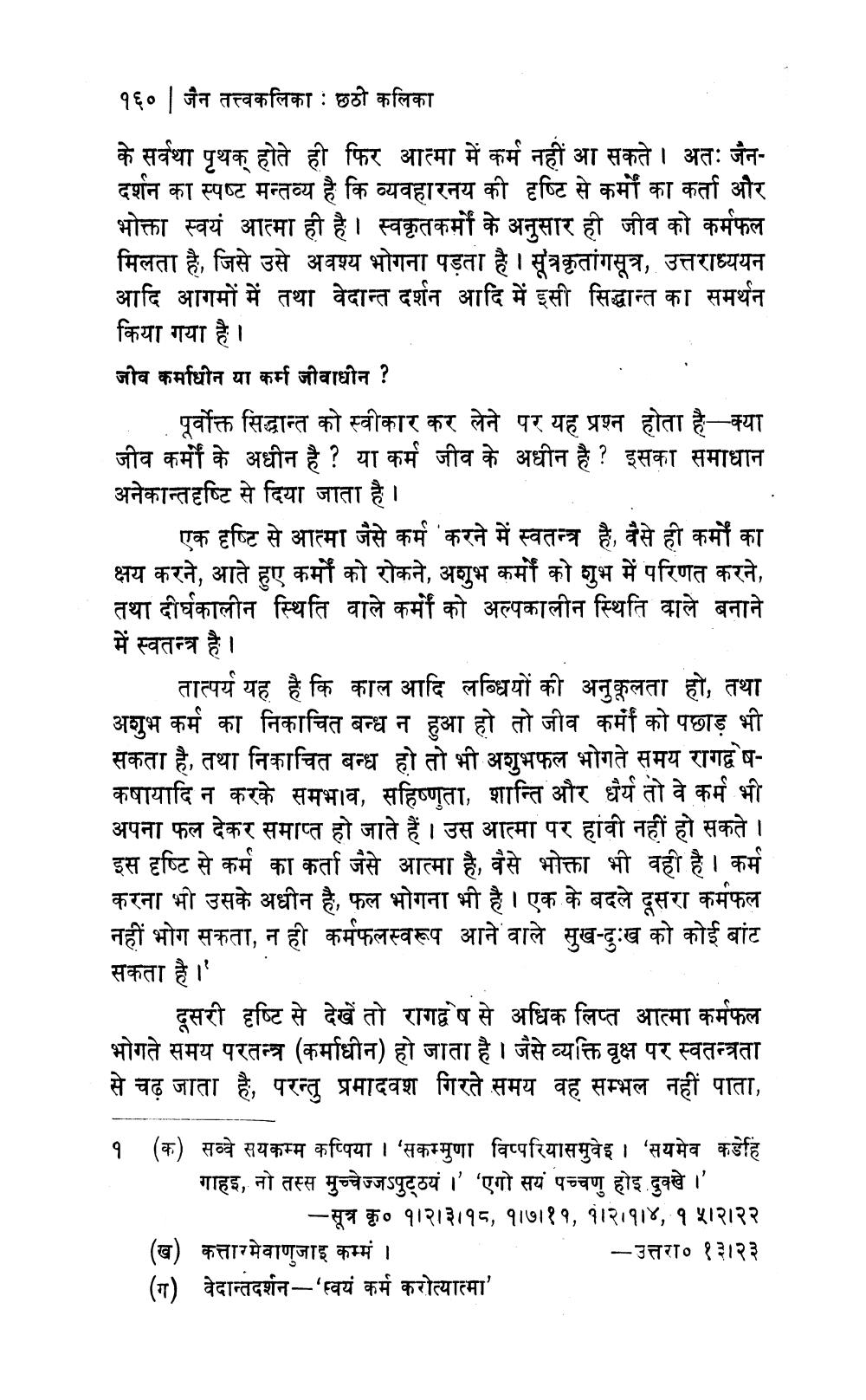________________
१६० | जैन तत्त्वकलिका : छठी कलिका के सर्वथा पृथक् होते ही फिर आत्मा में कर्म नहीं आ सकते । अतः जैनदर्शन का स्पष्ट मन्तव्य है कि व्यवहारनय की दृष्टि से कर्मों का कर्ता और भोक्ता स्वयं आत्मा ही है। स्वकृतकर्मों के अनुसार ही जीव को कर्मफल मिलता है, जिसे उसे अवश्य भोगना पड़ता है। सूत्रकृतांगसूत्र, उत्तराध्ययन आदि आगमों में तथा वेदान्त दर्शन आदि में इसी सिद्धान्त का समर्थन किया गया है। जीव कर्माधीन या कर्म जीवाधीन ?
पूर्वोक्त सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर यह प्रश्न होता है क्या जीव कर्मों के अधीन है ? या कर्म जीव के अधीन है ? इसका समाधान अनेकान्तदृष्टि से दिया जाता है।
एक दृष्टि से आत्मा जैसे कर्म करने में स्वतन्त्र है, वैसे ही कर्मों का क्षय करने, आते हुए कर्मों को रोकने, अशुभ कर्मों को शुभ में परिणत करने, तथा दीर्घकालीन स्थिति वाले कर्मों को अल्पकालीन स्थिति वाले बनाने में स्वतन्त्र है।
तात्पर्य यह है कि काल आदि लब्धियों की अनुकूलता हो, तथा अशुभ कर्म का निकाचित बन्ध न हुआ हो तो जीव कर्मी को पछाड़ भी सकता है, तथा निकाचित बन्ध हो तो भी अशुभफल भोगते समय रागद्वषकषायादि न करके समभाव, सहिष्णुता, शान्ति और धैर्य तो वे कर्म भी अपना फल देकर समाप्त हो जाते हैं । उस आत्मा पर हावी नहीं हो सकते । इस दृष्टि से कर्म का कर्ता जैसे आत्मा है, वैसे भोक्ता भी वही है। कर्म करना भी उसके अधीन है, फल भोगना भी है। एक के बदले दूसरा कमफल नहीं भोग सकता, न ही कर्मफलस्वरूप आने वाले सुख-दुःख को कोई बांट सकता है।'
दूसरी दृष्टि से देखें तो रागद्वेष से अधिक लिप्त आत्मा कर्मफल भोगते समय परतन्त्र (कर्माधीन) हो जाता है। जैसे व्यक्ति वृक्ष पर स्वतन्त्रता से चढ़ जाता है, परन्तु प्रमादवश गिरते समय वह सम्भल नहीं पाता,
१ (क) सव्वे सयकम्म कप्पिया । 'सकम्मुणा विप्परियासमुवेइ । 'सयमेव कडेहि गाहइ, नो तस्स मुच्चेज्जऽपुठ्ठयं ।' 'एगो सयं पच्चणु होइ दुक्खे ।'
-सूत्र कृ० १।२।३।१८, १७।११, १।२।१।४, १५।२।२२ (ख) कत्तारमेवाणुजाइ कम्मं ।
-उत्तरा०१३१२३ (ग) वेदान्तदर्शन- 'स्वयं कर्म करोत्यात्मा'