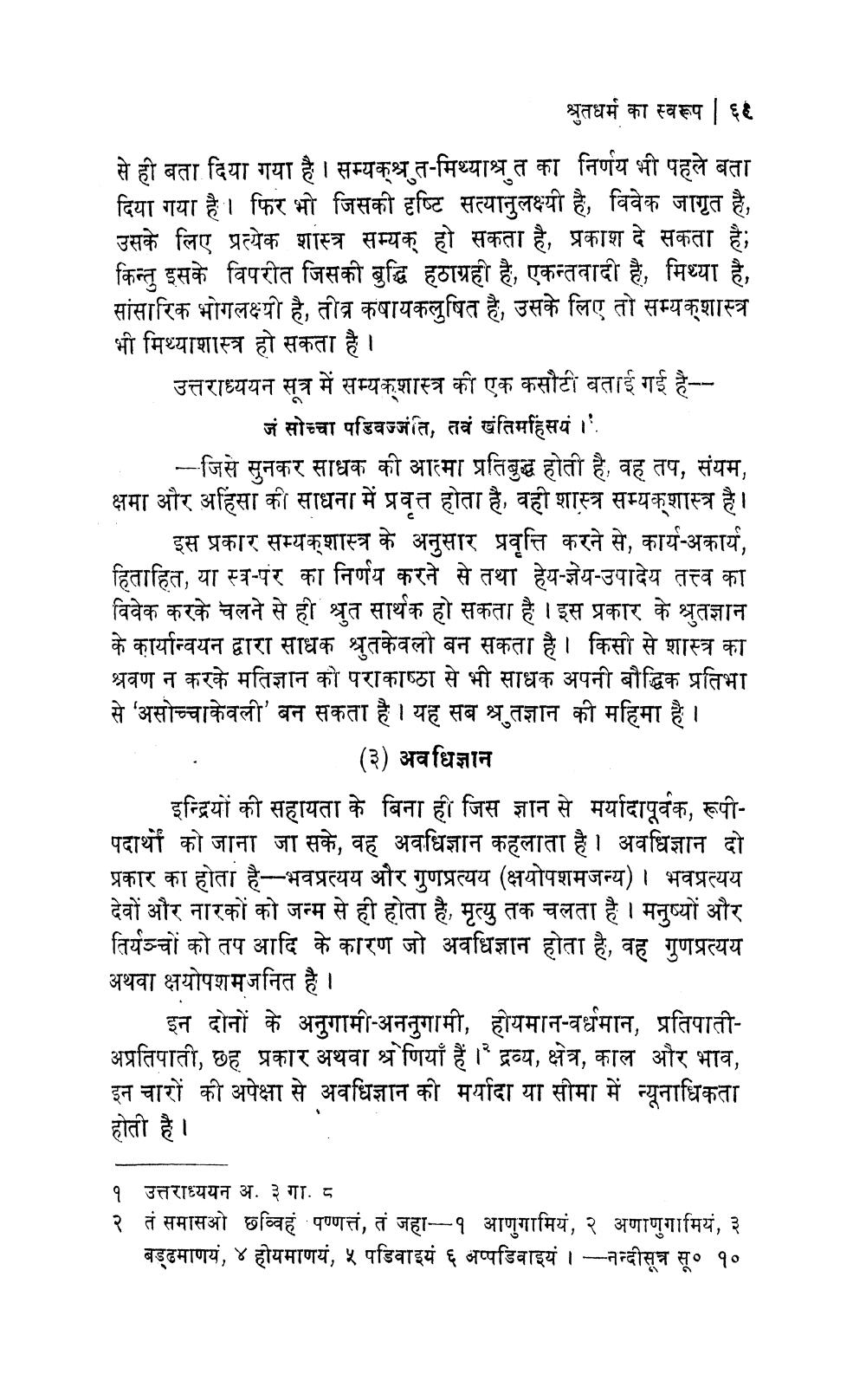________________
श्रुतधर्म का स्वरूप | ६६ से ही बता दिया गया है । सम्यक्च त-मिथ्याश्रु त का निर्णय भी पहले बता दिया गया है। फिर भी जिसकी दृष्टि सत्यानुलक्ष्यी है, विवेक जागृत है, उसके लिए प्रत्येक शास्त्र सम्यक् हो सकता है, प्रकाश दे सकता है; किन्तु इसके विपरीत जिसकी बुद्धि हठाग्रही है, एकन्तवादी है, मिथ्या है, सांसारिक भोगलक्ष्यी है, तीव्र कषायकलुषित है, उसके लिए तो सम्यकशास्त्र भी मिथ्याशास्त्र हो सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र में सम्यकशास्त्र की एक कसौटी बताई गई है--
जं सोच्चा पडिवज्जंति, तवं खंतिहिंसयं । . -जिसे सुनकर साधक की आत्मा प्रतिबुद्ध होती है, वह तप, संयम, क्षमा और अहिंसा की साधना में प्रवत्त होता है, वही शास्त्र सम्यकशास्त्र है।
इस प्रकार सम्यकशास्त्र के अनुसार प्रवृत्ति करने से, कार्य-अकार्य, हिताहित, या स्व-पर का निर्णय करने से तथा हेय-ज्ञेय-उपादेय तत्त्व का विवेक करके चलने से ही श्रुत सार्थक हो सकता है । इस प्रकार के श्रुतज्ञान के कार्यान्वयन द्वारा साधक श्रुतकेवलो बन सकता है। किसी से शास्त्र का श्रवण न करके मतिज्ञान को पराकाष्ठा से भी साधक अपनी बौद्धिक प्रतिभा से 'असोच्चाकेवली' बन सकता है । यह सब श्र तज्ञान की महिमा है।
(३) अवधिज्ञान इन्द्रियों की सहायता के बिना ही जिस ज्ञान से मर्यादापूर्वक, रूपीपदार्थों को जाना जा सके, वह अवधिज्ञान कहलाता है। अवधिज्ञान दो प्रकार का होता है-भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय (क्षयोपशमजन्य)। भवप्रत्यय देवों और नारकों को जन्म से ही होता है, मृत्यु तक चलता है । मनुष्यों और तिर्यञ्चों को तप आदि के कारण जो अवधिज्ञान होता है, वह गुणप्रत्यय अथवा क्षयोपशमजनित है।
इन दोनों के अनुगामी-अननुगामी, होयमान-वर्धमान, प्रतिपातीअप्रतिपाती, छह प्रकार अथवा श्रोणियाँ हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की अपेक्षा से अवधिज्ञान की मर्यादा या सीमा में न्यूनाधिकता होती है।
१ उत्तराध्ययन अ. ३ गा. ८ २ तं समासओ छव्विहं पण्णत्तं, तं जहा-१ आणुगामियं, २ अणाणुगामियं, ३
बड्ढमाणयं, ४ होयमाणयं, ५ पडिवाइयं ६ अप्पडिवाइयं । नन्दीसूत्र सू० १०