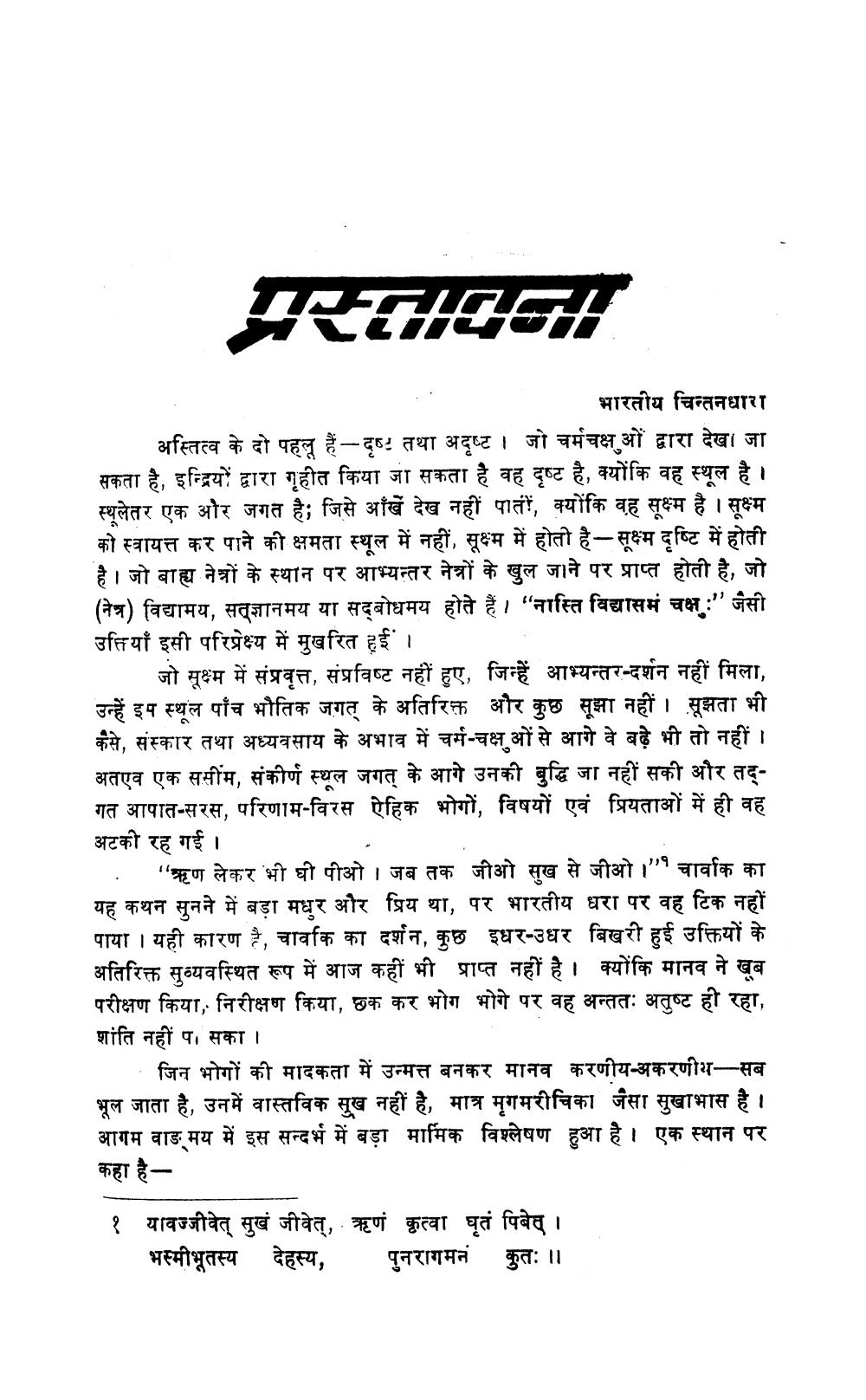________________
भारतीय चिन्तनधारा अस्तित्व के दो पहलू हैं- दृष्ट तथा अदृष्ट । जो चर्मचक्ष ओं द्वारा देखा जा सकता है, इन्द्रियों द्वारा गृहीत किया जा सकता है वह दृष्ट है, क्योंकि वह स्थूल है। स्थूलेतर एक और जगत है; जिसे आँखें देख नहीं पाती, क्योंकि वह सूक्ष्म है । सूक्ष्म को स्वायत्त कर पाने की क्षमता स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में होती है-सूक्ष्म दृष्टि में होती है। जो बाह्य नेत्रों के स्थान पर आभ्यन्तर नेत्रों के खुल जाने पर प्राप्त होती है, जो (नेत्र) विद्यामय, सत्ज्ञानमय या सद्बोधमय होते हैं। "नास्ति विद्यासमं चक्ष:" जैसी उत्तियाँ इसी परिप्रेक्ष्य में मुखरित हुई।
जो सूक्ष्म में संप्रवृत्त, संप्रविष्ट नहीं हुए, जिन्हें आभ्यन्तर-दर्शन नहीं मिला, उन्हें इस स्थूल पाँच भौतिक जगत् के अतिरिक्त और कुछ सूझा नहीं। सूझता भी कैसे, संस्कार तथा अध्यवसाय के अभाव में चर्म-चक्ष ओं से आगे वे बढ़े भी तो नहीं। अतएव एक ससीम, संकीर्ण स्थल जगत् के आगे उनकी बुद्धि जा नहीं सकी और तद्गत आपात-सरस, परिणाम-विरस ऐहिक भोगों, विषयों एवं प्रियताओं में ही वह अटकी रह गई।
. "ऋण लेकर भी घी पीओ । जब तक जीओ सुख से जीओ।' चार्वाक का यह कथन सुनने में बड़ा मधुर और प्रिय था, पर भारतीय धरा पर वह टिक नहीं पाया । यही कारण है, चार्वाक का दर्शन, कुछ इधर-उधर बिखरी हुई उक्तियों के अतिरिक्त सुव्यवस्थित रूप में आज कहीं भी प्राप्त नहीं है। क्योंकि मानव ने खुब परीक्षण किया निरीक्षण किया, छक कर भोग भोगे पर वह अन्ततः अतुष्ट ही रहा, शांति नहीं पा सका।
- जिन भोगों की मादकता में उन्मत्त बनकर मानव करणीय-अकरणीय-सब भूल जाता है, उनमें वास्तविक सुख नहीं है, मात्र मृगमरीचिका जैसा सुखाभास है। आगम वाङमय में इस सन्दर्भ में बड़ा मार्मिक विश्लेषण हुआ है। एक स्थान पर कहा है
१ यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।
भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुतः ।।