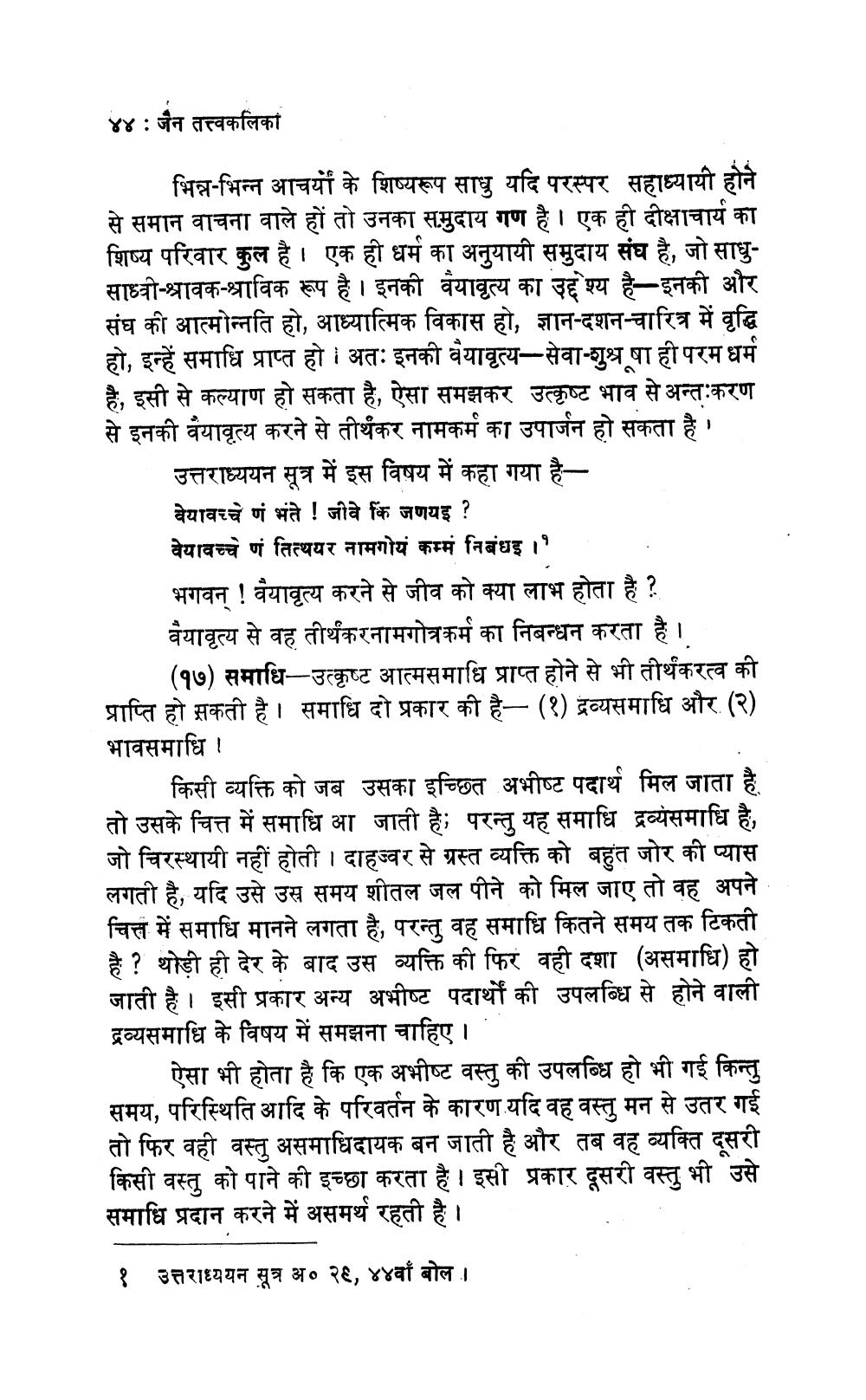________________
४४ : जैन तत्त्वकलिका
भिन्न-भिन्न आचर्यों के शिष्यरूप साधु यदि परस्पर सहाध्यायी होने से समान वाचना वाले हों तो उनका समुदाय गण है । एक ही दीक्षाचार्य का शिष्य परिवार कुल है। एक ही धर्म का अनुयायी समुदाय संघ है, जो साधुसाध्वी-श्रावक-श्राविक रूप है । इनकी वैयावृत्य का उद्देश्य है-इनकी और संघ की आत्मोन्नति हो, आध्यात्मिक विकास हो, ज्ञान-दशन-चारित्र में वृद्धि हो, इन्हें समाधि प्राप्त हो । अतः इनकी वैयावृत्य-सेवा-शुश्रूषा ही परम धर्म है, इसी से कल्याण हो सकता है, ऐसा समझकर उत्कृष्ट भाव से अन्तःकरण से इनकी वैयावृत्य करने से तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन हो सकता है ।
उत्तराध्ययन सूत्र में इस विषय में कहा गया हैवेयावच्चे णं भंते ! जीवे कि जणयइ ? वेयावच्चे णं तित्थयर नामगोयं कम्मं निबंधइ ।' भगवन् ! वैयावृत्य करने से जीव को क्या लाभ होता है ? वैयावृत्य से वह तीर्थंकरनामगोत्रकर्म का निबन्धन करता है।
(१७) समाधि-उत्कृष्ट आत्मसमाधि प्राप्त होने से भी तीर्थंकरत्व की प्राप्ति हो सकती है। समाधि दो प्रकार की है- (१) द्रव्यसमाधि और (२) भावसमाधि ।
किसी व्यक्ति को जब उसका इच्छित अभीष्ट पदार्थ मिल जाता है, तो उसके चित्त में समाधि आ जाती है। परन्तु यह समाधि द्रव्यसमाधि है, जो चिरस्थायी नहीं होती। दाहज्वर से ग्रस्त व्यक्ति को बहुत जोर की प्यास लगती है, यदि उसे उस समय शीतल जल पीने को मिल जाए तो वह अपने चित्त में समाधि मानने लगता है, परन्तु वह समाधि कितने समय तक टिकती है ? थोड़ी ही देर के बाद उस व्यक्ति की फिर वही दशा (असमाधि) हो जाती है। इसी प्रकार अन्य अभीष्ट पदार्थों की उपलब्धि से होने वाली द्रव्यसमाधि के विषय में समझना चाहिए।
ऐसा भी होता है कि एक अभीष्ट वस्तु की उपलब्धि हो भी गई किन्तु समय, परिस्थिति आदि के परिवर्तन के कारण यदि वह वस्तु मन से उतर गई तो फिर वही वस्तू असमाधिदायक बन जाती है और तब वह व्यक्ति दसरी किसी वस्तु को पाने की इच्छा करता है। इसी प्रकार दूसरी वस्तु भी उसे समाधि प्रदान करने में असमर्थ रहती है।
१ उत्तराध्ययन सूत्र अ० २६, ४४वाँ बोल ।