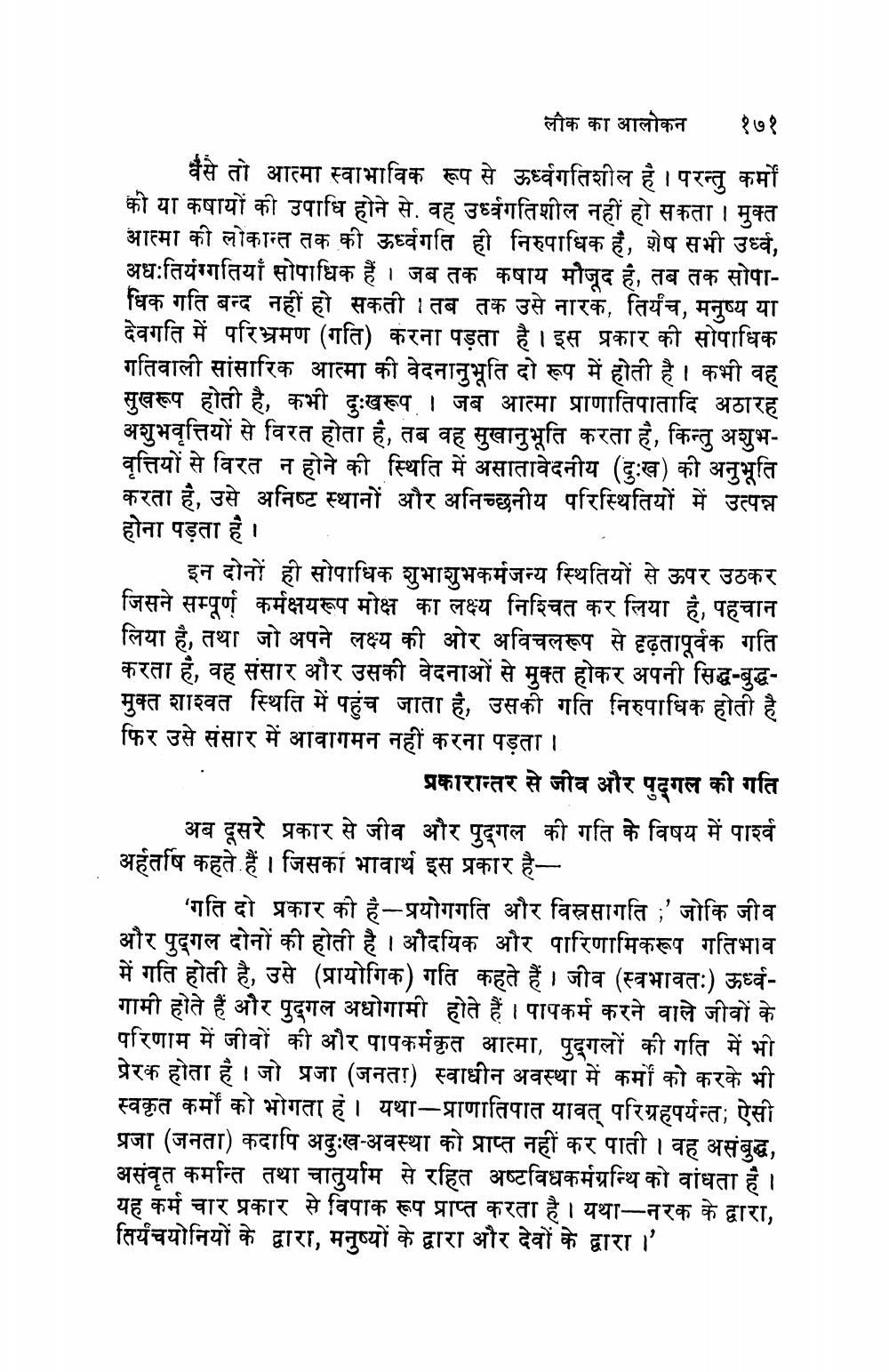________________
ate का आलोकन १७१
वैसे तो आत्मा स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगतिशील | परन्तु कर्मों की या कषायों की उपाधि होने से वह उर्ध्वगतिशील नहीं हो सकता । मुक्त आत्मा की लोकान्त तक की ऊर्ध्वगति ही निरुपाधिक है, शेष सभी उर्ध्व, अधः तिर्यग्गतियाँ सोपाधिक हैं । जब तक कषाय मौजूद है, तब तक सोपाधिक गति बन्द नहीं हो सकती । तब तक उसे नारक, तिर्यंच, मनुष्य या देवगति में परिभ्रमण (गति) करना पड़ता है । इस प्रकार की सोपाधिक गतिवाली सांसारिक आत्मा की वेदनानुभूति दो रूप में होती है । कभी वह सुखरूप होती है, कभी दुःखरूप । जब आत्मा प्राणातिपातादि अठारह अशुभवृत्तियों से विरत होता है, तब वह सुखानुभूति करता है, किन्तु अशुभवृत्तियों से विरत न होने की स्थिति में असातावेदनीय ( दुःख) की अनुभूति करता है, उसे अनिष्ट स्थानों और अनिच्छनीय परिस्थितियों में उत्पन्न होना पड़ता है ।
इन दोनों ही सोपाधिक शुभाशुभकर्मजन्य स्थितियों से ऊपर उठकर जिसने सम्पूर्ण कर्मक्षयरूप मोक्ष का लक्ष्य निश्चित कर लिया है, पहचान लिया है, तथा जो अपने लक्ष्य की ओर अविचलरूप से दृढ़तापूर्वक गति करता है, वह संसार और उसकी वेदनाओं से मुक्त होकर अपनी सिद्ध-बुद्धमुक्त शाश्वत स्थिति में पहुंच जाता है, उसकी गति निरुपाधिक होती है फिर उसे संसार में आवागमन नहीं करना पड़ता ।
प्रकारान्तर से जीव और पुद्गल की गति
अब दूसरे प्रकार से जीव और पुद्गल की गति के विषय में पार्श्व कहते हैं । जिसका भावार्थ इस प्रकार है
'गति दो प्रकार की है - प्रयोगगति और विस्रसागति' जोकि जीव और पुद्गल दोनों की होती है । औदयिक और पारिणामिकरूप गतिभाव में गति होती है, उसे ( प्रायोगिक) गति कहते हैं। जीव (स्वभावतः ) ऊर्ध्व - गामी होते हैं और पुद्गल अधोगामी होते हैं । पापकर्म करने वाले जीवों के परिणाम में जीवों की और पापकर्मकृत आत्मा, पुद्गलों की गति में भी प्रेरक होता है । जो प्रजा (जनता) स्वाधीन अवस्था में कर्मों को करके भी स्वकृत कर्मों को भोगता है । यथा - प्राणातिपात यावत् परिग्रहपर्यन्त; ऐसी प्रजा (जनता) कदापि अदुःख अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती । वह असंबुद्ध, असंवृत कर्मान्त तथा चातुर्याम से रहित अष्टविधकर्मग्रन्थि को वांधता है । यह कर्म चार प्रकार से विपाक रूप प्राप्त करता है । यथा-नरक के द्वारा, तिर्यंचयोनियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा और देवों के द्वारा ।'